UP Board Class 12 Hindi General Question Paper 2025 PDF (Code 302 HL) is available for download here. The Mathematics exam was conducted on February 24, 2025 in the Evening Shift from 2:00 PM to 5:15 PM. The total marks for the theory paper are 100. Students reported the paper to be easy to moderate.
UP Board Class 12 Hindi General Question Paper 2025 (Code 302 HL) with Solutions
| UP Board Class Hindi General Question Paper with Answer Key | Check Solutions |

‘पुनर्नवा’ उपन्यास के लेखक हैं
View Solution
पद १: लेखक की पहचान और उनकी विशिष्ट शैली।
'पुनर्नवा' हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आचार्य द्विवेदी को उनके ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिनमें वे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कथानकों को आधार बनाकर समकालीन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक प्रश्नों को उठाते हैं।
पद २: उपन्यास की विषय-वस्तु।
'पुनर्नवा' चौथी शताब्दी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया उपन्यास है। इसमें इतिहास, कल्पना और लोक-जीवन का अद्भुत मिश्रण है। यह उपन्यास नारी-जीवन की गरिमा और सामाजिक संघर्षों का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है।
पद ३: अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ।
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'बाणभट्ट की आत्मकथा', 'चारु चंद्रलेख', और 'अनामदास का पोथा' हैं। ये सभी उपन्यास उनकी गहरी ऐतिहासिक दृष्टि और सांस्कृतिक समझ को दर्शाते हैं।
पद ४: निष्कर्ष।
अतः, 'पुनर्नवा' उपन्यास के लेखक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं।
Quick Tip: प्रमुख उपन्यासकारों और उनके कम से कम दो-तीन प्रसिद्ध उपन्यासों की सूची बनाकर याद करें। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
‘महके आँगन चहके द्वार’ के लेखक हैं
View Solution
पद १: लेखक और उनकी गद्य-शैली का परिचय।
'महके आँगन चहके द्वार' हिंदी के प्रसिद्ध गद्य-शिल्पी कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ की रचना है। 'प्रभाकर' जी अपनी काव्यात्मक और भावपूर्ण गद्य-शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वे साधारण जीवन के अनुभवों को भी एक दार्शनिक और मानवीय स्पर्श प्रदान करते हैं।
पद २: कृति की विधा और शीर्षक की सार्थकता।
यह कृति 'ललित निबंध' विधा के अंतर्गत आती है। इसका शीर्षक 'महके आँगन चहके द्वार' स्वयं लेखक की शैली को दर्शाता है, जिसमें जीवन के उल्लास और सकारात्मकता की सुगंध है। उनके निबंधों में आत्मपरकता, भावुकता और एक सहज प्रवाह होता है।
पद ३: निष्कर्ष।
इस विशिष्ट काव्यात्मक गद्य-शैली के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि 'महके आँगन चहके द्वार' के लेखक कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियों में 'बाजे पायलिया के घुँघरू' और 'माटी हो गई सोना' शामिल हैं।
Quick Tip: हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे ललित निबंध, रिपोर्ताज, संस्मरण के प्रमुख लेखकों और उनकी एक-एक प्रसिद्ध रचना का नाम अवश्य याद रखें।
‘संस्कृति के चार अध्याय’ के लेखक हैं
View Solution
पद १: कृति का परिचय और पुरस्कार।
'संस्कृति के चार अध्याय' हिंदी साहित्य का एक गौरव-ग्रंथ है, जिसे भारतीय संस्कृति का महाकोश भी कहा जा सकता है। इस कृति की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे सन् 1959 में 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।
पद २: लेखक का परिचय।
इस महान कृति के रचनाकार 'राष्ट्रकवि' रामधारी सिंह ‘दिनकर’ हैं। दिनकर जी अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही वे एक गंभीर गद्य-चिंतक भी थे। यह ग्रंथ उनके गहन अध्ययन, चिंतन और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रमाण है।
पद ३: कृति की विषय-वस्तु।
इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत की संस्कृति को चार प्रमुख क्रांतियों के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आर्यों के आगमन, बौद्ध-जैन धर्मों के उदय, इस्लाम के प्रभाव और यूरोपीय संपर्क के फलस्वरूप हुईं। इसकी भूमिका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी।
पद ४: निष्कर्ष।
अतः, भारतीय संस्कृति का यह गहन विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ ‘संस्कृति के चार अध्याय’ के लेखक रामधारी सिंह ‘दिनकर’ हैं।
Quick Tip: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित रचनाओं और उनके लेखकों की सूची बनाना परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है।
मुंशी प्रेमचन्द द्वारा सम्पादित पत्र है
View Solution
पद १: प्रेमचंद और पत्रकारिता।
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द केवल एक महान कथाकार ही नहीं, बल्कि एक सजग विचारक और पत्रकार भी थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया।
पद २: 'हंस' का संपादन और उद्देश्य।
सन् 1930 में प्रेमचंद ने बनारस से 'हंस' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्रिका का उद्देश्य प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना और नवोदित लेखकों को एक मंच प्रदान करना था। 'हंस' अपने समय की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक बन गई।
पद ३: अन्य विकल्पों का निराकरण।
यद्यपि प्रेमचंद ने कुछ समय के लिए 'मर्यादा' का भी संपादन किया था, लेकिन 'हंस' के वे संस्थापक संपादक थे और यह पत्रिका सीधे तौर पर उनसे जुड़ी है। 'कर्मवीर' का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और 'धर्मयुग' का संपादन धर्मवीर भारती ने किया था।
पद ४: निष्कर्ष।
अतः, दिए गए विकल्पों में से 'हंस' वह प्रमुख पत्र है जिसका संपादन मुंशी प्रेमचन्द ने किया था।
Quick Tip: हिंदी के प्रमुख लेखकों और उनके द्वारा संपादित की गई पत्रिकाओं के नाम याद रखें। जैसे- भारतेन्दु हरिश्चंद्र ('कविवचन सुधा'), महावीर प्रसाद द्विवेदी ('सरस्वती') और प्रेमचंद ('हंस')।
निम्नलिखित में से कौन-सी रचना ‘अज्ञेय’ का यात्रा-वृत्तान्त है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न प्रसिद्ध साहित्यकार 'अज्ञेय' की रचनाओं की विधा की पहचान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने कई विधाओं में लेखन किया है।
(A) ‘स्मृतिलेखा’ एक डायरी है।
(B) ‘एक बूँद सहसा उछली’ एक प्रसिद्ध यात्रा-वृत्तान्त है। उनका एक अन्य यात्रा-वृत्तान्त 'अरे यायावर रहेगा याद' भी बहुत प्रसिद्ध है।
(C) ‘आँगन के पार द्वार’ उनका काव्य-संग्रह है।
(D) ‘अपने अपने अजनबी’ उनका उपन्यास है।
Step 3: Final Answer:
दिए गए विकल्पों में से ‘एक बूँद सहसा उछली’ ‘अज्ञेय’ का यात्रा-वृत्तान्त है। इसलिए, विकल्प (B) सही है।
Quick Tip: प्रमुख लेखकों की अलग-अलग विधाओं की रचनाओं को याद रखें। अज्ञेय जैसे बहुमुखी प्रतिभा के लेखक की कविता, उपन्यास और यात्रा-वृत्तान्त की एक-एक रचना का नाम याद रखना उपयोगी है।
‘चिदम्बरा’ कृति किस रचनाकार की है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न हिंदी साहित्य की एक पुरस्कृत कृति और उसके रचनाकार से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'चिदम्बरा' छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का एक प्रसिद्ध काव्य-संग्रह है।
यह पंत जी की काव्य-चेतना के विभिन्न सोपानों का प्रतिनिधित्व करता है।
इस कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को सन् 1968 में 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था, जो हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था।
Step 3: Final Answer:
‘चिदम्बरा’ के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। इसलिए, विकल्प (B) सही है।
Quick Tip: ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के सभी साहित्यकारों और उनकी पुरस्कृत कृतियों (जैसे- पंत को 'चिदम्बरा', दिनकर को 'उर्वशी', अज्ञेय को 'कितनी नावों में कितनी बार', महादेवी को 'यामा') के नाम अवश्य याद रखें।
‘कामायनी’ महाकाव्य किस काल की कृति है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न हिंदी के एक प्रसिद्ध महाकाव्य और उसके साहित्यिक काल की पहचान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'कामायनी' जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आधुनिक खड़ी बोली का एक अद्वितीय महाकाव्य है।
जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे।
'कामायनी' को छायावाद की सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि रचना माना जाता है। इसका प्रकाशन सन् 1936 में हुआ था।
Step 3: Final Answer:
‘कामायनी’ महाकाव्य छायावाद युग की कृति है। इसलिए, विकल्प (D) सही है।
Quick Tip: हिंदी साहित्य के प्रमुख युगों (आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल) और उनके प्रतिनिधि महाकाव्यों (जैसे- पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, कामायनी) को याद रखना महत्वपूर्ण है।
‘तीसरा सप्तक’ का प्रकाशन वर्ष है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न आधुनिक हिंदी कविता के 'प्रयोगवाद' और 'तार सप्तक' परंपरा से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'अज्ञेय' के संपादन में चार 'सप्तकों' का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी।
तार सप्तक का प्रकाशन सन् 1943 में हुआ।
दूसरा सप्तक का प्रकाशन सन् 1951 में हुआ।
तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन् 1959 में हुआ।
चौथा सप्तक का प्रकाशन सन् 1979 में हुआ।
Step 3: Final Answer:
‘तीसरा सप्तक’ का प्रकाशन वर्ष सन् 1959 है। इसलिए, विकल्प (C) सही है।
Quick Tip: चारों सप्तकों के प्रकाशन वर्ष (1943, 1951, 1959, 1979) और उनके संपादक 'अज्ञेय' का नाम अवश्य याद रखें। यह आधुनिक हिंदी कविता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
‘रामधारी सिंह दिनकर’ को काव्य कृति ‘उर्वशी’ पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न एक प्रसिद्ध काव्य कृति और उसे प्राप्त हुए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'उर्वशी' रामधारी सिंह 'दिनकर' द्वारा रचित एक गीतिनाट्य (काव्य-नाटक) है।
यह प्रेम, सौन्दर्य और दर्शन पर आधारित एक उत्कृष्ट रचना है।
इस महान कृति के लिए रामधारी सिंह 'दिनकर' को सन् 1972 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।
उन्हें 'संस्कृति के चार अध्याय' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
Step 3: Final Answer:
‘दिनकर’ को उनकी काव्य कृति ‘उर्वशी’ पर ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ प्राप्त हुआ था। इसलिए, विकल्प (C) सही है।
Quick Tip: एक ही लेखक को अलग-अलग रचनाओं के लिए मिले विभिन्न पुरस्कारों में अंतर करना सीखें। जैसे दिनकर को 'संस्कृति के चार अध्याय' पर 'साहित्य अकादमी' और 'उर्वशी' पर 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार मिला।
‘राम की शक्ति पूजा’ कृति के रचनाकार हैं
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न छायावादी युग की एक प्रसिद्ध लम्बी कविता और उसके रचनाकार से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'राम की शक्ति पूजा' सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ द्वारा रचित एक प्रसिद्ध लम्बी कविता है।
यह कविता राम के चरित्र के माध्यम से निराशा पर आशा की विजय और शक्ति के संघर्ष को दर्शाती है।
यह 'अनामिका' (द्वितीय संस्करण) नामक काव्य-संग्रह में संकलित है।
'निराला' छायावाद के चार स्तंभों में से एक हैं और अपनी विद्रोही चेतना के लिए जाने जाते हैं।
Step 3: Final Answer:
‘राम की शक्ति पूजा’ के रचनाकार सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ हैं। इसलिए, विकल्प (D) सही है।
Quick Tip: हिंदी की प्रसिद्ध लम्बी कविताओं जैसे- 'राम की शक्ति पूजा' (निराला), 'असाध्य वीणा' (अज्ञेय), 'अंधेरे में' (मुक्तिबोध) और उनके रचनाकारों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है।
दिये गये गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है। यदि भाषा में
विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों
का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नये शब्दों
का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात् उन विदेशी भाषाओं से सीधे अंकित रूप से
उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से उपयोग हों, साहित्यिक दायरे में कतई ग्रहणीय नहीं। यदि
ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न
की आवश्यकता प्रतीत होती है।
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में दिए गए पहले गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखने के लिए कहा गया है।
Step 2: Identifying the Text:
यह गद्यांश भाषा की प्रकृति, उसकी इकाई (शब्द), उसमें नवीन शब्दों के समावेश और साहित्यिक शुद्धता पर विचार करता है। यह विषय-वस्तु और शैली प्रसिद्ध विचारक और निबंधकार प्रोफेसर जी. सुन्दर रेड्डी के वैचारिक निबंध 'भाषा और आधुनिकता' से मेल खाती है।
पाठ का शीर्षक: भाषा और आधुनिकता
लेखक का नाम: प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी
Step 3: Final Answer:
प्रस्तुत गद्यांश 'भाषा और आधुनिकता' नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी हैं।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
(पहला गद्यांश: यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है।)
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पहले गद्यांश के रेखांकित अंश का भावार्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
Step 2: Detailed Explanation:
व्याख्या: लेखक प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी कहते हैं कि जब हम किसी विदेशी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में अपनाते हैं, तो उसे ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम उस शब्द को साहित्यिक भाषा का अंग बनाना चाहते हैं, तो उसे अपनी भाषा की मूल प्रकृति (उसके व्याकरण, ध्वनि और ساخت) के अनुसार ढालना पड़ता है। उसे एक साहित्यिक रूप और शुद्धता देनी पड़ती है, ताकि वह विदेशी या अटपटा न लगे और हमारी भाषा में सहजता से घुल-मिल जाए।
Step 3: Final Answer:
रेखांकित अंश का आशय यह है कि विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में साहित्यिक स्तर पर स्वीकार करने के लिए उन्हें अपनी भाषा के व्याकरण और स्वभाव के अनुसार परिवर्तित करके शुद्ध साहित्यिक रूप देना आवश्यक है।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, केवल शाब्दिक अर्थ न लिखें। अंश के पीछे छिपे लेखक के दृष्टिकोण और मंतव्य को भी स्पष्ट करने का प्रयास करें। अपने उत्तर को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें।
भाषा की साधारण इकाई क्या है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
प्रश्न में यह पूछा गया है कि भाषा की मूलभूत या सामान्य इकाई किसे माना गया है।
Step 2: Explanation from the Passage:
पहले गद्यांश की पहली ही पंक्ति में इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है: "भाषा की साधारण इकाई शब्द है"।
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, भाषा की साधारण इकाई 'शब्द' है।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
Step 2: Explanation from the Passage:
पहले गद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में इसका उत्तर मिलता है: "दैनन्दिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिये गए हैं।"
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, हम दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए अनेक नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
‘दैनन्दिन’ और ‘अविकृत’ शब्दों के अर्थ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
प्रश्न में 'दैनन्दिन' और 'अविकृत' इन दो शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहा गया है।
Step 2: Meaning of the Words:
(i) दैनन्दिन: इस शब्द का अर्थ है - 'दैनिक', 'प्रतिदिन का' या 'रोजमर्रा का'।
(ii) अविकृत: इस शब्द का अर्थ है - 'जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न हुआ हो', 'अपने मूल रूप में'।
Step 3: Final Answer:
दैनन्दिन = दैनिक / प्रतिदिन का
अविकृत = बिना किसी परिवर्तन के / अपने मूल रूप में
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। केवल उतना ही याद रहती है, जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को
फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रहती? सारा संसार
स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी
अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के
परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को ढाककर बड़ी हुई थी और लाखों-करोड़ों की उपेक्षा से जो
समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गये, समाज ढह गये और मदनोत्सव की धूम-धाम भी मिट गई।
उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक के नाम लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में दिए गए दूसरे गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखने के लिए कहा गया है।
Step 2: Identifying the Text:
यह गद्यांश अशोक के वृक्ष, दुनिया की स्वार्थपरता और सामंती सभ्यता के परिष्कृत रुचि का वर्णन करता है। यह ललित निबंधात्मक शैली आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध 'अशोक के फूल' की है।
पाठ का शीर्षक: अशोक के फूल
लेखक का नाम: आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
Step 3: Final Answer:
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक 'अशोक के फूल' है और इसके लेखक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक दुनिया को भुलक्कड़ (भूल जाने वाली) क्यों कहते हैं।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश की पहली और दूसरी पंक्ति में इसका सीधा उत्तर है: "कहते हैं दुनियाँ बड़ी भुलक्कड़ है। केवल उतना ही याद रखती है, जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है।"
Step 3: Final Answer:
लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ इसलिए कहा है क्योंकि वह केवल उन्हीं बातों को याद रखती है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी व्यर्थ की बातों को वह भुला देती है।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
अशोक वृक्ष किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि अशोक का वृक्ष किसके परिष्कृत (refined) स्वाद का प्रतीक है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश में लिखा है: "...परन्तु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी..."
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, अशोक का वृक्ष उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक ने स्वार्थी किसे कहा है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश में लेखक ने दुनिया (अर्थात दुनिया के लोगों) को स्वार्थी कहा है। वह कहता है कि "सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है।" इसका तात्पर्य है कि दुनिया में रहने वाले अधिकांश लोग केवल अपने मतलब की बात याद रखते हैं और जिनसे उनका मतलब नहीं सधता, उन्हें भूल जाते हैं।
Step 3: Final Answer:
लेखक ने दुनिया के उन सभी लोगों को स्वार्थी कहा है जो केवल अपने मतलब की बात याद रखते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं।
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।
‘परिष्कृत’ और ‘मदनोत्सव’ शब्दों के अर्थ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
प्रश्न में 'परिष्कृत' और 'मदनोत्सव' इन दो शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहा गया है।
Step 2: Meaning of the Words:
(i) परिष्कृत: इस शब्द का अर्थ है - 'शुद्ध किया हुआ', 'साफ़-सुथरा', 'सजा-सँवरा' या 'Refined'।
(ii) मदनोत्सव: यह दो शब्दों से मिलकर बना है - मदन (कामदेव) + उत्सव। इसका अर्थ है 'कामदेव का उत्सव' या 'वसंतोत्सव'।
Step 3: Final Answer:
परिष्कृत = शुद्ध किया हुआ / सँवारा हुआ
मदनोत्सव = कामदेव का उत्सव / वसंत का त्योहार
Quick Tip: परीक्षा में गद्य के पाठों का सन्दर्भ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके लिए अपनी पाठ्य-पुस्तक के सभी पाठों के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम की एक सूची बना लें और उसे नियमित रूप से दोहराएँ।

उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में दिए गए पद्यांश का सन्दर्भ लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें कवि का नाम और कविता का शीर्षक बताना होता है।
Step 2: Detailed Explanation:
प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य 'कुरुक्षेत्र' के षष्ठ सर्ग से हमारी पाठ्य-पुस्तक में संकलित 'अभिनव मनुष्य' नामक शीर्षक से उद्धृत है।
इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक मनुष्य की भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति का ओजस्वी वर्णन करते हुए उसकी आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता पर बल दिया है।
सन्दर्भ: प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' द्वारा रचित 'कुरुक्षेत्र' से हमारी पाठ्य-पुस्तक में संकलित 'अभिनव मनुष्य' शीर्षक काव्यांश से लिया गया है।
Step 3: Final Answer:
यह पद्यांश रामधारी सिंह 'दिनकर' द्वारा रचित 'अभिनव मनुष्य' नामक कविता से लिया गया है।
Quick Tip: पद्य का सन्दर्भ लिखते समय, कवि के नाम, कविता के शीर्षक के साथ-साथ यदि संभव हो तो उस काव्य-संग्रह या महाकाव्य का नाम भी लिखें जहाँ से कविता ली गई है। 'राष्ट्रकवि' जैसी उपाधि का उल्लेख करने से उत्तर और भी प्रभावशाली बनता है।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
(रेखांकित अंश: पर यह न परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय।)
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पद्यांश की रेखांकित पंक्ति का भावार्थ एवं काव्य-सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
Step 2: Detailed Explanation:
व्याख्या: इन पंक्तियों से पूर्व कवि ने आधुनिक मनुष्य की असीम भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। उसने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है और ज्ञान-विज्ञान का भंडार है। परन्तु, रेखांकित पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य की यह भौतिक प्रगति ही उसका सम्पूर्ण परिचय नहीं है और न ही यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि (श्रेय) है। कवि के अनुसार, मनुष्य की वास्तविक महानता केवल भौतिक विजयों में नहीं, बल्कि मानवीय गुणों, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने में है। भौतिक शक्ति प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
Step 3: Final Answer:
रेखांकित अंश में कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की वैज्ञानिक और भौतिक उपलब्धियाँ ही उसकी वास्तविक पहचान या सबसे बड़ी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी सच्ची महानता मानवीय मूल्यों को अपनाने में है।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सका ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह कौन है जिससे आकाश और पृथ्वी की कोई भी चीज छिपी नहीं है।
Step 2: Explanation from the Passage:
पद्यांश की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट लिखा है, "कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश"। यहाँ 'जिससे' सर्वनाम का प्रयोग पहली पंक्ति में वर्णित 'मनुज' (मनुष्य) के लिए किया गया है।
Step 3: Final Answer:
पद्यांश के अनुसार, आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व मनुज (आधुनिक मनुष्य) से अज्ञात नहीं रह सका है।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि संसार के जड़-चेतन पदार्थ मनुष्य को क्यों प्रणाम करते हैं।
Step 2: Explanation from the Passage:
पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में कहा गया है, "यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम / कर रहे जिसको चराचर भक्तियुक्त प्रणाम"। यहाँ 'शिखा उद्दाम' का अर्थ है 'प्रबल या प्रचंड बुद्धि-बल'। 'चराचर' का अर्थ है जड़ और चेतन।
Step 3: Final Answer:
संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ मनुष्य की प्रबल बुद्धि (उद्दाम शिखा) के कारण उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
‘उद्दाम’ और ‘आलोक’ शब्दों के अर्थ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
प्रश्न में 'उद्दाम' और 'आलोक' इन दो शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहा गया है।
Step 2: Meaning of the Words:
(i) उद्दाम: इस शब्द का अर्थ है - 'प्रबल', 'प्रचंड', 'निरंकुश' या 'Unrestrained'।
(ii) आलोक: इस शब्द का अर्थ है - 'प्रकाश', 'उजाला' या 'Light'।
Step 3: Final Answer:
उद्दाम = प्रबल / प्रचंड
आलोक = प्रकाश
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।

उपर्युक्त पद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में दिए गए दूसरे पद्यांश का सन्दर्भ लिखने के लिए कहा गया है।
Step 2: Detailed Explanation:
प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता 'हिरोशिमा' से उद्धृत है।
यह कविता उनके काव्य-संग्रह 'अरी ओ करुणा प्रभामय' में संकलित है। इसमें कवि ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम के हमले की भीषण विभीषिका का मार्मिक चित्रण किया है।
सन्दर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक में संकलित 'अज्ञेय' जी द्वारा रचित 'हिरोशिमा' शीर्षक कविता से लिया गया है।
Step 3: Final Answer:
यह पद्यांश 'अज्ञेय' द्वारा रचित 'हिरोशिमा' नामक कविता से लिया गया है।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत है ? स्पष्ट कीजिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि कविता किस ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करती है।
Step 2: Detailed Explanation:
प्रस्तुत कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नगर पर हुए अणु बम के हमले की विनाशकारी घटना का संकेत है।
स्पष्टीकरण: कविता में 'मानव का रचा हुआ सूरज' अणु बम का प्रतीक है, जिसके विस्फोट ने क्षण भर में 'मानव को भाप बनाकर सोख' लिया। 'झुलसे हुए पत्थरों पर' 'जली हुई छाया' का वर्णन उस भीषण त्रासदी का प्रमाण है, जहाँ मनुष्यों की छायाएँ तक पत्थरों पर अंकित रह गईं। यह सब अणु बम के विध्वंस की ओर स्पष्ट संकेत करता है।
Step 3: Final Answer:
इस कविता में हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट की घटना का संकेत है, जहाँ मनुष्य द्वारा निर्मित बम ने ही मनुष्य का संहार किया और उसके अमानवीय कृत्य के निशान पत्थरों पर जलती हुई छाया के रूप में आज भी साक्षी हैं।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
‘मानव का रचा हुआ सूरज’ किसे कहा गया है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में 'मानव का रचा हुआ सूरज' इस काव्यात्मक उक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मानव का रचा हुआ सूरज' अणु बम (Atomic Bomb) को कहा गया है। जिस प्रकार सूरज अपार प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार अणु बम के विस्फोट से भी सूरज के समान ही तीव्र प्रकाश और विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। चूँकि इस बम का निर्माण मनुष्य ने ही किया था, इसलिए कवि ने इसे 'मानव का रचा हुआ सूरज' कहा है।
Step 3: Final Answer:
'मानव का रचा हुआ सूरज' अणु बम को कहा गया है।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
मानव जन की छायाएँ लम्बी हो हो कर क्यों नहीं मिटीं ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य की छायाएँ लंबी होकर भी क्यों नहीं मिटीं।
Step 2: Detailed Explanation:
मानव जन की छायाएँ लंबी होकर इसलिए नहीं मिटीं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से बनी सामान्य छायाएँ नहीं थीं। वे अणु बम के विस्फोट की तीव्र ऊष्मा और प्रकाश से झुलसे हुए पत्थरों और सड़कों पर अंकित हो गई थीं। मनुष्य स्वयं तो भाप बनकर उड़ गए, परन्तु उनकी छायाएँ उस महाविनाश के स्थायी साक्षी के रूप में पत्थरों पर 'लिख' गईं। इसलिए वे अमिट हो गईं।
Step 3: Final Answer:
मानव जन की छायाएँ इसलिए नहीं मिटीं क्योंकि वे अणु बम के विस्फोट से पत्थरों पर स्थायी रूप से अंकित हो गई थीं और उस त्रासदी की अमिट साक्षी बन गईं।
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
‘गच’ और ‘साखी’ शब्दों के अर्थ लिखिए।
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
प्रश्न में 'गच' और 'साखी' इन दो शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहा गया है।
Step 2: Meaning of the Words:
(i) गच: इस शब्द का अर्थ है - 'पक्की सतह', 'फर्श' या 'सड़क की ऊपरी परत'। (Pavement)
(ii) साखी: यह 'साक्षी' का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है - 'गवाह', 'साक्ष्य' या 'प्रमाण'। (Witness/Testimony)
Step 3: Final Answer:
गच = फर्श / पक्की सतह
साखी = गवाह / साक्षी
Quick Tip: व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश से पहले की पंक्तियों का संदर्भ अवश्य दें। इससे व्याख्या अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। यहाँ भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के बीच का द्वंद्व ही मुख्य भाव है।
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए : ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ को अपने साहित्य का आधार बनाया। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, सरस और प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्यांकन किया।
प्रमुख रचनाएँ:
निबंध: 'अशोक के फूल', 'कुटज'
उपन्यास: 'बाणभट्ट की आत्मकथा', 'पुनर्नवा'
आलोचना: 'हिन्दी साहित्य की भूमिका', 'कबीर'
Quick Tip: साहित्यिक परिचय लिखते समय, लेखक की साहित्यिक विधा (निबंधकार, उपन्यासकार आदि), उनकी भाषा-शैली की विशेषताएँ और साहित्य में उनके योगदान का संक्षिप्त उल्लेख करें। रचनाओं को विधा के अनुसार वर्गीकृत करके लिखना अधिक प्रभावशाली होता है।
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए : ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
वासुदेवशरण अग्रवाल
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल हिन्दी साहित्य के एक प्रकांड विद्वान्, निबंधकार तथा भारतीय संस्कृति, पुरातत्त्व और कला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति और दर्शन का गहन एवं प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित और विषय के अनुकूल है।
प्रमुख कृतियाँ: 'पृथ्वी-पुत्र', 'कल्पवृक्ष', 'भारत की एकता', 'माता भूमि' (निबंध-संग्रह) तथा 'पाणिनीकालीन भारतवर्ष' (शोध-ग्रंथ)।
Quick Tip: वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे विद्वान् लेखक का परिचय देते समय, उनके ज्ञान के क्षेत्र (पुरातत्त्व, भारतीय संस्कृति) का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उनके लेखन का आधार है।
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए : ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक प्रेरक लेखक भी थे। उन्होंने अपने लेखन को देश के युवाओं को मार्गदर्शन देने और उन्हें प्रेरित करने का माध्यम बनाया। उनकी भाषा सरल, व्यावहारिक और ओजपूर्ण है।
प्रमुख कृतियाँ: उनकी आत्मकथा 'अग्नि की उड़ान' (Wings of Fire) ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं- 'इण्डिया 2020', 'तेजस्वी मन' (Ignited Minds), तथा 'मेरे सपनों का भारत'।
Quick Tip: डॉ. कलाम जैसे व्यक्तित्व का साहित्यिक परिचय देते समय, उनके मूल पेशे (वैज्ञानिक, राष्ट्रपति) का उल्लेख करते हुए उनके साहित्यिक योगदान (प्रेरक लेखन) को रेखांकित करें। यह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है।
निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखें :
महादेवी वर्मा
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
'आधुनिक युग की मीरा' कही जाने वाली महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। उनके काव्य में वेदना, विरह-अनुभूति और रहस्यवादी स्वर प्रमुख है। वे एक श्रेष्ठ गद्य-लेखिका भी थीं, जिनके रेखाचित्र और संस्मरण अद्वितीय हैं। उनकी भाषा तत्सम प्रधान, कोमल और संगीतात्मक है।
प्रमुख कृतियाँ:
काव्य: 'नीहार', 'नीरजा', 'दीपशिखा' और 'यामा' (ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त)
गद्य: 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ'
Quick Tip: जब कोई साहित्यकार पद्य और गद्य दोनों में समान रूप से कुशल हो, तो परिचय में दोनों का उल्लेख करें। इससे उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की समग्रता का पता चलता है।
निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखें :
रामधारी सिंह ‘दिनकर’
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' प्रगतिवादी काव्यधारा के एक ओजस्वी कवि हैं। उन्हें 'अनल कवि' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति का स्वर प्रमुख है, तो वहीं 'उर्वशी' जैसी रचनाओं में प्रेम और दर्शन की गहराई भी है। वे एक श्रेष्ठ गद्यकार भी थे।
प्रमुख कृतियाँ: 'कुरुक्षेत्र', 'रश्मिरथी', 'हुंकार' (काव्य); 'उर्वशी' (काव्य-नाटक, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त); 'संस्कृति के चार अध्याय' (गद्य)।
Quick Tip: 'दिनकर' का परिचय देते समय उन्हें 'राष्ट्रकवि' और 'अनल कवि' जैसी उपाधियों से संबोधित करें। उनकी पुरस्कृत रचनाओं ('उर्वशी' पर ज्ञानपीठ और 'संस्कृति के चार अध्याय' पर साहित्य अकादमी) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखें :
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’
View Solution
Step 1: साहित्यिक परिचय और रचनाएँ (Literary Introduction and Works):
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' हिन्दी में 'प्रयोगवाद' के प्रवर्तक और 'तार सप्तक' के संपादक थे। उन्होंने कविता में नए बिम्बों, प्रतीकों और भाषा-शिल्प का प्रयोग किया। उनके साहित्य में वैयक्तिक चेतना और बौद्धिकता का प्रभाव है। वे कवि के साथ-साथ सफल उपन्यासकार और निबंधकार भी थे।
प्रमुख कृतियाँ:
काव्य: 'हरी घास पर क्षण भर', 'कितनी नावों में कितनी बार' (ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त)
उपन्यास: 'शेखर: एक जीवनी', 'नदी के द्वीप'
Quick Tip: 'अज्ञेय' जैसे किसी साहित्यिक आंदोलन के प्रवर्तक का परिचय देते समय, उस आंदोलन (जैसे- प्रयोगवाद) और उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य (जैसे- तार सप्तक का संपादन) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
‘पंचलाइट’ कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए । ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
View Solution
Step 1: कहानी का उद्देश्य (Objective of the Story):
फणीश्वरनाथ 'रेणु' द्वारा रचित 'पंचलाइट' एक आंचलिक कहानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, रूढ़ियों और जातिगत भेदभाव पर व्यंग्य करना है। लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े-बड़े जातिगत बंधन और मान्यताएँ भी टूट जाती हैं। कहानी यह संदेश देती है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके गुण और काबिलियत से होनी चाहिए। गोधन के माध्यम से लेखक ने यह स्थापित किया है कि व्यक्ति का हुनर समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।
Quick Tip: 'दिनकर' का परिचय देते समय उन्हें 'राष्ट्रकवि' और 'अनल कवि' जैसी उपाधियों से संबोधित करें। उनकी पुरस्कृत रचनाओं ('उर्वशी' पर ज्ञानपीठ और 'संस्कृति के चार अध्याय' पर साहित्य अकादमी) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
‘लाटी’ कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए । ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
View Solution
Step 1: कहानी का उद्देश्य (Objective of the Story):
शिवानी द्वारा रचित 'लाटी' कहानी का उद्देश्य प्रेम, प्रतीक्षा और त्याग के मर्म को दर्शाना है। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम का आघात कितना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि प्रिय की खुशी के लिए निःस्वार्थ भाव से त्याग और सेवा करने का नाम है। यह कहानी पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विरह की मार्मिक पीड़ा को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है।
Quick Tip: 'दिनकर' का परिचय देते समय उन्हें 'राष्ट्रकवि' और 'अनल कवि' जैसी उपाधियों से संबोधित करें। उनकी पुरस्कृत रचनाओं ('उर्वशी' पर ज्ञानपीठ और 'संस्कृति के चार अध्याय' पर साहित्य अकादमी) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
‘बहादुर’ कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए । ( अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द )
View Solution
Step 1: कहानी का सारांश (Summary of the Story):
'बहादुर' अमरकांत द्वारा लिखी एक कहानी है जो एक नेपाली लड़के 'दिल बहादुर' के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अपने घर से भागकर एक मध्यमवर्गीय परिवार में नौकर लग जाता है। प्रारंभ में उसे बहुत स्नेह मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे परिवार के लोग उस पर रौब जमाने लगते हैं और छोटी-छोटी बातों पर उसे पीटते हैं। अंत में, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है, जिससे दुखी होकर वह बिना अपना वेतन लिए घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद परिवार के लोग अपनी गलती पर पछताते हैं।
Quick Tip: 'दिनकर' का परिचय देते समय उन्हें 'राष्ट्रकवि' और 'अनल कवि' जैसी उपाधियों से संबोधित करें। उनकी पुरस्कृत रचनाओं ('उर्वशी' पर ज्ञानपीठ और 'संस्कृति के चार अध्याय' पर साहित्य अकादमी) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
‘श्रवणकुमार’ खण्डकाव्य के आधार पर ‘दशरथ’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।
View Solution
Step 1: पात्र का चरित्र-चित्रण (Character Sketch):
'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य में दशरथ अयोध्या के न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा हैं। वे एक कुशल धनुर्धर हैं, किन्तु आखेट के व्यसन के कारण वे अनजाने में श्रवणकुमार का वध कर देते हैं। अपनी भूल का ज्ञान होने पर वे अत्यंत पश्चाताप करते हैं और स्वयं को अपराधी मानते हैं। वे श्रवणकुमार के माता-पिता से क्षमा माँगते हैं और शाप को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, दशरथ का चरित्र एक मानवीय भूल करने वाले और उस पर पश्चाताप करने वाले आदर्श राजा का चरित्र है।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण करते समय, पात्र के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों (जैसे- दशरथ का आखेट-प्रेम और उनका पश्चाताप) का उल्लेख करने से उत्तर संतुलित बनता है।
‘श्रवणकुमार’ खण्डकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए।
View Solution
Step 1: सर्ग की कथा (Story of the Canto):
'श्रवणकुमार' खण्डकाव्य के चतुर्थ सर्ग का शीर्षक 'दशरथ' है। इसमें राजा दशरथ के पश्चाताप का मार्मिक वर्णन है। अपने बाण से घायल श्रवणकुमार को देखकर वे अत्यंत दुःखी होते हैं। श्रवणकुमार उनसे अपने प्यासे माता-पिता को जल पिलाने का अनुरोध कर अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ जल लेकर जब आश्रम पहुँचते हैं और श्रवणकुमार के माता-पिता को पूरी घटना बताते हैं, तो वे विलाप करने लगते हैं। यह सर्ग दशरथ की मानसिक पीड़ा और करुणा से भरा हुआ है।
Quick Tip: जब किसी खण्डकाव्य के विशेष सर्ग (अध्याय) के बारे में पूछा जाए, तो अपना उत्तर केवल उसी सर्ग की घटनाओं तक सीमित रखें। पूरी कहानी लिखने से बचें।
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य का कथानक संक्षिप्त रूप से अपने शब्दों में लिखिए।
View Solution
Step 1: कथानक (Plot):
'रश्मिरथी' की कथा महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें कर्ण के जन्म से लेकर वीरगति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। सूत-पुत्र होने के कारण समाज द्वारा अपमानित कर्ण को दुर्योधन सम्मान देता है, जिससे कर्ण उसका अनन्य मित्र बन जाता है। श्रीकृष्ण के समझाने पर भी वह मित्र-धर्म निभाने के लिए पांडव पक्ष में जाने से इनकार कर देता है। अंत में, वह अपना कवच-कुण्डल दान कर महाभारत के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है।
Quick Tip: कथावस्तु लिखते समय कहानी की मुख्य घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करें। अनावश्यक विस्तार से बचें और शब्द-सीमा का ध्यान रखते हुए केवल सारगर्भित बातें ही लिखें।
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर ‘कर्ण’ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
View Solution
Step 1: नायक की विशेषताएँ (Characteristics of the Hero):
'रश्मिरथी' के नायक कर्ण एक महान योद्धा, सच्चे मित्र और अद्वितीय दानवीर हैं। वे सामाजिक तिरस्कार सहकर भी अपने पौरुष के बल पर श्रेष्ठता अर्जित करते हैं। दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता अटूट है। वे अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते। श्रीकृष्ण के प्रलोभनों को ठुकराकर वे मित्र-धर्म निभाते हैं। अपना कवच-कुण्डल दान देकर वे 'दानवीर कर्ण' कहलाते हैं। उनका चरित्र त्याग, वीरता और मित्रता का प्रतीक है।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण करते समय, पात्र के गुणों को शीर्षकों (जैसे- महान योद्धा, दानवीर) में विभाजित करके उनके बारे में एक-एक पंक्ति लिखना उत्तर को अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है।
‘मुक्तियज्ञ’ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
View Solution
Step 1: सारांश (Summary):
'मुक्तियज्ञ' खण्डकाव्य की कथावस्तु महात्मा गाँधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित है। कथा का आरम्भ अंग्रेजों के नमक कानून से होता है। गाँधीजी इस काले कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दाण्डी तक की पदयात्रा करते हैं। इसके बाद वे दलितों के उद्धार के लिए भी संघर्ष करते हैं। अंत में, 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के फलस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिलती है। यह काव्य भारत की मुक्ति के लिए किए गए यज्ञ की गाथा है।
Quick Tip: सारांश लिखते समय 'मुक्तियज्ञ' शब्द के अर्थ (मुक्ति के लिए यज्ञ) को ध्यान में रखें। अपनी प्रस्तुति को गाँधीजी के स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के चारों ओर केंद्रित करें, जिसमें 'नमक सत्याग्रह' एक महत्वपूर्ण आहुति है।
‘मुक्तियज्ञ’ के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए।
View Solution
Step 1: नायक का चरित्र-चित्रण (Character Sketch of the Hero):
'मुक्तियज्ञ' के नायक महात्मा गाँधी एक अलौकिक महापुरुष हैं, जिनमें मानवीय गुणों का समावेश है। वे सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक हैं तथा इन्हीं शस्त्रों से ब्रिटिश शासन का सामना करते हैं। वे समाज से छुआछूत जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैं और दलितों का उद्धार करते हैं। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं और एक दृढ़-निश्चयी नेता के रूप में भारत को स्वतंत्रता दिलाते हैं।
Quick Tip: गाँधीजी जैसे महान व्यक्तित्व का चरित्र-चित्रण करते समय, उनके मानवीय और नैतिक गुणों (जैसे- सत्य, अहिंसा, दलितोद्धार) पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खण्डकाव्य में इन्हीं गुणों को प्रमुखता दी गई है।
‘त्यागपथी’ खण्डकाव्य के आधार पर ‘राज्यश्री’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।
View Solution
Step 1: पात्र का चरित्र-चित्रण (Character Sketch):
'त्यागपथी' में राज्यश्री एक आदर्श भारतीय नारी हैं। वे त्याग, तपस्या और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। अपने पति की मृत्यु और भाई की हत्या के बाद वे अनेक कष्ट सहती हैं, किन्तु अपना धैर्य नहीं खोतीं। वे अपने भाई हर्षवर्धन के साथ मिलकर शासन करती हैं और अपना जीवन प्रजा-सेवा में समर्पित कर देती हैं। उनका चरित्र दुःख सहकर भी लोक-कल्याण के मार्ग पर चलने वाली एक तपस्विनी का चरित्र है।
Quick Tip: किसी नारी पात्र का चरित्र-चित्रण करते समय, भारतीय संस्कृति में नारी के आदर्शों (त्याग, सेवा, करुणा) को आधार बनाना उत्तर को प्रभावी बनाता है, जैसा कि राज्यश्री के चरित्र में है।
‘त्यागपथी’ खण्डकाव्य की कथा का सारांश लिखिए।
View Solution
Step 1: सारांश (Summary):
'त्यागपथी' की कथा कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। कहानी उनके पिता की मृत्यु, भाई राज्यवर्धन की हत्या और बहन राज्यश्री के अपहरण से आरम्भ होती है। हर्षवर्धन कठिन परिस्थितियों में शासन संभालते हैं और अपनी बहन को खोजकर कन्नौज का राज्य भी संभालते हैं। वे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और अपने जीवन में त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रयाग में अपना सर्वस्व दान कर देते हैं।
Quick Tip: 'त्यागपथी' की कथा का सारांश लिखते समय, हर्षवर्धन के जीवन के 'त्याग' वाले पक्ष को उजागर करें, जैसे राज्य का त्याग, सुखों का त्याग और अंत में सर्वस्व का त्याग। यही इस काव्य का मूल भाव है।
‘आलोकवृत्त’ खण्डकाव्य के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए।
View Solution
Step 1: नायक का चरित्र-चित्रण (Character Sketch of the Hero):
'आलोकवृत्त' के नायक महात्मा गाँधी एक युगपुरुष हैं, जिन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व से भारत को नई दिशा दी। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और इन्हीं सिद्धांतों के बल पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। वे दृढ़-संकल्प वाले व्यक्ति हैं, जो एक बार निश्चय कर लेने पर पीछे नहीं हटते। वे केवल भारत ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता से प्रेम करने वाले विश्व-मानव हैं। उनका चरित्र त्याग, देश-प्रेम और मानवता का संदेश देता है।
Quick Tip: 'आलोकवृत्त' के नायक के रूप में गाँधीजी का चरित्र-चित्रण करते समय, उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर प्रकाश डालें जो सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणास्रोत हैं, क्योंकि 'आलोकवृत्त' केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्रकाश का प्रतीक है।
‘आलोकवृत्त’ खण्डकाव्य के आधार पर असहयोग आन्दोलन की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए।
View Solution
Step 1: कथावस्तु (Plot):
'आलोकवृत्त' खण्डकाव्य में असहयोग आन्दोलन का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। गाँधीजी के आह्वान पर पूरा देश अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट हो जाता है। विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज छोड़ देते हैं, वकील वकालत का त्याग कर देते हैं और लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाते हैं। यह आन्दोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। चौरी-चौरा की हिंसक घटना से दुखी होकर गाँधीजी यह आन्दोलन वापस ले लेते हैं, जो उनके अहिंसा के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
Quick Tip: किसी विशेष घटना या आंदोलन के बारे में पूछा जाए, तो अपना उत्तर उसी घटना पर केंद्रित रखें। असहयोग आन्दोलन के संदर्भ में, इसके सकारात्मक पक्ष (देशव्यापी एकता) और इसके स्थगन के कारण (चौरी-चौरा) दोनों का उल्लेख महत्वपूर्ण है।
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए।
View Solution
Step 1: कथावस्तु (Plot):
'सत्य की जीत' की कथावस्तु महाभारत के द्यूत-प्रसंग पर आधारित है। कौरवों द्वारा आयोजित द्यूत-क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी दाँव पर लगाकर हार जाते हैं। दुःशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके उसे अपमानित करने का प्रयास करता है। इसके विरोध में द्रौपदी सभासदों से न्याय की माँग करती है और धर्म-अधर्म पर तर्कपूर्ण प्रश्न उठाती है। उसके तर्कों और सत्य के तेज के आगे सभी मौन हो जाते हैं। अंत में, द्रौपदी के सत्य और सतीत्व की ही जीत होती है।
Quick Tip: कथावस्तु लिखते समय यह स्पष्ट करें कि कहानी का केंद्रीय संघर्ष क्या है। 'सत्य की जीत' में केंद्रीय संघर्ष द्रौपदी का अपने सम्मान के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किया गया तार्किक और नैतिक संघर्ष है।
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर ‘दुःशासन’ का चरित्र-चित्रण कीजिए।
View Solution
Step 1: पात्र का चरित्र-चित्रण (Character Sketch):
'सत्य की जीत' खण्डकाव्य में दुःशासन एक खलनायक है। वह अविवेकी, दुराचारी और अहंकारी है। वह अपने बड़े भाई दुर्योधन के गलत आदेशों का आँख बंद करके पालन करता है। उसमें नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वह भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने जैसा घृणित कार्य करता है। वह शक्ति के मद में चूर है और धर्म-अधर्म का विचार नहीं करता। उसका चरित्र पाशविक प्रवृत्ति और विवेकहीनता का प्रतीक है।
Quick Tip: किसी खलनायक का चरित्र-चित्रण करते समय, उसके अवगुणों (जैसे- अहंकार, अविवेक, दुराचार) को स्पष्ट रूप से बताएं और काव्य में वर्णित उसके किसी एक प्रमुख दुष्कर्म (जैसे- द्रौपदी चीरहरण) का उदाहरण दें।
दिये गये संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससन्दर्भ हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच-मैत्रेयि ! उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि । ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति । मैत्रेयी उवाच-यdiyं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, तत् किं तेनाहममृता स्यामिति । याज्ञवल्क्य उवाच-नेति । यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् । अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति । सा मैत्रेयी उवाच-येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम् । यदेव भगवान् केवलममृतत्वसाधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि । याज्ञवल्क्य उवाच-प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाषसे । एहि उपविश व्याख्यास्यामिते अमृतत्वसाधनम् ।
View Solution
Step 1: सन्दर्भ (Context):
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के 'संस्कृत दिग्दर्शिका' खण्ड में संकलित 'आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः' नामक पाठ से उद्धृत है।
Step 2: हिन्दी अनुवाद (Hindi Translation):
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा - "हे मैत्रेयी! मैं इस (गृहस्थ) स्थान से ऊपर (संन्यास आश्रम में) जाने वाला हूँ। अतः तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बँटवारा कर दूँ।" मैत्रेयी ने कहा - "यदि यह सम्पूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊँगी?" याज्ञवल्क्य ने कहा - "नहीं।" "जैसा साधन-सम्पन्न (धनी) लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है।" उस मैत्रेयी ने कहा - "जिससे मैं अमर नहीं होऊँगी, उसे लेकर मैं क्या करूँगी। आप जो केवल अमरता का साधन जानते हैं, वही मुझे बताएँ।" याज्ञवल्क्य ने कहा - "तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। आओ, बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा।"
Quick Tip: अनुवाद करते समय संवाद के भाव को बनाए रखें। मैत्रेयी के प्रश्नों में भौतिक संपत्ति के प्रति वैराग्य और अमरता (ज्ञान) के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रमुख है, इसे अनुवाद में स्पष्ट करें।
दिये गये संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससन्दर्भ हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
हिन्दी-संस्कृताङ्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत् । हिन्दी-हिन्दु-हिन्दुस्थानानामुत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नमकरोत् । शिक्षयैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयस्य संस्थापनमकरोत् । अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत् जनाश्च महत्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रायच्छन्, तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति ।
View Solution
Step 1: सन्दर्भ (Context):
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के 'संस्कृत दिग्दर्शिका' खण्ड में संकलित 'महामना मालवीयः' नामक पाठ से लिया गया है।
Step 2: हिन्दी अनुवाद (Hindi Translation):
हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका (मालवीय जी का) समान अधिकार था। हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरन्तर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन माँगा और लोगों ने इस महान ज्ञान-यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित है।
Quick Tip: अनुवाद करते समय विशेष नामों (जैसे- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) और अवधारणाओं (जैसे- ज्ञानयज्ञ) को स्पष्ट रूप से लिखें। गद्यांश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए वाक्यों को सही क्रम में जोड़ें।
दिये गये पद्यांशों में से किसी एक का ससन्दर्भ हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ।।
View Solution
Step 1: सन्दर्भ (Context):
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य-पुस्तक के 'संस्कृत दिग्दर्शिका' खण्ड में संकलित 'सुभाषितरत्नानि' नामक पाठ से उद्धृत है।
Step 2: हिन्दी अनुवाद (Hindi Translation):
पीठ-पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय (मीठा) बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे उस विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है जिसके मुख पर दूध लगा हो।
Quick Tip: इस श्लोक में उपमा अलंकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा दी गई है। अनुवाद करते समय उपमा ('विषकुम्भं पयोमुखम्') को स्पष्ट करते हुए मित्र के कपटपूर्ण व्यवहार को उजागर करें।
दिये गये पद्यांशों में से किसी एक का ससन्दर्भ हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
विरलविरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः ।
मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नमभून्नभः ।।
अपसरति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिव दुर्जनः ।
व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीः अनुद्यमिनामिव ।।
View Solution
Step 1: सन्दर्भ (Context):
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य-पुस्तक के 'संस्कृत दिग्दर्शिका' खण्ड में संकलित 'सुभाषितरत्नानि' नामक पाठ से लिया गया है।
Step 2: हिन्दी अनुवाद (Hindi Translation):
(शरद ऋतु के आगमन पर) कलियुग में सज्जनों की भाँति, बड़े-बड़े तारे आकाश में कहीं-कहीं ही (विरले) दिखाई दे रहे हैं।
मुनि के मन की भाँति, आकाश सब ओर से स्वच्छ हो गया है।
सज्जनों के हृदय से दुष्टों की भाँति, अन्धकार दूर हो रहा है।
और उद्यमहीन (आलसी) व्यक्ति के धन की भाँति, रात्रि शीघ्रता से समाप्त हो रही है।
Quick Tip: इस श्लोक में अनेक उपमा अलंकार हैं। अनुवाद करते समय प्रत्येक उपमा (जैसे - 'कलाविव सज्जनाः', 'मन इव मुनेः') को स्पष्ट रूप से समझाएं। यह श्लोक शरद ऋतु के प्रातःकाल का सुन्दर वर्णन करता है।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :
दाँत खट्टे करना
View Solution
Step 1: अर्थ (Meaning):
दाँत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है - बुरी तरह पराजित करना या हरा देना।
Step 2: वाक्य प्रयोग (Usage in a sentence):
भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के दाँत खट्टे कर दिए थे।
Quick Tip: मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते समय, वाक्य ऐसा बनाएं जिससे मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :
दाल में काला होना
View Solution
Step 1: अर्थ (Meaning):
दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है - किसी गड़बड़ी का संदेह होना या कुछ रहस्य छिपा होना।
Step 2: वाक्य प्रयोग (Usage in a sentence):
रात में चौकीदार का अचानक गायब हो जाना और सुबह चोरी हो जाना, मुझे तो इस दाल में कुछ काला लगता है।
Quick Tip: इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी घटना या व्यवहार पर शक होता है और लगता है कि सच्चाई कुछ और है जो छिपाई जा रही है।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :
नाकों चने चबाना
View Solution
Step 1: अर्थ (Meaning):
नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ है - बहुत अधिक परेशान करना या बहुत तंग करना। (ध्यान दें: 'चबवाना' होता है, 'चबाना' नहीं। 'नाकों चने चबाना' का अर्थ होता है - बहुत कष्ट झेलना।)
(प्रश्न में दिए गए रूप 'चबाना' के अनुसार अर्थ: बहुत कष्ट झेलना)
सही रूप 'नाकों चने चबवाना' का अर्थ: बहुत परेशान करना।
Step 2: वाक्य प्रयोग (Usage in a sentence):
(अर्थ 'बहुत परेशान करना' के अनुसार): शिवाजी ने अपनी वीरता से मुगलों को नाकों चने चबवा दिए थे।
Quick Tip: 'नाकों चने चबाना' और 'नाकों चने चबवाना' में अंतर है। 'चबाना' का अर्थ है खुद कष्ट सहना, जबकि 'चबवाना' का अर्थ है दूसरे को कष्ट देना। प्रश्न में प्रायः 'चबवाना' का भाव ही अभीष्ट होता है।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :
पौ बारह होना
View Solution
Step 1: अर्थ (Meaning):
पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है - चारों ओर से लाभ ही लाभ होना, खूब लाभ होना।
Step 2: वाक्य प्रयोग (Usage in a sentence):
जब से रमेश ने कपड़ों का नया व्यापार शुरू किया है, तब से तो उसकी पौ बारह हो रही है।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसा होता है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में गद्यांश के आधार पर सज्जन या महात्मा पुरुषों के व्यवहार के बारे में पूछा गया है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है: "सज्जन या महात्मा ठीक इसके विपरीत होते हैं। उनका ध्यान दूसरों के अवगुणों के बजाय केवल गुणों पर जाता है।"
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, सज्जन या महात्माओं का आचरण दुर्जनों के विपरीत होता है। वे दूसरों की बुराइयों पर ध्यान न देकर उनके गुणों को ही देखते हैं।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कौन से व्यक्ति देवता की कोटि में आते हैं ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार, किन व्यक्तियों को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश की चौथी पंक्ति में इसका सीधा उत्तर दिया गया है: "कोई भी बुराई न होने पर व्यक्ति देवता की कोटि में आ जाता है।"
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, जिन व्यक्तियों में कोई भी बुराई नहीं होती है, वे देवता की कोटि में आते हैं।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में अपनी उन्नति करने का सबसे अच्छा रास्ता पूछा गया है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है: "आत्मनिरीक्षण आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।"
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, आत्मोन्नति (अपनी उन्नति) का सर्वश्रेष्ठ मार्ग आत्मनिरीक्षण (अपने मन की परख करना) है।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आधुनिकता की पहचान लेखक के अनुसार किन-किन तथ्यों से मिलकर होती है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार आधुनिकता किन चीजों से पहचानी जाती है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश के अनुसार, आधुनिकता की पहचान निम्नलिखित तथ्यों से मिलकर होती है:
नैतिकता, सौन्दर्य बोध और अध्यात्म का होना।
औद्योगीकरण और साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार।
एक गतिशील और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था।
सामंती और मध्यकालीन सामाजिक संरचनाओं का समाप्त होना।
जातिप्रथा, गोत्रवाद, अंधविश्वास और संकीर्णता से मुक्ति।
Step 3: Final Answer:
लेखक के अनुसार, आधुनिकता की पहचान नैतिकता, सौन्दर्य बोध, अध्यात्म, औद्योगीकरण, साक्षरता, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा जातिप्रथा और अंधविश्वास से मुक्त समाज जैसे तथ्यों से मिलकर होती है।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आधुनिक समाज को मुक्त कहने का क्या अभिप्राय है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक समाज को 'मुक्त' (free/open) कहने का क्या मतलब है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश के अनुसार, आधुनिक समाज में उन्मुक्तता (खुलापन) होती है। इसका अभिप्राय ऐसे समाज से है जो पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों से आजाद हो। लेखक के अनुसार, जो समाज जातिप्रथा, गोत्रवाद, अंधविश्वास, गतानुगतिकता (पुरानी लीक पर चलना) और संकीर्णता से पीड़ित है, वह आधुनिक नहीं हो सकता। अतः, आधुनिक समाज को मुक्त कहने का अभिप्राय है कि वह इन सभी सामाजिक बुराइयों और संकीर्णताओं से मुक्त होता है।
Step 3: Final Answer:
आधुनिक समाज को मुक्त कहने का अभिप्राय है कि वह जातिप्रथा, गोत्रवाद, अंधविश्वास और संकीर्णता जैसी सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होता है।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कौन समाज जातिप्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन-सा समाज जातिप्रथा और गोत्रवाद से ग्रस्त है।
Step 2: Explanation from the Passage:
गद्यांश में लेखक उस समाज का वर्णन करते हैं जो आधुनिक नहीं है। उसी के संदर्भ में वे कहते हैं, "वह जातिप्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है तथा अंधविश्वासी गतानुगतिक एवं संकीर्ण है।" लेखक यह टिप्पणी भारतीय समाज के संदर्भ में कर रहे हैं जिसे वे आधुनिक बनाने का प्रयत्न करते हुए नहीं देखते।
Step 3: Final Answer:
गद्यांश के अनुसार, वह समाज जातिप्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है जो आधुनिक नहीं है, जो अंधविश्वासी, पुरानी लीक पर चलने वाला और संकीर्ण है।
Quick Tip: यह मुहावरा अत्यधिक लाभ या बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित शब्द-युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए :
पुरुष-परुष
View Solution
Step 1: Understanding the Words:
यह प्रश्न श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों पर आधारित है, जो सुनने में समान लगते हैं परन्तु उनके अर्थ भिन्न होते हैं।
पुरुष: इस शब्द का अर्थ 'आदमी', 'नर' या 'व्यक्ति' (Man) होता है।
परुष: इस शब्द का अर्थ 'कठोर' या 'कर्कश' (Harsh/Hard) होता है।
Step 2: Matching with Options:
दिए गए अर्थों के अनुसार, सही क्रम 'आदमी' और 'कठोर' है।
विकल्प (B) में यह क्रम सही दिया गया है।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'पुरुष-परुष' का सही अर्थ है 'आदमी और कठोर'। विकल्प (B) सही है।
Quick Tip: 'ष' और 'श' के सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दें। 'परुष' शब्द का प्रयोग अक्सर वाणी के लिए होता है, जैसे - परुष वचन।
निम्नलिखित शब्द-युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए :
तरंग-तुरंग
View Solution
Step 1: Understanding the Words:
यह प्रश्न भी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों पर आधारित है।
तरंग: इस शब्द का अर्थ 'लहर' (Wave) होता है।
तुरंग: इस शब्द का अर्थ 'घोड़ा' या 'अश्व' (Horse) होता है।
Step 2: Matching with Options:
दिए गए अर्थों के अनुसार, सही क्रम 'लहर' और 'घोड़ा' है।
विकल्प (B) में यह क्रम सही दिया गया है।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'तरंग-तुरंग' का सही अर्थ है 'लहर और घोड़ा'। विकल्प (B) सही है।
Quick Tip: संस्कृत मूल के पर्यायवाची शब्दों को याद करना ऐसे प्रश्नों में बहुत सहायक होता है। 'तुरंग' घोड़े का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द है।
निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए :
(i) अनन्त
(ii) अक्षर
(iii) अक्षत
(iv) अक्ष
View Solution
Step 1: Understanding the Question:
इस प्रश्न में दिए गए शब्दों में से किसी एक के दो अलग-अलग अर्थ (अनेकार्थी शब्द) लिखने हैं। यहाँ सभी के अर्थ दिए जा रहे हैं।
Step 2: Meanings of the Words:
(i) अनन्त: (अन् + अन्त)
1. जिसका अन्त न हो/असीम (Endless)
2. आकाश (Sky)
3. विष्णु (Lord Vishnu)
(ii) अक्षर: (अ + क्षर)
1. जिसका नाश न हो/अविनाशी (Imperishable)
2. वर्ण (Letter of alphabet)
3. ब्रह्म/ईश्वर (The Supreme Being)
(iii) अक्षत:
1. बिना टूटा हुआ/सम्पूर्ण (Unbroken)
2. पूजा में प्रयुक्त होने वाले साबुत चावल (Rice used in worship)
(iv) अक्ष:
1. आँख (Eye)
2. धुरी (Axis)
3. पासा (Dice)
Quick Tip: अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान भाषा की गहरी समझ के लिए आवश्यक है। शब्दों के यौगिक अर्थ (जैसे अनन्त, अक्षर) को समझने से उनके अर्थों का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सही शब्द का चयन करके लिखिए :
जिसके पास कुछ न हो -
View Solution
N/A
जो कहा न जा सके -
View Solution
'जो कहा न जा सके' वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकथनीय (अ + कथनीय = जो कहने योग्य न हो)।
'अनकहा' का अर्थ है 'जो कहा नहीं गया है'।
अतः, सही विकल्प (C) है।
Quick Tip: वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनते समय, शब्दों के सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दें। 'अकथनीय' का अर्थ है जिसे व्यक्त करना संभव न हो (जैसे- अकथनीय सौंदर्य), जबकि 'अनकहा' का अर्थ है जिसे जानबूझकर या अवसर न मिलने पर कहा न गया हो।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए :
(i) मैं सकुशलपूर्वक हूँ ।
(ii) पाँच रेलवे के कर्मचारी पकड़े गये ।
(iii) उसका प्राण निकलने वाला है ।
(iv) आप प्रातःकाल के समय आइएगा ।
View Solution
(i) अशुद्ध वाक्य: मैं सकुशलपूर्वक हूँ।
शुद्ध वाक्य: मैं सकुशल हूँ। या मैं कुशलपूर्वक हूँ।
(कारण: 'सकुशल' और 'पूर्वक' दोनों का एक साथ प्रयोग अनावश्यक है। 'सकुशल' में 'स' उपसर्ग का अर्थ ही 'सहित' है।)
(ii) अशुद्ध वाक्य: पाँच रेलवे के कर्मचारी पकड़े गये।
शुद्ध वाक्य: रेलवे के पाँच कर्मचारी पकड़े गये।
(कारण: पदक्रम संबंधी अशुद्धि। विशेषण (पाँच) को विशेष्य (कर्मचारी) के पास होना चाहिए।)
(iii) अशुद्ध वाक्य: उसका प्राण निकलने वाला है।
शुद्ध वाक्य: उसके प्राण निकलने वाले हैं।
(कारण: 'प्राण' शब्द हिन्दी में नित्य बहुवचन होता है, इसलिए क्रिया और सर्वनाम भी बहुवचन में होंगे।)
(iv) अशुद्ध वाक्य: आप प्रातःकाल के समय आइएगा।
शुद्ध वाक्य: आप प्रातःकाल आइएगा। या आप प्रातः के समय आइएगा।
(कारण: 'प्रातःकाल' में 'काल' शब्द पहले से ही है, अतः 'समय' का प्रयोग अनावश्यक है।)
Quick Tip: वाक्य शुद्धि के लिए वर्तनी, लिंग, वचन, कारक और पदक्रम के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। 'प्राण', 'दर्शन', 'हस्ताक्षर', 'आँसू' जैसे नित्य बहुवचन शब्दों का सही प्रयोग सीखें।
‘वीर’ रस अथवा ‘करुण’ रस का स्थायीभाव लिखकर उदाहरण दीजिए।
View Solution
वीर रस
स्थायी भाव: उत्साह।
लक्षण: जब युद्ध, दान, धर्म या दया को लेकर मन में 'उत्साह' का भाव जाग्रत होता है, तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है।
उदाहरण:
मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे,
यमराज से भी युद्ध में, प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
करुण रस
स्थायी भाव: शोक।
लक्षण: जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से हृदय में 'शोक' का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है।
उदाहरण:
मणि खोये भुजंग सी जननी,
फन सा पटक रही थी शीश,
अंधी आज बनाकर मुझको,
किया न्याय तुमने जगदीश?
Quick Tip: रस का उत्तर लिखते समय स्थायी भाव का उल्लेख करना अनिवार्य है। लक्षण (परिभाषा) और उदाहरण दोनों देना आवश्यक है। उदाहरण ऐसा चुनें जो आपको अच्छी तरह याद हो और सरल हो।
‘उपमा’ अलंकार अथवा ‘रूपक’ अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए।
View Solution
उपमा अलंकार
लक्षण: जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उसके रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है।
उदाहरण:
पीपर पात सरिस मन डोला।
(यहाँ मन (उपमेय) की तुलना पीपल के पत्ते (उपमान) से की गई है।)
रूपक अलंकार
लक्षण: जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात् उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है।
उदाहरण:
चरण-कमल बन्दौं हरि राई।
(यहाँ 'चरण' (उपमेय) पर 'कमल' (उपमान) का आरोप है, दोनों को एक मान लिया गया है।)
Quick Tip: उपमा और रूपक में मुख्य अंतर है कि उपमा में 'सा', 'जैसा', 'सरिस' जैसे वाचक शब्दों से तुलना की जाती है, जबकि रूपक में उपमेय को सीधे उपमान का रूप दे दिया जाता है, कोई वाचक शब्द नहीं होता।
‘चौपाई’ छन्द अथवा ‘कुण्डलिया’ छन्द का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए।
View Solution
चौपाई छन्द
लक्षण: यह एक सम मात्रिक छन्द है। इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। चरण के अन्त में जगण (।ऽ।) और तगण (ऽऽ।) का आना वर्जित है।
उदाहरण:
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।।
(प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएँ हैं।)
कुण्डलिया छन्द
लक्षण: यह एक विषम मात्रिक छन्द है। यह एक दोहा और एक रोला को मिलाकर बनता है। इसमें छः चरण होते हैं। यह छन्द जिस शब्द से प्रारम्भ होता है, उसी शब्द से समाप्त भी होता है।
उदाहरण:
साईं बैर न कीजिये, गुरु, पंडित, कवि, यार।
बेटा, बनिता, पौरिया, यज्ञ करावन हार।।
यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई।
विप्र, पड़ोसी, वैद्य, आपकी तपै रसोई।।
कह गिरिधर कविराय, जुगन सों यह चलि आई।
इन तेरह सों तरह, दिये बनि आवै साईं।।
Quick Tip: कुण्डलिया छन्द को पहचानना बहुत आसान है। बस यह देखें कि क्या पहला और आखिरी शब्द समान है और क्या छन्द में छः पंक्तियाँ हैं। यदि हाँ, तो वह कुण्डलिया ही है।
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थनापत्र लिखिए।
अथवा
अपने मुहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिये नगरपालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए।
View Solution
(यहाँ पहले पत्र का प्रारूप दिया जा रहा है)
सेवा में,
श्रीमान शाखा प्रबंधक,
बैंक का नाम,
[ाखा का पता,
शहर का नाम।
विषय: नया बचत खाता खुलवाने के संबंध में।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं, [आपका नाम], [आपके पिता का नाम] का पुत्र/पुत्री, [आपका पता] का निवासी हूँ। मैं आपके प्रतिष्ठित बैंक में एक नया बचत खाता (Savings Account) खुलवाना चाहता/चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी बचत को सुरक्षित रख सकूँ और बैंक की अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकूँ।
मैंने खाता खुलवाने के लिए आवश्यक सभी प्रपत्र (फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फोटो) इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर दिए हैं।
अतः, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरा बचत खाता खोलने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/रहूँगी।
सधन्यवाद।
भवदीय,
[आपका नाम]
[आपका पता]
[मोबाइल नंबर]
दिनांक: [आज की तारीख]
Quick Tip: औपचारिक पत्र में प्रारूप (format) का विशेष महत्व होता है। प्रेषक का पता, दिनांक, पाने वाले का पद और पता, विषय, संबोधन, मुख्य विषय-वस्तु, और अंत में भवदीय/प्रार्थी आदि का सही क्रम में प्रयोग करें।
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा-शैली में निबन्ध लिखिए :
(i) मेरा प्रिय खेल
(ii) नयी शिक्षा नीति की विशेषताएँ
(iii) महिला सशक्तीकरण का समाज के विकास में प्रभाव
(iv) आतंकवाद की समस्या और समाधान
(v) विद्यालय में पुस्तकालय का महत्त्व
View Solution
(यहाँ विषय (iv) 'आतंकवाद की समस्या और समाधान' पर निबंध का प्रारूप दिया जा रहा है)
आतंकवाद की समस्या और समाधान
प्रस्तावना: आतंकवाद का अर्थ है 'आतंक' अर्थात् भय का साम्राज्य स्थापित करना। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा और भय का सहारा लेकर निर्दोष लोगों की हत्या करना आतंकवाद कहलाता है। आज यह केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सबसे गंभीर समस्या बन चुका है।
आतंकवाद के कारण: आतंकवाद के पीछे कई कारण हैं, जैसे - गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ और पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित हिंसा। अक्सर गुमराह युवाओं को धर्म या धन का लालच देकर इस गलत रास्ते पर धकेल दिया जाता है।
भारत में आतंकवाद: भारत लम्बे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद हो या देश के विभिन्न शहरों में हुए बम धमाके, भारत ने इसकी भारी कीमत चुकाई है।
समाधान के उपाय: आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। हमें अपनी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना होगा। इसके साथ ही, देश के भीतर गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं को दूर करना होगा ताकि कोई भी युवा गुमराह न हो सके।
उपसंहार: आतंकवाद मानवता का शत्रु है। इसे केवल सैन्य कार्यवाही से नहीं, बल्कि शिक्षा, विकास और आपसी सद्भाव से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
Quick Tip: निबंध को हमेशा रूपरेखा (प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार) में विभाजित करके लिखें। मध्य भाग में विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं (जैसे- कारण, प्रभाव, समाधान) पर अलग-अलग अनुच्छेद लिखें। इससे निबंध सुगठित और प्रभावशाली लगता है।











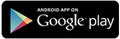


Comments