UP Board Class 10 Hindi Question Paper 2025 PDF (Code 801 BB) with Answer Key and Solutions PDF is available for download here. UP Board Class 10 exams were conducted between February 24th to March 12th 2025. The total marks for the theory paper were 70. Students reported the paper to be easy to moderate.
UP Board Class 10 Hindi Question Paper 2025 (Code 801 BB) with Solutions
| UP Board Class 10 Hindi (801 BB) Question Paper with Answer Key | Check Solutions |

'बादल की मृत्यु' किसकी रचना है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना और उसके लेखक से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
'बादल की मृत्यु' हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, एकांकीकार और आलोचक डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक एकांकी (एक अंक का नाटक) है।
इसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन् 1930 में हुआ था।
यह रचना आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी विधा की शुरुआत का प्रतीक है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'बादल की मृत्यु' डॉ. रामकुमार वर्मा की रचना है।
Quick Tip: प्रमुख साहित्यिक रचनाओं और उनके लेखकों की एक सूची बनाना परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होता है। विशेष रूप से उन रचनाओं पर ध्यान दें जिन्हें किसी विधा में 'प्रथम' होने का श्रेय प्राप्त है, जैसे 'बादल की मृत्यु' को प्रथम हिंदी एकांकी माना जाता है।
किस कहानीकार की कहानियाँ 'मानसरोवर' नाम से आठ भागों में संकलित हैं ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी के एक महान कहानीकार के कहानी-संग्रह के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation
'मानसरोवर' उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है।
उनकी लगभग 300 से अधिक कहानियाँ इस शीर्षक के अंतर्गत आठ खंडों में प्रकाशित हैं।
'मानसरोवर' में 'ईदगाह', 'पूस की रात', 'कफ़न', 'बड़े घर की बेटी' जैसी अनेक प्रसिद्ध कहानियाँ शामिल हैं।
Step 3: Final Answer
अतः, प्रेमचंद की कहानियाँ 'मानसरोवर' नाम से संकलित हैं।
Quick Tip: प्रमुख लेखकों के कहानी-संग्रहों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। 'मानसरोवर' प्रेमचंद से, 'आकाशदीप' और 'इंद्रजाल' जयशंकर प्रसाद से संबंधित हैं।
'शेखर : एक जीवनी' उपन्यास के लेखक हैं
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास और उसके लेखक की पहचान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
'शेखर : एक जीवनी' सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' द्वारा लिखा गया एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है।
यह उपन्यास नायक 'शेखर' के मानसिक विकास और उसके विद्रोह के कारणों का चित्रण करता है।
इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ था और इसे हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'शेखर : एक जीवनी' के लेखक 'अज्ञेय' हैं।
Quick Tip: लेखकों के उपनामों और उनके पूरे नामों को जानना महत्वपूर्ण है। 'अज्ञेय' का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है।
'अरे यायावर रहेगा याद' की विधा है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न एक साहित्यिक कृति की विधा (genre) की पहचान करने के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation
'अरे यायावर रहेगा याद' 'अज्ञेय' द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध यात्रा-वृत्तांत (travelogue) है।
इसमें लेखक ने अपनी भारत यात्रा के अनुभवों का बहुत ही रोचक और काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है।
यह कृति हिंदी यात्रा-साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। 'यायावर' का अर्थ घुमक्कड़ होता है, जो शीर्षक को सार्थक करता है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'अरे यायावर रहेगा याद' यात्रा-साहित्य विधा की रचना है।
Quick Tip: विभिन्न साहित्यिक विधाओं को समझें, जैसे- उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा-वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण आदि। इससे रचनाओं को वर्गीकृत करने में आसानी होती है।
हरिवंश राय 'बच्चन' द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध चार-खंडों वाली आत्मकथा के ज्ञान पर आधारित है।
Step 2: Detailed Explanation
हरिवंश राय 'बच्चन' की आत्मकथा को हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह चार खंडों में प्रकाशित हुई थी, जिनके नाम हैं:
1. क्या भूलूँ क्या याद करूँ (1969)
2. नीड़ का निर्माण फिर (1970)
3. बसेरे से दूर (1978)
4. दशद्वार से सोपान तक (1985)
दिए गए विकल्पों में, 'मेरी आत्मकहानी' इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'मेरी आत्मकहानी' बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है।
Quick Tip: प्रमुख लेखकों की आत्मकथाओं के नाम याद रखें। बच्चन जी की चार-खंडों वाली आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, इनके चारों नाम और क्रम को याद करना उपयोगी है।
रीतिकाल की काव्यभाषा है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में 'रीतिकाल' के दौरान प्रयुक्त मुख्य काव्य भाषा के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसे 'रीतिकाल' (लगभग 1650-1850 ई.) के नाम से जाना जाता है, में काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया।
केशवदास, बिहारी, भूषण, घनानंद जैसे रीतिकाल के सभी प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में ही कीं।
इस काल में ब्रजभाषा अपने साहित्यिक सौंदर्य और माधुर्य के चरम पर थी। खड़ीबोली का गद्य में विकास तो हो रहा था, पर काव्य में उसका प्रयोग आधुनिक काल में शुरू हुआ।
Step 3: Final Answer
अतः, रीतिकाल की प्रमुख काव्यभाषा ब्रजभाषा थी।
Quick Tip: हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों (आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल) की प्रमुख भाषाओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों को याद रखें। जैसे भक्तिकाल में ब्रज और अवधी दोनों थीं, पर रीतिकाल में ब्रजभाषा का वर्चस्व था।
कवि भूषण की रचना नहीं है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण की रचनाओं के ज्ञान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
कवि भूषण रीतिकाल के एक वीर-रस के कवि थे। उनकी प्रामाणिक रचनाओं में तीन प्रमुख हैं:
शिवराज भूषण: यह एक अलंकार-ग्रंथ है जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है।
शिवा बावनी: इसमें शिवाजी के शौर्य से संबंधित 52 छंद हैं।
छत्रसाल दशक: इसमें बुंदेला राजा छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा में 10 छंद हैं।
'रामचन्द्रिका' रीतिकाल के ही एक अन्य प्रमुख कवि 'केशवदास' की रचना है। केशवदास को 'कठिन काव्य का प्रेत' भी कहा जाता है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'रामचन्द्रिका' कवि भूषण की रचना नहीं है, यह केशवदास की रचना है।
Quick Tip: एक ही काल के विभिन्न कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं में अंतर करना सीखें। भूषण और केशवदास दोनों ही रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन उनकी शैली और रचनाएँ अलग-अलग हैं।
'द्विवेदी युग' नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग के नामकरण के आधार के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation
आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद के समय को 'द्विवेदी युग' (लगभग 1900-1920 ई.) के नाम से जाना जाता है।
इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है।
उन्होंने 1903 में 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन संभाला और भाषा के परिष्कार, व्याकरण की शुद्धि और हिंदी गद्य को एक मानक रूप देने में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके इसी योगदान के कारण इस पूरे युग को उनके नाम से जाना जाता है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'द्विवेदी युग' का नामकरण महावीरप्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है।
Quick Tip: द्विवेदी उपनाम वाले कई साहित्यकार हैं, इसलिए भ्रमित न हों। 'द्विवेदी युग' का संबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी से है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध आलोचक और उपन्यासकार हैं जो बाद के काल के हैं।
'तार सप्तक' के कवियों को 'अज्ञेय' ने क्या कहकर संबोधित किया है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न 'तार सप्तक' और उसके कवियों के संबंध में संपादक 'अज्ञेय' द्वारा प्रयुक्त एक विशेष उक्ति के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation
'अज्ञेय' के संपादन में 1943 में 'तार सप्तक' का प्रकाशन हुआ, जिसमें सात कवियों की कविताएँ संकलित थीं। इसे प्रयोगवाद का प्रस्थान बिंदु माना जाता है।
इसकी भूमिका में 'अज्ञेय' ने स्पष्ट किया कि ये सातों कवि किसी एक विचारधारा के नहीं हैं, और न ही वे कविता के किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचे हैं।
उन्होंने इन कवियों को 'राहों के अन्वेषी' कहा, जिसका अर्थ है 'नए रास्तों के खोजकर्ता'। यह उक्ति उनकी प्रयोगधर्मिता और नवीनता की खोज की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'अज्ञेय' ने 'तार सप्तक' के कवियों को 'राहों के अन्वेषी' कहकर संबोधित किया है।
Quick Tip: 'तार सप्तक' और उसके बाद प्रकाशित अन्य सप्तकों (दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक) का हिंदी साहित्य में बहुत महत्व है। इनके प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रमुख कवियों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है।
'धूप के धान' रचना किसकी है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न एक प्रसिद्ध काव्य-संग्रह और उसके रचयिता की पहचान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
'धूप के धान' एक प्रसिद्ध काव्य-संग्रह है जिसके रचयिता गिरिजाकुमार माथुर हैं।
गिरिजाकुमार माथुर 'तार सप्तक' के सात कवियों में से एक थे और वे अपनी रोमानी और चित्रमयी कविताओं के लिए जाने जाते हैं।
'धूप के धान' के अतिरिक्त 'नाश और निर्माण', 'शिलापंख चमकीले', 'भीतरी नदी की यात्रा' उनकी अन्य प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं।
Step 3: Final Answer
अतः, 'धूप के धान' गिरिजाकुमार माथुर की रचना है।
Quick Tip: 'तार सप्तक' के सभी सात कवियों - अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर और रामविलास शर्मा - की एक-एक प्रमुख रचना को याद कर लें।
'करुण रस' का स्थायी भाव है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र में 'रस' सिद्धांत के अंतर्गत 'करुण रस' के स्थायी भाव से संबंधित है। स्थायी भाव वे मूल भावनाएँ हैं जो हृदय में स्थायी रूप से रहती हैं।
Step 2: Detailed Explanation
काव्यशास्त्र में प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित किया गया है।
करुण रस: इसका स्थायी भाव 'शोक' है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट से उत्पन्न दुःख या शोक की भावना जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होती है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है।
निर्वेद: यह शांत रस का स्थायी भाव है।
रति: यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है।
रौद्र: यह एक रस है, जिसका स्थायी भाव 'क्रोध' होता है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'करुण रस' का स्थायी भाव 'शोक' है।
Quick Tip: सभी प्रमुख रसों और उनके स्थायी भावों की तालिका बनाकर याद करें, जैसे - श्रृंगार (रति), हास्य (हास), करुण (शोक), वीर (उत्साह), रौद्र (क्रोध), भयानक (भय), वीभत्स (जुगुप्सा), अद्भुत (विस्मय), शांत (निर्वेद)।
"चमचमात चंचल नयन, बिच घूँघट पट झीन ।
मानहुँ सुरसरिता-विमल-जल दृग उछरत जुग मीन ।।"
उपर्युक्त दोहे में अलंकार है :
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न दिए गए काव्य पंक्तियों में अलंकार की पहचान करने से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहाँ उपमेय (जिसकी तुलना की जाए) में उपमान (जिससे तुलना की जाए) की संभावना या कल्पना की जाती है।
इसकी पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे - मनु, मानो, मनहुँ, जानो, जनहुँ, आदि।
दी गई पंक्तियों में, नायिका के चंचल नयनों (उपमेय) को देखकर ऐसी कल्पना की जा रही है मानो (मानहुँ) गंगा के निर्मल जल में दो मछलियाँ (उपमान) उछल रही हों।
यहाँ 'मानहुँ' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से संभावना को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है।
Step 3: Final Answer
अतः, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
Quick Tip: अलंकारों की पहचान के लिए उनके वाचक शब्दों पर ध्यान दें। 'सा, सी, सम, सरिस' आदि उपमा के वाचक हैं, जबकि 'मनु, मानो, जनु, जानो' आदि उत्प्रेक्षा के वाचक हैं।
'रोला' छंद किस प्रकार का छंद है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी काव्यशास्त्र में 'छंद' के वर्गीकरण से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है:
सम छंद: जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे - चौपाई, रोला, हरिगीतिका।
अर्धसम छंद: जिसके पहले और तीसरे (विषम) चरण में तथा दूसरे और चौथे (सम) चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे - दोहा, सोरठा, बरवै।
विषम छंद: जिसके चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है और जो दो छंदों के मेल से बनता है। जैसे - कुंडलिया, छप्पय।
'रोला' एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति (विराम) होती है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'रोला' एक सम छंद है।
Quick Tip: प्रमुख छंदों (दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया) के लक्षण और उदाहरण याद कर लें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे सम, अर्धसम या विषम हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं।
'अध्यक्ष' में प्रयुक्त उपसर्ग है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न शब्द-रचना के अंतर्गत उपसर्ग की पहचान करने से संबंधित है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं।
Step 2: Detailed Explanation
'अध्यक्ष' शब्द की संधि-विच्छेद करने पर हमें इसका मूल शब्द और उपसर्ग मिलता है।
यह यण संधि का उदाहरण है:
\[ अध्यक्ष = अधि + अक्ष \]
यहाँ 'इ' + 'अ' मिलकर 'य' बन जाता है।
इस प्रकार, 'अक्ष' मूल शब्द में 'अधि' उपसर्ग जुड़ा है। 'अधि' उपसर्ग का अर्थ होता है 'ऊपर', 'श्रेष्ठ' या 'प्रधान'।
Step 3: Final Answer
अतः, 'अध्यक्ष' शब्द में 'अधि' उपसर्ग है।
Quick Tip: उपसर्गों की पहचान के लिए संधि-विच्छेद का ज्ञान बहुत सहायक होता है, विशेषकर यण संधि, क्योंकि इसमें उपसर्ग का अंतिम स्वर और मूल शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं।
जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है, उसे कहते हैं –
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी व्याकरण में 'समास' (compound) के प्रकारों और उनकी परिभाषाओं से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
समास के विभिन्न प्रकारों की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:
अव्ययीभाव समास: पहला पद अव्यय और प्रधान होता है।
बहुव्रीहि समास: कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
द्वंद्व समास: दोनों पद प्रधान होते हैं।
द्विगु समास: इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है।
प्रश्न में दी गई परिभाषा ("पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है") द्विगु समास के लक्षण हैं। उदाहरण: चौराहा (चार राहों का समूह), त्रिलोक (तीन लोकों का समाहार), पंचवटी (पाँच वटों का समूह)।
Step 3: Final Answer
अतः, इस प्रकार के समास को द्विगु समास कहते हैं।
Quick Tip: 'द्विगु' शब्द में ही 'द्वि' (दो) संख्या का बोध है। इससे आप याद रख सकते हैं कि द्विगु समास संख्या से संबंधित है।
'खीर' शब्द का तत्सम रूप है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न तत्सम और तद्भव शब्दों के ज्ञान पर आधारित है। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।
Step 2: Detailed Explanation
'खीर' एक तद्भव शब्द है। इसका मूल संस्कृत शब्द 'क्षीर' है।
संस्कृत में 'क्षीर' का अर्थ दूध या दूध से बना कोई पकवान होता है। समय के साथ ध्वनि परिवर्तन के कारण 'क्ष' का 'ख' और 'र' का 'र' ही रहने से 'क्षीर' शब्द 'खीर' बन गया।
अन्य विकल्पों के अर्थ:
नीर: जल, पानी
क्षेत्र: खेत (तद्भव) का तत्सम रूप
Step 3: Final Answer
अतः, 'खीर' शब्द का तत्सम रूप 'क्षीर' है।
Quick Tip: तत्सम-तद्भव शब्दों में कुछ सामान्य ध्वनि परिवर्तन होते हैं, जैसे - 'क्ष' का 'ख' या 'छ' हो जाना (क्षीर -> खीर), 'त्र' का 'त' हो जाना (रात्रि -> रात), 'श' का 'स' हो जाना (श्यामल -> साँवला)। इन्हें याद रखने से पहचानना आसान हो जाता है।
'तस्मै' में विभक्ति और वचन है
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न संस्कृत व्याकरण के शब्द-रूप (declension) के ज्ञान पर आधारित है, जो हिंदी व्याकरण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Step 2: Detailed Explanation
'तस्मै' शब्द 'तत्' (वह) सर्वनाम के पुल्लिंग रूप का शब्द-रूप है।
'तत्' सर्वनाम (पुल्लिंग) का रूप इस प्रकार चलता है:
प्रथमा: सः, तौ, ते
द्वितीया: तम्, तौ, तान्
तृतीया: तेन, ताभ्याम्, तैः
चतुर्थी: तस्मै, ताभ्याम्, तेभ्यः
पञ्चमी: तस्मात्, ताभ्याम्, तेभ्यः
इस तालिका से स्पष्ट है कि 'तस्मै' चतुर्थी विभक्ति, एकवचन का रूप है। इसका अर्थ होता है 'उसके लिए'।
Step 3: Final Answer
अतः, 'तस्मै' में चतुर्थी विभक्ति और एकवचन है।
Quick Tip: संस्कृत के कुछ प्रमुख सर्वनामों (जैसे- तत्, किम्, अस्मद्, युष्मद्) और संज्ञाओं (जैसे- राम, हरि, गुरु, नदी) के शब्द-रूप याद करना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जिस वाक्य से आश्चर्य, दुःख या सुख का बोध हो, उस वाक्य को कहते हैं
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों की पहचान से संबंधित है।
Step 2: Detailed Explanation
अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद होते हैं। प्रश्न में दिए गए भाव (आश्चर्य, दुःख, सुख, घृणा, हर्ष आदि) को व्यक्त करने वाले वाक्यों को विस्मयबोधक वाक्य (Exclamatory Sentence) कहते हैं।
इन वाक्यों में प्रायः 'अरे!', 'वाह!', 'हाय!', 'ओह!' जैसे विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग होता है और अंत में विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लगाया जाता है।
उदाहरण: "वाह! कितना सुंदर दृश्य है।" (सुख/आश्चर्य), "हाय! यह क्या हो गया।" (दुःख)।
Step 3: Final Answer
अतः, ऐसे वाक्य को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं।
Quick Tip: अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, और विस्मयबोधक। इनकी परिभाषाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
'रोहन से चला नहीं जाता ।' इस वाक्य में कौन-सा वाच्य है ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न हिंदी व्याकरण में 'वाच्य' (Voice) की पहचान से संबंधित है। वाच्य यह बताता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म, या भाव है।
Step 2: Detailed Explanation
वाच्य के तीन मुख्य भेद हैं:
कर्तृवाच्य (Active Voice): क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। (जैसे - रोहन चलता है।)
कर्मवाच्य (Passive Voice): क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' का प्रयोग होता है। (जैसे - रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।)
भाववाच्य (Impersonal Voice): क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न कर्म से, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक, पुल्लिंग, और एकवचन में होती है। कर्ता के साथ 'से' का प्रयोग होता है और प्रायः असमर्थता का भाव प्रकट होता है।
दिए गए वाक्य "रोहन से चला नहीं जाता" में, कर्ता 'रोहन' के साथ 'से' लगा है, क्रिया 'चला नहीं जाता' अकर्मक, पुल्लिंग, एकवचन है और असमर्थता का भाव है। यह सभी लक्षण भाववाच्य के हैं।
Step 3: Final Answer
अतः, इस वाक्य में भाववाच्य है। ('विशेषण वाच्य' कोई वाच्य का भेद नहीं होता है।)
Quick Tip: भाववाच्य की पहचान का सरल तरीका है: कर्ता + 'से' + अकर्मक क्रिया (जो हमेशा पुल्लिंग, एकवचन में होगी) + प्रायः नकारात्मकता/असमर्थता।
निम्नलिखित में अविकारी शब्द है :
View Solution
Step 1: Understanding the Concept
यह प्रश्न विकारी और अविकारी शब्दों की पहचान से संबंधित है।
विकारी शब्द: वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं।
अविकारी शब्द (अव्यय): वे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता। क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द हैं।
Step 2: Detailed Explanation
आइए विकल्पों का विश्लेषण करें:
(A) बालक (संज्ञा): इसका रूप बदलता है (बालक, बालकों, बालिका)। यह विकारी है।
(B) पुस्तक (संज्ञा): इसका रूप बदलता है (पुस्तक, पुस्तकें)। यह विकारी है।
(C) निकट (क्रिया-विशेषण/संबंधबोधक): इसका रूप नहीं बदलता। 'लड़का निकट बैठा है', 'लड़की निकट बैठी है', 'लड़के निकट बैठे हैं' - इन सभी वाक्यों में 'निकट' अपरिवर्तित है। यह अविकारी (अव्यय) है।
(D) पुराना (विशेषण): इसका रूप बदलता है (पुराना, पुरानी, पुराने)। यह विकारी है।
Step 3: Final Answer
अतः, 'निकट' एक अविकारी शब्द है।
Quick Tip: किसी शब्द के विकारी या अविकारी होने की जाँच करने के लिए उसे अलग-अलग लिंग और वचन के कर्ता के साथ वाक्य में प्रयोग करके देखें। यदि शब्द का रूप बदल जाता है, तो वह विकारी है, अन्यथा अविकारी।
निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
गद्यांश - 1
बहुत-से लोग ऐसे होते हैं, जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं।
(i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
(ii) गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
(iii) किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है ?
View Solution
(i) सन्दर्भ :
प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध 'मित्रता' से उद्धृत है। इस निबंध में लेखक ने अच्छी संगति के महत्व और बुरी संगति के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश बुरी संगति के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या :
रेखांकित अंश : "बहुत-से लोग ऐसे होते हैं, जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है।"
व्याख्या : लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल बुरी संगति के खतरों से आगाह करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों का साथ इतना हानिकारक होता है कि उनके साथ बिताया गया एक क्षण भी हमारी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोग उस थोड़े से समय में भी अनुचित और अश्लील बातें करते हैं। ये बातें हमारे कानों के माध्यम से हमारे मन-मस्तिष्क पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह प्रभाव इतना विषैला होता है कि हमारे मन की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत तीव्र और घातक होता है।
(iii) उत्तर :
गद्यांश के अनुसार, व्यक्ति पर बुरी, भद्दी और फूहड़ बातों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भद्दे और फूहड़ गीत हमें तुरंत याद हो जाते हैं, उसी प्रकार बुरी बातें भी हमारे मन में शीघ्रता से घर कर लेती हैं, जबकि कोई गंभीर या अच्छी बात उतनी जल्दी अपना प्रभाव नहीं छोड़ती।
Quick Tip: सन्दर्भ लिखते समय, पाठ का नाम और लेखक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। व्याख्या करते समय, रेखांकित अंश के प्रत्येक हिस्से का अर्थ अपने शब्दों में विस्तार से समझाएं और उसे गद्यांश के मूल भाव से जोड़ें।
जो तरुण संसार के जीवन-संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, जो वृद्ध हो गये हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीतकाल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असन्तोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रान्ति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत-गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है।
(i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
(ii) गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
(iii) तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण (सोचने-समझने का नजरिया) में अंतर बताइए।
View Solution
(i) सन्दर्भ :
प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध निबंधकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित निबंध 'क्या लिखूँ?' से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने युवा और वृद्ध पीढ़ी के दृष्टिकोण में पाए जाने वाले स्वाभाविक अंतर को स्पष्ट किया है।
(नोट: इस गद्यांश में कोई अंश रेखांकित नहीं है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में प्रथम वाक्य की व्याख्या की जाती है।)
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या (प्रथम वाक्य के आधार पर) :
वाक्य : "जो तरुण संसार के जीवन-संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, जो वृद्ध हो गये हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीतकाल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है।"
व्याख्या : लेखक कहते हैं कि युवा, जिन्होंने अभी जीवन के वास्तविक संघर्षों और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, वे दुनिया को बहुत आकर्षक और सुंदर समझते हैं। अनुभव की कमी के कारण वे आदर्शवादी होते हैं और उन्हें भविष्य सुनहरा दिखाई देता है। इसके विपरीत, वृद्ध व्यक्ति, जो अपने बचपन और जवानी के दिन बहुत पीछे छोड़ आए हैं, उन्हें अपने अतीत का स्मरण करना बहुत सुखद लगता है। वे अपने बीते हुए दिनों की यादों में खोए रहते हैं और उन्हीं में आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार, लेखक युवा और वृद्ध के जीवन के प्रति दो बिल्कुल भिन्न नजरियों को प्रस्तुत करते हैं - एक भविष्योन्मुखी और दूसरा अतीतजीवी।
(iii) तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में अंतर :
गद्यांश के अनुसार, तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं:
समय पर ध्यान केंद्रित करना: तरुण भविष्य की ओर देखते हैं और उनके लिए भविष्य उज्ज्वल होता है, जबकि वृद्ध अतीत में जीते हैं और उन्हें अतीत की यादें सुखद लगती हैं।
वर्तमान के प्रति दृष्टिकोण: दोनों ही पीढ़ियाँ वर्तमान से असंतुष्ट रहती हैं।
लक्ष्य और क्रिया: तरुण अपने उज्ज्वल भविष्य की कल्पना को वर्तमान में साकार करना चाहते हैं, जबकि वृद्ध अपने गौरवशाली अतीत को ही वर्तमान में फिर से देखना चाहते हैं।
परिवर्तन के प्रति रवैया: तरुण क्रान्ति और तीव्र परिवर्तन के समर्थक होते हैं, जबकि वृद्ध अतीत के गौरव और परंपराओं के संरक्षक होते हैं। Quick Tip: जब किसी गद्यांश में रेखांकित अंश न दिया गया हो, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश के मुख्य विचार या पहले कुछ वाक्यों को आधार बनाना एक सुरक्षित रणनीति है। तुलनात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय, बिंदुओं में अंतर स्पष्ट करना प्रस्तुति को बेहतर बनाता है।
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
पद्यांश - 1
ऊधौ मन न भए दस बीस ।
एक हुतौ सो गयौ स्याम सँग, को अवराधै ईस ।।
इंद्री सिथिल भई केशव बिनु, ज्यौं देही बिनु सीस ।
आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस ।।
तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के, सकल जोग के ईस ।
सूर हमारै नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदीस ।।
(i) उपर्युक्त पद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
(ii) गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म (ईश्वर) की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं ?
(iii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
View Solution
(i) सन्दर्भ :
प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित 'सूरसागर' महाकाव्य के 'भ्रमरगीत' प्रसंग से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य-पुस्तक के 'पद' नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इन पदों में सूरदास जी ने गोपियों की विरह-वेदना और श्रीकृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है।
(ii) उत्तर :
गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना में स्वयं को इसलिए असमर्थ बताती हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही मन था, जो श्रीकृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। वे कहती हैं कि ईश्वर की आराधना करने के लिए मन का होना आवश्यक है, और जब उनका मन ही उनके पास नहीं है तो वे किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। उनका मन पूरी तरह से श्रीकृष्ण में रम चुका है।
(iii) रेखांकित अंश की व्याख्या :
रेखांकित अंश : "सूर हमारै नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदी"स ।।"
व्याख्या : सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव! हमारे लिए तो नंदजी के पुत्र श्रीकृष्ण ही सब कुछ हैं, वे ही हमारे एकमात्र जगदीश (संसार के स्वामी) हैं। उनके बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर या आराध्य नहीं है। गोपियाँ यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि वे श्रीकृष्ण के सगुण रूप की ही उपासक हैं और उनके लिए नंद के नंदन श्रीकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है।
Quick Tip: सन्दर्भ लिखते समय कवि का नाम, रचना का नाम, प्रसंग (यदि ज्ञात हो) और पाठ का शीर्षक अवश्य लिखें। इससे उत्तर पूर्ण और प्रभावशाली बनता है। 'भ्रमरगीत' प्रसंग सूरदास की गोपियों की वाक्पटुता और तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध है।
पद्यांश - 2
सहे वार पर वार अंत तक,
लड़ी वीर बाला-सी ।
आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर,
चमक उठी ज्वाला-सी ।।
बढ़ जाता है मान वीर का,
रण में बलि होने से ।
मूल्यवती होती सोने की,
भस्म यथा सोने से ।।
(i) उपर्युक्त पद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
(iii) 'आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी' पंक्ति में कौन-सा अलंकार है ?
View Solution
(i) सन्दर्भ :
प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता 'झाँसी की रानी की समाधि पर' से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य-पुस्तक के काव्य-खंड में संकलित है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का गौरवगान करते हुए उनकी वीरता और आत्म-त्याग को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या :
रेखांकित अंश : "बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से । मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से ।।"
व्याख्या : कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिस प्रकार युद्धभूमि में बलिदान देने से किसी वीर का सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का आत्म-त्याग उनके गौरव को अनंत गुना बढ़ा देता है। वे अपने कथन को पुष्ट करने के लिए सोने का उदाहरण देती हैं। जिस प्रकार शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की वह भस्म (राख) होती है जो औषधि के रूप में काम आती है, उसी प्रकार साधारण मृत्यु की अपेक्षा देश के लिए दिया गया बलिदान व्यक्ति को और भी अधिक मूल्यवान और सम्माननीय बना देता है।
(iii) उत्तर :
'आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी' पंक्ति में उपमा अलंकार है।
यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के चिता पर बलिदान होने की क्रिया की तुलना यज्ञ में दी जाने वाली 'आहुति' से और उनके यश के चमकने की तुलना 'ज्वाला' से की गई है। 'सी' वाचक शब्द का प्रयोग उपमा अलंकार को स्पष्ट करता है।
Quick Tip: अलंकार पहचानते समय वाचक शब्दों (जैसे - सा, सी, से, सम, सरिस - उपमा के लिए; मनु, मानो, जनु, जानो - उत्प्रेक्षा के लिए) पर ध्यान दें। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म - इन चार अंगों का ध्यान रखा जाता है।
नीचे दिये गये संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
संस्कृत गद्यांश - 1
दुर्मुख ! द्वितीयः कशाघातः । (दुर्मुखः पुनः ताडयति ।) ताडितः चन्द्रशेखरः पुनः पुनः 'भारतं जयतु' इति वदति । (एवं स पञ्चदशकशाघातैः ताडितः) यदा चन्द्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च ।
View Solution
सन्दर्भ :
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के संस्कृत-खंड में संकलित 'देशभक्तः चन्द्रशेखरः' नामक पाठ से लिया गया है। इस अंश में, देशभक्त चंद्रशेखर पर कारागार में हो रहे अत्याचार और कारागार से मुक्त होने पर जनता द्वारा उनके भव्य स्वागत का वर्णन किया गया है।
हिन्दी में अनुवाद :
दुर्मुख! (यह) दूसरा कोड़ा है। (दुर्मुख फिर से मारता है।) कोड़ों से पीटे जाते हुए चंद्रशेखर बार-बार 'भारत माता की जय हो' ऐसा बोलते हैं। (इस प्रकार वह पंद्रह कोड़ों से पीटे गए।) जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तभी सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और मालाओं से उनका अभिनंदन (स्वागत) करते हैं।
Quick Tip: संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय शब्दों के सही अर्थ और विभक्ति के अनुसार कारक चिह्नों (जैसे - तस्य = उसके, पादयोः = पैरों पर) का ध्यान रखें। कोष्ठक में दिए गए वाक्यों का भी अनुवाद करना आवश्यक है क्योंकि वे क्रिया को स्पष्ट करते हैं।
भारतीया संस्कृतिः तु सर्वेषां मतावलम्बिनां संगमस्थली । काले-काले विविधाः विचाराः भारतीय-संस्कृतौ समाहिताः । एषा संस्कृतिः सामासिकी संस्कृतिः यस्याः विकासे विविधानां जातीनां सम्प्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते । अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृतिः एका च राष्ट्रीयता ।
View Solution
सन्दर्भ :
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक के संस्कृत-खंड में संकलित 'भारतीय संस्कृतिः' नामक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी और उदार प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है।
हिन्दी में अनुवाद :
भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम-स्थली (मिलने का स्थान) है। समय-समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिल गए हैं। यह संस्कृति एक सामासिक (मिली-जुली) संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। इसीलिए हम सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है।
Quick Tip: 'सामासिकी संस्कृतिः' जैसे महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ (मिली-जुली संस्कृति या composite culture) समझना गद्यांश के मूल भाव को पकड़ने के लिए आवश्यक है। अनुवाद करते समय भाषा को सरल और प्रवाहपूर्ण रखने का प्रयास करें।
नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का सन्दर्भ-सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः ।।
अथवा
मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति ।
कामं हित्वार्थवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत् ।।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह श्लोक 'विष्णु पुराण' से लिया गया है। इसमें 'भारत' देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है और यहाँ के निवासियों को 'भारती' कहा गया है।
Step 2: Detailed Explanation:
सन्दर्भ:
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खण्ड में संकलित 'लक्ष्य-भेद परीक्षा' नामक पाठ से उद्धृत है। यह मूलतः 'विष्णु पुराण' में वर्णित है और इसमें भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है।
अनुवाद:
जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नामक देश है, और वहाँ की संतानें (निवासी) भारती कहलाती हैं।
This verse defines the geographical boundaries of the land of Bharat, placing it north of the ocean (Indian Ocean) and south of the Himalayas. The inhabitants of this land are referred to as 'Bharati', the descendants of Bharata.
Step 3: Final Answer:
The verse defines India (Bharat) as the land situated north of the ocean and south of the Himalayas, and its people are called Bharati.
Quick Tip: संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करते समय, पहले सन्दर्भ (पाठ और ग्रन्थ का नाम) लिखें, फिर प्रसंग (श्लोक में क्या कहा जा रहा है) और अंत में शब्दशः अनुवाद करें। इससे उत्तर की प्रस्तुति बेहतर होती है और पूरे अंक मिलते हैं।
'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य के नायक महात्मा गाँधी हैं। इस प्रश्न में उनके चरित्र की उन विशेषताओं का वर्णन करना है जो काव्य में प्रस्तुत की गई हैं।
Step 2: Detailed Explanation:
'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य में महात्मा गाँधी के चरित्र को अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. अलौकिक महापुरुष: कवि ने गाँधीजी को ईश्वर का अवतार बताया है जो भारत को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए जन्मे थे। वह मानवता के संरक्षक और दीन-दुखियों के उद्धारक हैं।
2. सत्य और अहिंसा के पुजारी: गाँधीजी सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानते थे। उन्होंने बिना किसी हिंसा के अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया।
3. हरिजनों के उद्धारक: गाँधीजी समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने हरिजनों को सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और उन्हें 'ईश्वर के जन' कहा।
4. दृढ़ निश्चयी और साहसी: गाँधीजी अपने निश्चय पर अडिग रहते थे। उन्होंने जो भी करने का संकल्प लिया, उसे पूरा करके ही दम लिया, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आईं हों।
5. महान देश-भक्त: गाँधीजी के हृदय में देश-प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'मुक्तिदूत' के नायक महात्मा गाँधी एक अलौकिक, सत्य-अहिंसा के समर्थक, हरिजनों के उद्धारक, दृढ़-निश्चयी और महान देश-भक्त महापुरुष हैं।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण करते समय, उत्तर को विभिन्न शीर्षकों (जैसे - महान नेता, सत्य के पुजारी, आदि) में बांटकर लिखें। प्रत्येक शीर्षक के समर्थन में काव्य से एक-दो पंक्तियाँ (यदि याद हों) उद्धृत करने से उत्तर और भी प्रभावी हो जाता है।
'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य के चौथे सर्ग की प्रमुख घटनाओं का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहता है। यह सर्ग गाँधीजी के प्रसिद्ध 'नमक सत्याग्रह' या 'दांडी मार्च' पर केंद्रित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मुक्तिदूत' खण्डकाव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश इस प्रकार है:
पृष्ठभूमि: अंग्रेज सरकार ने नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगा दिया था, जिससे आम जनता, विशेषकर गरीब, बहुत परेशान थी। गाँधीजी ने इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने का निश्चय किया।
दांडी यात्रा का आरम्भ: गाँधीजी ने इस कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक पदयात्रा आरम्भ की। उनके साथ 78 स्वयंसेवक थे। यह यात्रा 24 दिनों तक चली।
यात्रा का प्रभाव: गाँधीजी जहाँ भी जाते, हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते और उनके विचारों से प्रेरित होते। इस यात्रा ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई लहर पैदा कर दी।
कानून का उल्लंघन: 6 अप्रैल, 1930 को गाँधीजी दांडी पहुँचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।
इस सर्ग में कवि ने गाँधीजी के नेतृत्व कौशल और उनके अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को सफलतापूर्वक दर्शाया है।
Step 3: Final Answer:
चतुर्थ सर्ग में गाँधीजी द्वारा नमक कानून के विरोध में की गई ऐतिहासिक दांडी यात्रा का वर्णन है, जिसमें वे साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं और नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं, जिससे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात होता है।
Quick Tip: किसी सर्ग का सारांश लिखते समय, केवल मुख्य घटनाओं और उनके क्रम पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक विस्तार से बचें और सारांश को संक्षिप्त और सारगर्भित रखें।
'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य के नायक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस प्रश्न में काव्य के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य में कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट और प्रेरक व्यक्तित्व को चित्रित किया है। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. अलौकिक पुरुष: कवि ने नेहरूजी के व्यक्तित्व को सूर्य की तरह तेजस्वी और हिमालय की तरह अचल बताया है। वे एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी।
2. महान स्वतंत्रता सेनानी: नेहरूजी ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने देश की आजादी के लिए अनेक कष्ट सहे और कई बार जेल गए।
3. विश्व शांति के समर्थक: नेहरूजी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के नेता थे। उन्होंने 'पंचशील' के सिद्धांतों के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया।
4. प्रकृति-प्रेमी: काव्य में नेहरूजी को एक महान प्रकृति-प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें नदियों, पर्वतों और प्राकृतिक सौन्दर्य से गहरा लगाव था।
5. दृढ़-संकल्प और कर्मयोगी: वे जो भी निश्चय करते थे, उसे पूरा करने के लिए निरंतर कर्म करते रहते थे। वे आलस्य के प्रबल विरोधी और कर्म में विश्वास रखने वाले थे।
Step 3: Final Answer:
संक्षेप में, 'ज्योति जवाहर' के नायक पंडित नेहरू एक अलौकिक, महान स्वतंत्रता सेनानी, विश्व शांति के अग्रदूत, प्रकृति-प्रेमी और एक सच्चे कर्मयोगी हैं।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण के प्रश्नों में, नायक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं (जैसे- राजनैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत) को उजागर करने का प्रयास करें। इससे उत्तर अधिक व्यापक और संतुलित बनता है।
'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग के कथानक का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य के दूसरे सर्ग की कथावस्तु को संक्षेप में लिखने के लिए कहता है। इस सर्ग में नेहरूजी के व्यक्तित्व के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का वर्णन है।
Step 2: Detailed Explanation:
'ज्योति जवाहर' खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक इस प्रकार है:
इस सर्ग का आरम्भ 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' से होता है। अंग्रेज सरकार भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में बंदी बना लिया जाता है।
जेल में रहते हुए नेहरूजी आत्म-चिंतन करते हैं। वे भारत के गौरवशाली अतीत, उसकी संस्कृति और महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे सोचते हैं कि भारत जो कभी विश्व गुरु था, आज पराधीन क्यों है।
वे भारत के भविष्य के बारे में सोचते हैं और एक स्वतंत्र, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं। वे भारत की गरीबी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेते हैं।
इस सर्ग में कवि ने नेहरूजी की गहन चिंतनशीलता, उनके ऐतिहासिक ज्ञान और भारत के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि को उजागर किया है। जेल का एकांतवास उनके लिए आत्म-विश्लेषण और भविष्य की योजना बनाने का अवसर बन जाता है।
Step 3: Final Answer:
द्वितीय सर्ग में 1942 के आंदोलन के दौरान नेहरूजी की गिरफ्तारी, अहमदनगर किले में उनके बंदी जीवन, और वहाँ उनके द्वारा भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर किए गए गहन चिंतन का वर्णन है।
Quick Tip: कथानक लिखते समय घटनाओं को कालानुक्रमिक (chronological) रूप से प्रस्तुत करें। सर्ग के आरम्भ, मध्य और अंत की मुख्य घटनाओं का उल्लेख अवश्य करें।
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य के 'आयोजन' सर्ग की कथावस्तु लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य महाभारत की घटना पर आधारित है। इसका 'आयोजन' सर्ग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की तैयारियों और उसके आयोजन का वर्णन करता है।
Step 2: Detailed Explanation:
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य के 'आयोजन' सर्ग की कथावस्तु इस प्रकार है:
यज्ञ का विचार: हस्तिनापुर में राज्य स्थापित करने के बाद, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का विचार करते हैं। वे इस विषय पर अपने भाइयों और भगवान श्रीकृष्ण से परामर्श करते हैं।
श्रीकृष्ण का परामर्श: श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को यज्ञ करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे मगध के अत्याचारी राजा जरासंध के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, जो यज्ञ में बाधा डाल सकता है। श्रीकृष्ण पहले जरासंध का वध करने का सुझाव देते हैं।
जरासंध का वध: श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण कर मगध जाते हैं। वहाँ भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्ल-युद्ध होता है, जिसमें श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम जरासंध का वध कर देते हैं। जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जाता है।
यज्ञ की तैयारी: जरासंध की मृत्यु के बाद, राजसूय यज्ञ के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाती है। युधिष्ठिर भव्य यज्ञ की तैयारी आरम्भ करते हैं। देश-विदेश के राजाओं, ऋषियों और मुनियों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ को भव्य रूप से सजाया जाता है और यज्ञ के लिए एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है।
इस सर्ग में श्रीकृष्ण की राजनीतिक सूझबूझ और पांडवों के पराक्रम का सुंदर वर्णन है।
Step 3: Final Answer:
'आयोजन' सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संकल्प लेने, श्रीकृष्ण के परामर्श पर भीम द्वारा जरासंध का वध करने और इसके पश्चात् यज्ञ की भव्य तैयारियों का वर्णन किया गया है।
Quick Tip: उत्तर लिखते समय सर्ग के शीर्षक ('आयोजन') को कथावस्तु से जोड़ें। बताएं कि किस प्रकार सर्ग की घटनाएँ 'आयोजन' को सार्थक करती हैं।
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य के नायक भगवान श्रीकृष्ण हैं। यद्यपि काव्य पांडवों के राजसूय यज्ञ पर आधारित है, परन्तु श्रीकृष्ण ही केन्द्रीय पात्र हैं जो सभी घटनाओं को दिशा देते हैं। प्रश्न में उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'अग्रपूजा' खण्डकाव्य में भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं:
1. सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ: श्रीकृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ हैं। वे युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ से पहले जरासंध का वध करने की सलाह देते हैं, जो उनकी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता का प्रमाण है।
2. लोक-कल्याणकारी: श्रीकृष्ण का प्रत्येक कार्य लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। वे जरासंध का वध इसलिए करवाते हैं ताकि निर्दोष राजाओं को मुक्त किया जा सके और धर्म की स्थापना हो।
3. धर्म-संस्थापक: वे धर्म के पक्षधर हैं और अधर्म का नाश करना अपना कर्तव्य समझते हैं। वे पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
4. अलौकिक शक्ति-संपन्न: शिशुपाल वध के प्रसंग में श्रीकृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय देते हैं। वे ईश्वर के अवतार हैं।
5. शांत और गंभीर: वे अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में भी अपना संयम नहीं खोते। शिशुपाल द्वारा अपनी निंदा सुनकर भी वे शांत रहते हैं और सौ अपशब्द पूरे होने पर ही उसे दंड देते हैं।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'अग्रपूजा' के नायक श्रीकृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ, लोक-कल्याणकारी, धर्म-संस्थापक, अलौकिक शक्तियों से युक्त और शांत-गंभीर स्वभाव के महापुरुष हैं।
Quick Tip: किसी पौराणिक पात्र का चरित्र-चित्रण करते समय, उनकी मानवीय और दैवीय दोनों विशेषताओं का उल्लेख करें। इससे उत्तर संतुलित और पूर्ण होता है।
'मेवाड़-मुकुट' खण्डकाव्य के नायक का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'मेवाड़-मुकुट' खण्डकाव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं। यह काव्य हल्दीघाटी के युद्ध के बाद उनके संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाता है। प्रश्न में उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मेवाड़-मुकुट' खण्डकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. अद्वितीय देश-भक्त और स्वतंत्रता-प्रेमी: महाराणा प्रताप एक महान देश-भक्त हैं। वे मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। वे अकबर की अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा जंगलों में भटकना और कष्ट सहना श्रेयस्कर समझते हैं।
2. दृढ़-प्रतिज्ञ और साहसी: वे अपने संकल्प के धनी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे, तब तक महलों में नहीं रहेंगे और राजसी सुखों का त्याग करेंगे। वे इस प्रतिज्ञा पर अंत तक अटल रहे।
3. महान त्यागी और कष्ट-सहिष्णु: उन्होंने मातृभूमि के लिए राज-सुख, ऐश्वर्य और परिवार के सुखों का त्याग कर दिया। वे अरावली के जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटियाँ खाईं, पर झुके नहीं।
4. आदर्श पारिवारिक पुरुष: वे एक स्नेही पिता और पति हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को कष्ट में देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है, लेकिन कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होते।
5. स्वाभिमानी: महाराणा प्रताप का स्वाभिमान अद्वितीय है। वे किसी भी कीमत पर अपना आत्म-सम्मान और मेवाड़ का गौरव बेचना नहीं चाहते।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'मेवाड़-मुकुट' के नायक महाराणा प्रताप एक महान देश-भक्त, स्वतंत्रता-प्रेमी, दृढ़-प्रतिज्ञ, त्यागी, कष्ट-सहिष्णु और स्वाभिमानी योद्धा हैं।
Quick Tip: ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय, उनकी ऐतिहासिक छवि और काव्य में प्रस्तुत छवि, दोनों का संतुलन बनाए रखें। उनके मानवीय गुणों पर विशेष ध्यान दें।
'मेवाड़-मुकुट' के पंचम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'मेवाड़-मुकुट' खण्डकाव्य के पाँचवें सर्ग की कथावस्तु को संक्षेप में लिखने के लिए कहता है। इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पुत्री के दृष्टिकोण से कथा आगे बढ़ती है और भामाशाह के आगमन का संकेत मिलता है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मेवाड़-मुकुट' के पंचम सर्ग का शीर्षक 'चिंता' है। इसकी कथावस्तु इस प्रकार है:
यह सर्ग महाराणा प्रताप की पुत्री के एक स्वप्न से आरम्भ होता है। वह स्वप्न में देखती है कि उसकी माँ (रानी) एक भिखारिणी के वेश में है और उसे भोजन मांगना पड़ रहा है। वह भयभीत होकर जाग जाती है और अपनी माँ से इस स्वप्न के बारे में बताती है।
रानी अपनी पुत्री को समझाती है और उसे वीरांगनाओं की कथाएँ सुनाकर धैर्य बँधाती है। वह उसे बताती है कि देश के लिए कष्ट सहना गौरव की बात है।
इसी बीच, एक दौलत नाम की भीलनी वहाँ आती है। वह बहुत चिंतित और उदास है। वह रानी को बताती है कि उसने शत्रु के एक सैनिक को यह कहते सुना है कि दौलत बेगम (अकबर की पत्नी) प्रताप की पुत्री को अपनी पुत्री के रूप में पालना चाहती है।
यह सुनकर रानी चिंतित हो जाती है। उन्हें अपनी पुत्री की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। सर्ग के अंत में रानी इसी चिंता में डूबी हुई है कि कैसे अपनी पुत्री की रक्षा की जाए। यह सर्ग पारिवारिक चिंताओं और संघर्षों के बीच भी कर्तव्य-पथ पर डटे रहने की प्रेरणा देता है।
Step 3: Final Answer:
पंचम सर्ग में प्रताप की पुत्री द्वारा देखे गए बुरे स्वप्न, रानी द्वारा उसे धैर्य बँधाने और एक भीलनी द्वारा लाए गए चिंताजनक समाचार का वर्णन है, जिससे रानी अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हो जाती है।
Quick Tip: सर्ग का सारांश लिखते समय, यदि सर्ग का कोई शीर्षक (जैसे 'चिंता') है, तो उसे अपनी व्याख्या के केंद्र में रखें। बताएं कि सर्ग की घटनाएँ उस शीर्षक को कैसे सार्थक करती हैं।
'जय सुभाष' खण्डकाव्य के आधार पर सुभाषचन्द्र बोस का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'जय सुभाष' खण्डकाव्य के नायक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस हैं। इस प्रश्न में काव्य के आधार पर उनके ओजस्वी और प्रेरक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'जय सुभाष' खण्डकाव्य में कवि ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साहसी और क्रांतिकारी व्यक्तित्व को चित्रित किया है। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त: सुभाषचन्द्र बोस के जीवन का एकमात्र लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता थी। उन्होंने इस लक्ष्य के लिए अपना घर-परिवार, सुख-सुविधा सब कुछ त्याग दिया। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा" उनकी देशभक्ति का प्रतीक है।
2. कुशल संगठनकर्ता और ओजस्वी वक्ता: उन्होंने 'आजाद हिन्द फौज' का गठन करके अपनी अद्वितीय संगठन क्षमता का परिचय दिया। उनके भाषण अत्यंत प्रेरणादायक होते थे और वे अपने शब्दों से सैनिकों में जोश भर देते थे।
3. साहसी और निर्भीक: वे अत्यंत साहसी और निडर थे। अंग्रेजों की कैद से छद्म वेश में निकलकर जर्मनी और जापान पहुँचना उनके अदम्य साहस का प्रमाण है।
4. दृढ़-संकल्प: वे अपने निश्चय पर अडिग रहते थे। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प लिया, उस पर वे अंत तक कार्य करते रहे।
5. त्याग की प्रतिमूर्ति: उन्होंने आई.सी.एस. (I.C.S.) जैसी प्रतिष्ठित नौकरी को देश-सेवा के लिए त्याग दिया, जो उनके महान त्याग को दर्शाता है।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'जय सुभाष' के नायक सुभाषचन्द्र बोस एक महान देशभक्त, कुशल संगठनकर्ता, साहसी, दृढ़-संकल्प वाले और त्यागी महापुरुष हैं।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण में, पात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं (जैसे- कैद से भागना, आजाद हिन्द फौज का गठन) का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि ये घटनाएँ ही उनके चरित्र को परिभाषित करती हैं।
'जय सुभाष' खण्डकाव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'जय सुभाष' खण्डकाव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु को संक्षेप में लिखने के लिए कहता है। इस सर्ग में सुभाषचन्द्र बोस के भारत से बाहर जाने की योजना और उनके साहसिक पलायन का वर्णन है।
Step 2: Detailed Explanation:
'जय सुभाष' खण्डकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक इस प्रकार है:
पृष्ठभूमि: सर्ग का आरम्भ द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से होता है। सुभाषचन्द्र बोस को अंग्रेजों ने उनके कलकत्ता स्थित घर में नजरबंद कर दिया है। वे सोचते हैं कि इस समय अंग्रेजों के शत्रु देशों से मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए।
पलायन की योजना: सुभाष बाबू अंग्रेजों की कैद से बाहर निकलने की एक साहसिक योजना बनाते हैं। वे दाढ़ी बढ़ाकर और पठानी वेश धारण कर एक मौलवी का रूप धरते हैं। वे अपना नाम जियाउद्दीन रखते हैं।
साहसिक यात्रा: घोर संकटों और जोखिमों के बीच, वे अंग्रेजों की आँखों में धूल झोंककर अपने घर से निकलने में सफल हो जाते हैं। वे अपने भतीजे शिशिर की मदद से कार द्वारा गोमो स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़कर पेशावर के लिए निकल जाते हैं।
भारत से प्रस्थान: पेशावर से वे और भी कठिन यात्रा करते हुए काबुल पहुँचते हैं और अंततः जर्मनी जाने में सफल होते हैं।
इस सर्ग में सुभाष बाबू की दूरदर्शिता, उनकी योजना-निर्माण क्षमता और उनके अदम्य साहस का प्रभावशाली वर्णन किया गया है।
Step 3: Final Answer:
प्रथम सर्ग में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा अंग्रेजों की नजरबंदी से भागने की योजना बनाने, वेश बदलकर घर से निकलने और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत की सीमा से बाहर पहुँचने की साहसिक घटना का वर्णन है।
Quick Tip: किसी सर्ग का सारांश लिखते समय, स्थान और पात्रों के बदले हुए नामों (जैसे- सुभाष का जियाउद्दीन बनना) पर ध्यान दें, क्योंकि ये कथा के महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं।
'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र या नायक अमर शहीद चन्द्रशेखर 'आजाद' हैं। इस प्रश्न में उनके क्रांतिकारी और प्रेरणादायक चरित्र का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के आधार पर चन्द्रशेखर 'आजाद' की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. महान देशभक्त और स्वतंत्रता-प्रेमी: आजाद के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मातृभूमि की स्वतंत्रता थी। वे बचपन से ही स्वतंत्रता के दीवाने थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया।
2. अदम्य साहसी और वीर: वे वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति थे। उनका नाम 'आजाद' उनके इसी गुण का प्रतीक है। वे अंग्रेजों से कभी नहीं डरे और अंत तक उनका मुकाबला करते रहे।
3. दृढ़-प्रतिज्ञ: उन्होंने जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा की थी और अपनी अंतिम साँस तक इस प्रतिज्ञा को निभाया। अल्फ्रेड पार्क में जब वे चारों ओर से घिर गए, तो उन्होंने अपनी ही गोली से प्राण त्याग दिए, पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए।
4. कुशल संगठनकर्ता और नेता: वे एक कुशल नेता थे। उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी दल का सफलतापूर्वक संचालन किया।
5. त्यागी और बलिदानी: उन्होंने देश के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, परिवार और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'मातृभूमि के लिए' के नायक चन्द्रशेखर 'आजाद' एक महान देशभक्त, साहसी, वीर, दृढ़-प्रतिज्ञ, कुशल नेता और एक सच्चे बलिदानी थे।
Quick Tip: क्रांतिकारी पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय उनकी विचारधारा और उनके कार्यों के पीछे की प्रेरणा को उजागर करें। यह बताएं कि वे क्यों और किसके लिए लड़ रहे थे।
'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के तृतीय सर्ग (बलिदान) का कथानक संक्षेप में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के तीसरे और अंतिम सर्ग 'बलिदान' का सारांश लिखने के लिए कहता है। यह सर्ग चन्द्रशेखर आजाद के जीवन के अंतिम क्षणों और उनके बलिदान का वर्णन करता है।
Step 2: Detailed Explanation:
'मातृभूमि के लिए' खण्डकाव्य के तृतीय सर्ग 'बलिदान' का कथानक इस प्रकार है:
अल्फ्रेड पार्क की घटना: सर्ग का आरम्भ प्रयागराज (इलाहाबाद) के अल्फ्रेड पार्क के दृश्य से होता है। चन्द्रशेखर आजाद अपने एक साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं।
विश्वासघात और पुलिस का घेराव: तभी एक देशद्रोही की सूचना पर ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक नॉट बाबर भारी पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचता है और पार्क को चारों ओर से घेर लेता है।
वीरतापूर्ण संघर्ष: आजाद अपने साथी को सुरक्षित भगा देते हैं और अकेले ही पुलिस से लोहा लेने लगते हैं। वे एक पेड़ की आड़ लेकर अपनी पिस्तौल से अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। वे कई पुलिसवालों को घायल कर देते हैं और नॉट बाबर की कलाई भी जख्मी कर देते हैं।
अंतिम बलिदान: जब उनकी पिस्तौल में अंतिम गोली बचती है, तो वे अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं कि वे कभी भी जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आएँगे। वे उस अंतिम गोली को अपनी कनपटी पर मारकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं।
आजाद का यह बलिदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
Step 3: Final Answer:
तृतीय सर्ग में चन्द्रशेखर आजाद के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा घेर लिए जाने, उनके द्वारा वीरतापूर्वक संघर्ष करने और अंत में अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु स्वयं को गोली मारकर बलिदान देने की शौर्यपूर्ण गाथा का वर्णन है।
Quick Tip: किसी पात्र के बलिदान का वर्णन करते समय, घटना के भावनात्मक पहलू को भी उजागर करें। बताएं कि उस बलिदान का क्या महत्व और प्रभाव पड़ा।
'कर्ण' खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग (द्यूत सभा में द्रौपदी) की कथावस्तु लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'कर्ण' खण्डकाव्य के दूसरे सर्ग की कथावस्तु लिखने के लिए कहता है, जो महाभारत की कुख्यात 'द्यूत-क्रीड़ा' (जुआ) और द्रौपदी के चीर-हरण की घटना पर केंद्रित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'कर्ण' खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु इस प्रकार है:
द्यूत-क्रीड़ा का आयोजन: सर्ग का आरम्भ हस्तिनापुर की द्यूत-सभा से होता है, जहाँ शकुनि की कुटिल चालों के कारण युधिष्ठिर अपना सब कुछ - राज्य, धन, अपने भाइयों और स्वयं को भी हार जाते हैं।
द्रौपदी को दाँव पर लगाना: अंत में, दुर्योधन के उकसाने पर, युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाँव पर लगा देते हैं और उसे भी हार जाते हैं।
द्रौपदी का अपमान: दुर्योधन अपने भाई दुःशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आए। दुःशासन द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी सभा में उपस्थित गुरुजनों - भीष्म, द्रोण, विदुर - से न्याय की भीख माँगती है, पर सब मौन रहते हैं।
कर्ण की भूमिका: इस अवसर पर, दुर्योधन के मित्र होने के नाते और द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में किए गए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए, कर्ण भी द्रौपदी का अपमान करते हैं। वे उसे 'वेश्या' कहते हैं और दुःशासन को उसके वस्त्र उतारने के लिए उकसाते हैं।
चीर-हरण और श्रीकृष्ण की कृपा: जब दुःशासन द्रौपदी का चीर-हरण करने का प्रयास करता है, तो द्रौपदी भगवान श्रीकृष्ण को पुकारती है। श्रीकृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती है और दुःशासन थककर हार जाता है।
यह सर्ग कौरवों के अधर्म और उस सभा में उपस्थित महापुरुषों की विवशता को दर्शाता है।
Step 3: Final Answer:
द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा जुए में सब कुछ हारने, द्रौपदी को दाँव पर लगाने, भरी सभा में दुःशासन द्वारा उसका अपमान करने, कर्ण द्वारा कटु वचन कहने और अंत में श्रीकृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बचने की घटना का वर्णन है।
Quick Tip: महाभारत जैसे प्रसिद्ध प्रसंगों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय, सुनिश्चित करें कि आप घटनाओं का सही क्रम और प्रमुख पात्रों की भूमिका का सटीक वर्णन करें।
'कर्ण' खण्डकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्रांकन कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'कर्ण' खण्डकाव्य के नायक दानवीर कर्ण हैं। यह प्रश्न महाभारत के इस महान, किन्तु悲극 (tragic) पात्र के चरित्र की विशेषताओं का काव्य के आधार पर विश्लेषण करने के लिए कहता है।
Step 2: Detailed Explanation:
'कर्ण' खण्डकाव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्रांकन इस प्रकार है:
1. महान धनुर्धर और वीर योद्धा: कर्ण अर्जुन के समान ही एक महान धनुर्धर थे। उनकी वीरता और युद्ध-कौशल से सभी परिचित थे।
2. दानवीर: कर्ण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन-रक्षक कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिए, यह जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित है। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था।
3. सच्चा मित्र: कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता के लिए जाने जाते हैं। दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया, इसलिए कर्ण ने अधर्म का साथ देते हुए भी अंत तक अपनी मित्रता निभाई।
4. जाति-प्रथा से पीड़ित: कर्ण को जीवन भर 'सूत-पुत्र' होने के कारण अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में और द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा न दिए जाने की घटनाएँ उनके जीवन की बड़ी त्रासदियाँ हैं। यह अपमान उनके मन में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न करता है।
5. स्वाभिमानी: कर्ण अत्यंत स्वाभिमानी थे। वे किसी का अहसान नहीं लेना चाहते थे और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते थे।
6.悲극 नायक (Tragic Hero): इन सभी गुणों के बावजूद, कर्ण का जीवन एक त्रासदी है। वे गुणी होते हुए भी परिस्थितियों के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं और अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं।
Step 3: Final Answer:
अतः, कर्ण एक महान योद्धा, अद्वितीय दानवीर, सच्चे मित्र और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जिनका जीवन सामाजिक तिरस्कार और परिस्थितियों की विडंबना के कारण एक悲극 (tragic) नायक के रूप में समाप्त होता है।
Quick Tip: 'Tragic Hero' या悲劇 नायक का चरित्र-चित्रण करते समय, उनके गुणों के साथ-साथ उनके जीवन की विडंबनाओं और उन कारणों का भी उल्लेख करें जिनकी वजह से उनका अंत悲劇पूर्ण हुआ।
'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य रामायण के पात्र भरत के चरित्र पर केंद्रित है। इस प्रश्न में काव्य की सम्पूर्ण कथावस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य की कथावस्तु भरत के महान त्याग और भ्रातृ-प्रेम पर आधारित है। इसका सारांश इस प्रकार है:
राम का वनगमन और भरत की वापसी: काव्य का आरम्भ राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन के बाद होता है। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या को सूना और श्रीहीन देखकर वे चिंतित हो जाते हैं।
भरत का विलाप: जब उन्हें अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र का पता चलता है कि उनके कारण ही राम को वनवास हुआ है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित होते हैं। वे अपनी माता की बहुत भर्त्सना करते हैं और स्वयं को इस अनर्थ का कारण मानकर ग्लानि से भर जाते हैं।
चित्रकूट की यात्रा: भरत निश्चय करते हैं कि वे राम को वन से वापस लाकर राजगद्दी सौंपेंगे। वे अयोध्यावासियों, तीनों माताओं और सेना के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं।
राम-भरत मिलाप: चित्रकूट में राम और भरत का भावुक मिलन होता है। भरत राम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने का आग्रह करते हैं।
पादुका लेकर लौटना: जब राम पिता के वचन का मान रखने के लिए लौटने से इंकार कर देते हैं, तो भरत उनकी खड़ाऊँ (पादुका) को सिंहासन पर रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करने का निश्चय करते हैं।
तपस्वी जीवन: भरत अयोध्या लौटकर राजमहल में न रहकर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और चौदह वर्षों तक राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर एक सेवक की भांति राज-काज चलाते हैं।
Step 3: Final Answer:
इस काव्य में भरत द्वारा ननिहाल से लौटने पर राम-वनगमन का समाचार पाकर दुखी होने, राम को मनाने चित्रकूट जाने, और उनके न लौटने पर उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर चौदह वर्षों तक तपस्वी के रूप में राज्य का संचालन करने की त्यागमयी कथा है।
Quick Tip: कथावस्तु लिखते समय, कहानी के मुख्य मोड़ों (turning points) पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे - भरत का लौटना, कैकेयी पर क्रोध, चित्रकूट यात्रा, और पादुका-शासन।
'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य के आधार पर 'कौशल्या-सुमित्रा मिलन' नामक तृतीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य के तीसरे सर्ग, जिसका शीर्षक 'कौशल्या-सुमित्रा मिलन' है, की कथावस्तु को लिखने के लिए कहता है। यह सर्ग राम के वनगमन के बाद दोनों माताओं के दुःख और उनके संवाद पर केंद्रित है।
Step 2: Detailed Explanation:
'कर्मवीर भरत' खण्डकाव्य के तृतीय सर्ग 'कौशल्या-सुमित्रा मिलन' की कथावस्तु इस प्रकार है:
कौशल्या का दुःख: सर्ग का आरम्भ राम के वन चले जाने के बाद माता कौशल्या के गहरे दुःख से होता है। वे अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं और रो रही हैं। उनकी आँखों के आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे राम के बचपन की लीलाओं को याद करके और भी दुखी हो जाती हैं।
सुमित्रा का आगमन: तभी वहाँ सुमित्रा आती हैं। वे स्वयं भी अपने पुत्र लक्ष्मण के वियोग में दुखी हैं, लेकिन वे कौशल्या से अधिक धैर्यवान और ज्ञानी हैं। वे कौशल्या को सांत्वना देने का प्रयास करती हैं।
दोनों माताओं का संवाद: सुमित्रा कौशल्या को समझाती हैं कि राम केवल उनके पुत्र नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के रक्षक हैं। वे धर्म की स्थापना और राक्षसों का संहार करने के लिए ही वन गए हैं। वे कहती हैं कि लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की सेवा करने के पुण्य कार्य के लिए गए हैं, अतः हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए।
सुमित्रा का आदर्श चरित्र: सुमित्रा के ज्ञानपूर्ण वचनों को सुनकर कौशल्या को धैर्य मिलता है। इस सर्ग में सुमित्रा का एक आदर्श, धैर्यवान और विवेकशील नारी के रूप में चरित्र उभरकर सामने आता है। वे कौशल्या को उनके कर्तव्य का बोध कराती हैं।
यह सर्ग दो माताओं के दुःख के माध्यम से त्याग, कर्तव्य और धर्म के महत्व को दर्शाता है।
Step 3: Final Answer:
तृतीय सर्ग में राम के वनगमन के पश्चात् शोकमग्न कौशल्या और धैर्यशीला सुमित्रा के बीच हुए संवाद का वर्णन है। सुमित्रा अपने ज्ञानपूर्ण वचनों से कौशल्या को सांत्वना देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि राम और लक्ष्मण धर्म की रक्षा के महान उद्देश्य से वन गए हैं, अतः हमें शोक के स्थान पर गर्व करना चाहिए।
Quick Tip: किसी विशेष सर्ग का उत्तर लिखते समय, उस सर्ग के शीर्षक को अपनी व्याख्या का आधार बनाएं। बताएं कि सर्ग की घटनाएँ 'कौशल्या-सुमित्रा मिलन' को कैसे चरितार्थ करती हैं और इस मिलन का क्या महत्व है।
'तुमुल' खण्डकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र-चित्रण कीजिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'तुमुल' खण्डकाव्य रामायण के लंका-कांड पर आधारित है, विशेषकर लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध पर। इसके प्रमुख पात्र लक्ष्मण हैं। प्रश्न में उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'तुमुल' खण्डकाव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. अतुलनीय भ्रातृ-भक्त: लक्ष्मण का चरित्र भ्रातृ-भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने अपने भाई राम की सेवा के लिए राज-सुख का त्याग कर दिया और चौदह वर्षों तक वन में उनके साथ रहे। वे राम की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं।
2. अदम्य साहसी और महान योद्धा: लक्ष्मण एक महान वीर और साहसी योद्धा हैं। वे अकेले ही मेघनाद जैसे अजेय योद्धा से युद्ध करने का निश्चय करते हैं। उनका रण-कौशल अद्भुत है और वे युद्ध में अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते।
3. शीघ्र क्रुद्ध होने वाले (आवेशी): लक्ष्मण का स्वभाव अत्यंत उग्र और आवेशपूर्ण है। वे अन्याय को सहन नहीं कर पाते और शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। उनका यही क्रोध उन्हें मेघनाद से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है।
4. कर्तव्यनिष्ठ और त्यागी: वे अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। भाई और भाभी की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। इसी कर्तव्य-भावना के कारण वे शक्ति-बाण लगने पर भी विचलित नहीं होते।
5. मानवता के प्रतीक: काव्य में उन्हें एक आदर्श मानव के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने संबंधों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है। उनका चरित्र मानवीय भावनाओं (क्रोध, प्रेम, सेवा) से परिपूर्ण है।
Step 3: Final Answer:
अतः, 'तुमुल' खण्डकाव्य के नायक लक्ष्मण एक आदर्श भाई, महान योद्धा, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, परन्तु आवेशपूर्ण स्वभाव के स्वामी हैं। उनका चरित्र त्याग और सेवा का प्रतीक है।
Quick Tip: चरित्र-चित्रण में पात्र के सकारात्मक गुणों के साथ-साथ यदि कोई नकारात्मक या मानवीय कमजोरी (जैसे लक्ष्मण का अत्यधिक क्रोध) हो, तो उसका भी संतुलित उल्लेख करें। इससे उत्तर यथार्थवादी लगता है।
'तुमुल' खण्डकाव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
'तुमुल' खण्डकाव्य का कथानक रामायण के लंका-युद्ध से लिया गया है। इसका केंद्रीय विषय लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुआ भयंकर युद्ध है। इस प्रश्न में सम्पूर्ण काव्य का सारांश प्रस्तुत करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
'तुमुल' खण्डकाव्य की कथावस्तु का सारांश इस प्रकार है:
युद्ध की पृष्ठभूमि: काव्य का आरम्भ लंका के युद्ध-क्षेत्र से होता है। रावण के कई वीर पुत्र और योद्धा मारे जा चुके हैं। अब रावण अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजता है।
मेघनाद का पराक्रम: मेघनाद युद्ध-भूमि में आकर अपनी मायावी शक्तियों से वानर-सेना में हाहाकार मचा देता है। वह राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बाँध देता है। गरुड़ के आने पर राम और लक्ष्मण मुक्त होते हैं।
लक्ष्मण का क्रोध और प्रतिज्ञा: मेघनाद के इस कृत्य से लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अकेले ही मेघनाद का वध करेंगे। राम और विभीषण उन्हें समझाते हैं, क्योंकि मेघनाद को मारना बहुत कठिन था।
लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध: लक्ष्मण किसी की नहीं सुनते और मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर और विनाशकारी युद्ध होता है। देवता भी इस युद्ध को देखकर चकित रह जाते हैं।
शक्ति-बाण और लक्ष्मण का मूर्छित होना: युद्ध के दौरान मेघनाद अपनी कुलदेवी से प्राप्त अमोघ शक्ति-बाण का प्रयोग लक्ष्मण पर करता है। बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।
संजीवनी बूटी और लक्ष्मण का पुनर्जीवन: लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करने लगते हैं। विभीषण के कहने पर हनुमानजी संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा होती है।
मेघनाद का वध: स्वस्थ होने पर लक्ष्मण पुनः मेघनाद से युद्ध करते हैं और अंत में उसका वध कर देते हैं, जिससे राम की सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है।
Step 3: Final Answer:
'तुमुल' खण्डकाव्य में लंका-युद्ध के दौरान मेघनाद द्वारा राम-लक्ष्मण को नागपाश में बाँधने, लक्ष्मण द्वारा क्रोधित होकर मेघनाद-वध की प्रतिज्ञा करने, दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने, लक्ष्मण को शक्ति-बाण लगने, हनुमान द्वारा संजीवनी लाकर उनके प्राण बचाने और अंत में लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध करने का वीरतापूर्ण वर्णन है।
Quick Tip: किसी भी खण्डकाव्य का सारांश लिखते समय, कथा के प्रारम्भ, मध्य (चरमोत्कर्ष), और अंत का स्पष्ट उल्लेख करें। 'तुमुल' में चरमोत्कर्ष लक्ष्मण को शक्ति लगना और अंत मेघनाद का वध है।
निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन-परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए :
(i) जयशंकर प्रसाद
(ii) भगवत शरण उपाध्याय
(iii) रामधारी सिंह 'दिनकर'
(iv) जयप्रकाश भारती
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
इस प्रश्न में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन-परिचय, साहित्यिक योगदान और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। हम यहाँ 'जयशंकर प्रसाद' का जीवन-परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।
Step 2: Detailed Explanation:
जयशंकर प्रसाद (1889 ई. - 1937 ई.)
जीवन-परिचय:
छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सम्पन्न वैश्य परिवार में सन् 1889 ई. में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीप्रसाद था। परिवार का मुख्य व्यवसाय तम्बाकू का था, और वे 'सुँघनी साहू' के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के बाल्यकाल में ही उनके माता-पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार का सारा भार उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने घर पर ही हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। अत्यधिक परिश्रम और जीवन के संघर्षों के कारण वे क्षय रोग (टी.बी.) से ग्रस्त हो गए और मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में सन् 1937 ई. में उनका निधन हो गया।
साहित्यिक परिचय:
जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे एक महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबन्धकार थे। उनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ीबोली है।
प्रमुख रचना:
कामायनी: यह प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन के विकास की कथा को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है।
अन्य रचनाएँ:
नाटक: चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु।
उपन्यास: कंकाल, तितली, इरावती (अपूर्ण)।
कहानी-संग्रह: आकाशदीप, इन्द्रजाल, आँधी।
Step 3: Final Answer:
अतः, जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रमुख स्तम्भ थे, जिनका महाकाव्य 'कामायनी' हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है।
Quick Tip: जीवन-परिचय लिखते समय, जन्म-मृत्यु की तिथियाँ, जन्म-स्थान, माता-पिता का नाम, और साहित्यिक युग का उल्लेख अवश्य करें। उत्तर को 'जीवन-परिचय', 'साहित्यिक परिचय' और 'प्रमुख रचनाएँ' जैसे शीर्षकों में बाँटने से उत्तर अधिक सुव्यवस्थित और पठनीय हो जाता है।
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन-परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए :
(i) तुलसीदास
(ii) बिहारीलाल
(iii) सुमित्रानंदन पंत
(iv) श्यामनारायण पाण्डेय
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
इस प्रश्न में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन-परिचय, साहित्यिक योगदान और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। हम यहाँ 'गोस्वामी तुलसीदास' का जीवन-परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।
Step 2: Detailed Explanation:
गोस्वामी तुलसीदास (1532 ई. - 1623 ई.)
जीवन-परिचय:
लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु अधिकतर विद्वान उनका जन्म बाँदा जिले के 'राजापुर' गाँव में सन् 1532 ई. में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, जिन्होंने इन्हें शिक्षा-दीक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। कहते हैं कि अपनी पत्नी की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये ईश्वर-भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। सन् 1623 ई. में काशी में इनका निधन हो गया।
साहित्यिक परिचय:
तुलसीदास जी भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के 'रामभक्ति शाखा' के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें 'हिन्दी साहित्य का सूर्य' कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में समन्वय की भावना स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में काव्य-रचना की।
प्रमुख रचना:
श्रीरामचरितमानस: यह तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध और विश्व-विख्यात महाकाव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान श्री राम के सम्पूर्ण जीवन का आदर्श रूप में वर्णन किया गया है। यह हिन्दू धर्म का एक पवित्र ग्रन्थ माना जाता है।
अन्य रचनाएँ:
विनय-पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण-गीतावली, जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल।
Step 3: Final Answer:
अतः, गोस्वामी तुलसीदास रामभक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि थे, जिनका महाकाव्य 'श्रीरामचरितमानस' भारतीय संस्कृति और साहित्य का गौरव है।
Quick Tip: कवियों का जीवन-परिचय लिखते समय उनकी काव्य-धारा (जैसे - भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद) और भाषा-शैली का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख रचना के बारे में एक-दो पंक्तियों में उसका महत्व भी बताएं।
अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खण्ड की पाठ्यवस्तु से कण्ठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न-पत्र में न आया हो ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
इस प्रश्न में अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खण्ड से कोई ऐसा श्लोक लिखना है जिसे आपने याद किया हो, और वह इस प्रश्न-पत्र में पहले से न दिया गया हो।
Step 2: Detailed Explanation:
यहाँ एक आदर्श श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है जो सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों में होता है और याद करने में सरल है।
श्लोक:
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।
हिन्दी अनुवाद:
सब सुखी हों, सब निरोगी (रोग-मुक्त) हों।
सब कल्याण देखें (सबका भला हो), और कोई भी दुःख का भागी न बने।
Step 3: Final Answer:
उपरोक्त श्लोक और उसका अर्थ प्रश्न की आवश्यकता को पूरा करता है। यह श्लोक प्रश्न-पत्र में दिए गए श्लोकों से भिन्न है।
Quick Tip: परीक्षा के लिए हमेशा 2-3 सरल और महत्वपूर्ण श्लोक उनके अर्थ सहित याद कर लें। इससे यदि कोई एक श्लोक प्रश्न-पत्र में आ भी जाए, तो आपके पास लिखने के लिए दूसरा विकल्प मौजूद रहेगा। श्लोक को शुद्ध रूप में लिखना बहुत आवश्यक है।
आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएँ बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न एक औपचारिक पत्र (प्रार्थना-पत्र) लिखने के लिए है। पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को संबोधित है और इसका विषय विद्यालय में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने का अनुरोध करना है।
Step 2: Detailed Explanation:
पत्र का प्रारूप:
सेवा में,
प्रधानाचार्य महोदय,
[अपने विद्यालय का नाम],
[विद्यालय का पता - शहर का नाम]
दिनांक: [आज की तारीख]
विषय: खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र।
महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा दसवीं 'अ' का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में खेल सुविधाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
हमारे विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, परन्तु खेल-कूद की सुविधाओं का अभाव है। विद्यालय में खेल का मैदान तो है, लेकिन वह समतल नहीं है और उसमें घास उगी हुई है। इसके अतिरिक्त, छात्रों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे-बैट, बॉल, नेट आदि, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस कारण हम छात्र खेल-कूद की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जबकि शारीरिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी अत्यंत आवश्यक हैं।
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया विद्यालय में खेल के मैदान को ठीक कराने और खेल का पर्याप्त सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम सब छात्र इसके लिए आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद!
आपका आज्ञाकारी शिष्य,
[अपना नाम]
कक्षा - १० (अ)
अनुक्रमांक - [अपना रोल नंबर]
Step 3: Final Answer:
यह पत्र औपचारिक पत्र के सही प्रारूप का पालन करता है और विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या और अनुरोध को प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करता है।
Quick Tip: औपचारिक पत्र लिखते समय भाषा की शालीनता और विनम्रता का विशेष ध्यान रखें। विषय (Subject) स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में अपनी पहचान (नाम, कक्षा) और दिनांक का उल्लेख करना न भूलें।
आपके जन्मदिन पर दादा जी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है। दादा जी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए ।
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न एक अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए है। यह पत्र अपने दादाजी को उनके द्वारा भेजे गए जन्मदिन के उपहार (पुस्तक) के लिए धन्यवाद देने हेतु लिखा जाना है।
Step 2: Detailed Explanation:
पत्र का प्रारूप:
अपना पता,
शहर का नाम
दिनांक: [आज की तारीख]
आदरणीय दादा जी,
सादर चरण स्पर्श।
मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप और दादी जी भी वहाँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे।
दादा जी, मुझे कल ही आपका भेजा हुआ स्नेहपूर्ण पत्र और उपहार मिला। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजी गई 'भारत की खोज' नामक पुस्तक पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यह मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार है। मुझे ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है और यह पुस्तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक से मुझे अपने देश के गौरवशाली इतिहास को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। इस सुंदर और उपयोगी उपहार के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।
दादी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपके पत्र का इंतजार रहेगा।
आपका प्रिय पोता,
अपना नाम
Step 3: Final Answer:
यह पत्र अनौपचारिक पत्र के सही प्रारूप का पालन करता है और दादाजी के प्रति स्नेह और कृतज्ञता का भाव प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है।
Quick Tip: अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों, मित्रों या संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनकी भाषा आत्मीय और स्नेहपूर्ण होती है। पत्र के आरम्भ में अभिवादन (जैसे - सादर चरण स्पर्श, नमस्ते) और अंत में संबंध के अनुसार समापन (जैसे - आपका प्रिय पोता, तुम्हारा मित्र) का प्रयोग करें।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए :
दानं कस्य मित्रं भवति ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'जीवन-सूत्राणि' पाठ में वर्णित यक्ष-युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। इसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है।
Step 2: Detailed Explanation:
यक्ष के प्रश्न "किंस्विद् मित्रं मरिष्यतः?" (मरने वाले का मित्र कौन है?) के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, "दानं मित्रं मरिष्यतः।" (दान मरने वाले का मित्र है)।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा जीवन में किया गया दान ही मृत्यु के पश्चात् परलोक में उसका साथ देता है।
अतः, प्रश्न "दानं कस्य मित्रं भवति?" का उत्तर होगा "दानं मरिष्यतः मित्रं भवति।"
Step 3: Final Answer:
The final answer in Sanskrit is: दानं मरिष्यतः मित्रं भवति। (दान मरने वाले का मित्र होता है।)
Quick Tip: संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर देते समय, प्रश्नवाचक शब्द (जैसे - कस्य, केन, कुत्र, किम्) के स्थान पर सही उत्तर शब्द रखकर वाक्य को पूरा करें। इससे व्याकरण की दृष्टि से उत्तर सही बनता है।
विद्या केन वर्धते ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न एक सामान्य सूक्ति पर आधारित है, जिसमें पूछा गया है कि विद्या (ज्ञान) किस प्रकार बढ़ती है।
Step 2: Detailed Explanation:
संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है - "अनभ्यासे विषं विद्या", अर्थात अभ्यास के बिना विद्या विष के समान हो जाती है।
इसका तात्पर्य है कि विद्या को बढ़ाने का एकमात्र साधन निरंतर अभ्यास है।
अतः, प्रश्न "विद्या केन वर्धते?" (विद्या किससे बढ़ती है?) का उत्तर होगा "विद्या अभ्यासेन वर्धते।" (विद्या अभ्यास से बढ़ती है)।
Step 3: Final Answer:
The final answer in Sanskrit is: विद्या अभ्यासेन वर्धते। (विद्या अभ्यास से बढ़ती है।)
Quick Tip: सूक्ति-आधारित प्रश्नों के लिए, अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई महत्वपूर्ण सूक्तियों और उनके अर्थों को अच्छी तरह याद कर लें। ये अक्सर एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
कुत्र मरणं मङ्गलं भवति ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'वाराणसी' नामक पाठ से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कहाँ पर मरना मंगलकारी (शुभ) माना जाता है।
Step 2: Detailed Explanation:
पाठ के अनुसार, वाराणसी एक पवित्र नगरी है। यहाँ की मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पाठ में एक पंक्ति है: "अत्र मरणं मङ्गलम् भवति", जहाँ 'अत्र' का अर्थ 'यहाँ' अर्थात 'वाराणसी में' है।
अतः, प्रश्न "कुत्र मरणं मङ्गलं भवति?" (कहाँ मरना मंगलकारी होता है?) का उत्तर होगा "वाराणस्यां मरणं मङ्गलं भवति।"
Step 3: Final Answer:
The final answer in Sanskrit is: वाराणस्यां मरणं मङ्गलं भवति। (वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है।)
Quick Tip: पाठ-आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय, पाठ की विषय-वस्तु को याद रखना आवश्यक है। प्रश्नवाचक शब्द 'कुत्र' (कहाँ) का उत्तर हमेशा किसी स्थानवाचक शब्द में होता है, जैसे यहाँ 'वाराणस्याम्' (वाराणसी में)।
चन्द्रशेखरः स्वपितुः नाम किम् अकथयत् ?
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न 'देशभक्तः चन्द्रशेखरः' पाठ से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि चन्द्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया था।
Step 2: Detailed Explanation:
पाठ के अनुसार, जब किशोर चन्द्रशेखर को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो न्यायाधीश ने उनसे उनके पिता का नाम पूछा।
इसके उत्तर में चन्द्रशेखर ने गर्व से कहा, "स्वतन्त्रः" (स्वतंत्र)।
अतः, प्रश्न "चन्द्रशेखरः स्वपितुः नाम किम् अकथयत्?" (चन्द्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या कहा?) का उत्तर होगा "चन्द्रशेखरः स्वपितुः नाम 'स्वतन्त्रः' इति अकथयत्।"
Step 3: Final Answer:
The final answer in Sanskrit is: चन्द्रशेखरः स्वपितुः नाम 'स्वतन्त्रः' इति अकथयत्। (चन्द्रशेखर ने अपने पिता का नाम 'स्वतन्त्र' बताया।)
Quick Tip: किसी के द्वारा कहे गए कथन को संस्कृत में लिखते समय, उस कथन को एकल उद्धरण चिह्न (' ') में रखकर 'इति' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि उत्तर में 'स्वतन्त्रः' इति अकथयत्' लिखा गया है।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिए :
(i) मेरा प्रिय साहित्यकार
(ii) वृक्ष धरा के आभूषण
(iii) राष्ट्रीय एकता
(iv) बेरोजगारी : समस्या और समाधान
(v) मोबाइल फोन : वरदान या अभिशाप
View Solution
Step 1: Understanding the Concept:
इस प्रश्न में दिए गए विषयों में से किसी एक पर एक संरचित निबंध लिखना है। हम यहाँ विषय '(v) मोबाइल फोन : वरदान या अभिशाप' पर एक आदर्श निबंध प्रस्तुत कर रहे हैं।
Step 2: Detailed Explanation:
मोबाइल फोन : वरदान या अभिशाप
प्रस्तावना:
विज्ञान के इस युग में अनगिनत आविष्कार हुए हैं, जिन्होंने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इन्हीं आविष्कारों में से एक है 'मोबाइल फोन'। आज यह छोटा-सा उपकरण केवल बात करने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसने दुनिया को हमारी मुट्ठी में कैद कर दिया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार मोबाइल फोन के लाभ हैं तो हानियाँ भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे वरदान बनाते हैं या अभिशाप।
मोबाइल फोन : एक वरदान (लाभ):
मोबाइल फोन आधुनिक जीवन के लिए एक महान वरदान है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
1. संचार का सुगम साधन: मोबाइल फोन के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क साध सकते हैं। वीडियो कॉलिंग ने तो दूरियों को और भी कम कर दिया है।
2. ज्ञान का भंडार: इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन ज्ञान का असीमित भंडार है। छात्र किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
3. मनोरंजन का उत्तम माध्यम: मोबाइल फोन पर हम संगीत सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। यह हमारे खाली समय का अच्छा साथी है।
4. दैनिक जीवन में सहायक: ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग, रास्ता खोजने के लिए जीपीएस (GPS), और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाओं ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है।
मोबाइल फोन : एक अभिशाप (हानियाँ):
मोबाइल फोन का अत्यधिक और विवेकहीन उपयोग इसे एक अभिशाप बना देता है। इसकी प्रमुख हानियाँ इस प्रकार हैं:
1. स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव: मोबाइल फोन के निरंतर उपयोग से आँखों पर जोर पड़ता है, गर्दन और पीठ में दर्द की समस्या होती है। इसकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद को भी प्रभावित करती है।
2. समय की बर्बादी और लत: सोशल मीडिया और गेम्स की लत के कारण युवा और बच्चे अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं।
3. सामाजिक दूरी: आज लोग एक-दूसरे के साथ बैठकर भी अपने-अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं।
4. साइबर अपराध: मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और गलत सूचनाओं (अफवाहों) का प्रसार जैसी समस्याएँ बढ़ गई हैं।
उपसंहार:
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन स्वयं में न तो वरदान है और न ही अभिशाप। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग मानव के विवेक पर निर्भर करता है। यदि हम इसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, ज्ञान-प्राप्ति और अच्छे कार्यों के लिए सीमित और संतुलित रूप से करते हैं, तो यह निश्चय ही एक वरदान है। परन्तु यदि हम इसके आदी हो जाते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए एक भयंकर अभिशाप सिद्ध हो सकता है। हमें इसका दास नहीं, बल्कि स्वामी बनकर इसका उपयोग करना चाहिए।
Step 3: Final Answer:
The essay provides a balanced view on the topic "Mobile Phone: Boon or Bane," covering its introduction, advantages, disadvantages, and a concluding thought, structured as required.
Quick Tip: निबंध लिखते समय, रूपरेखा बनाना बहुत सहायक होता है। अपने निबंध को प्रस्तावना, विषय-विस्तार (लाभ-हानि, कारण-परिणाम), और उपसंहार जैसे भागों में विभाजित करें। प्रत्येक भाग में विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।
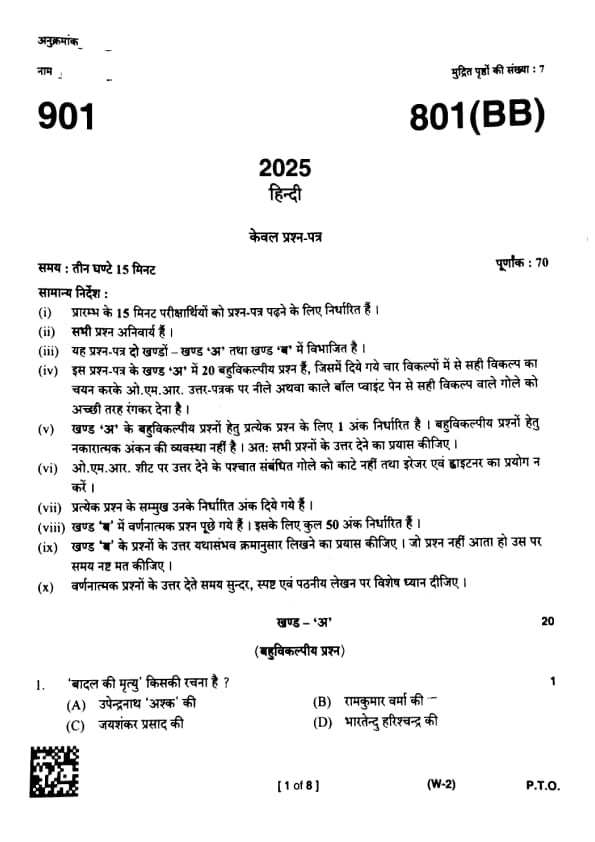
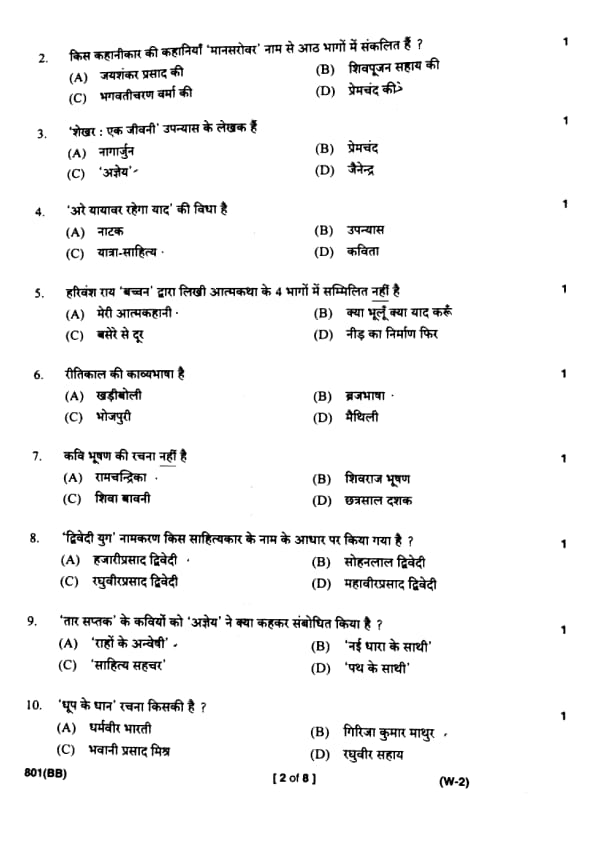
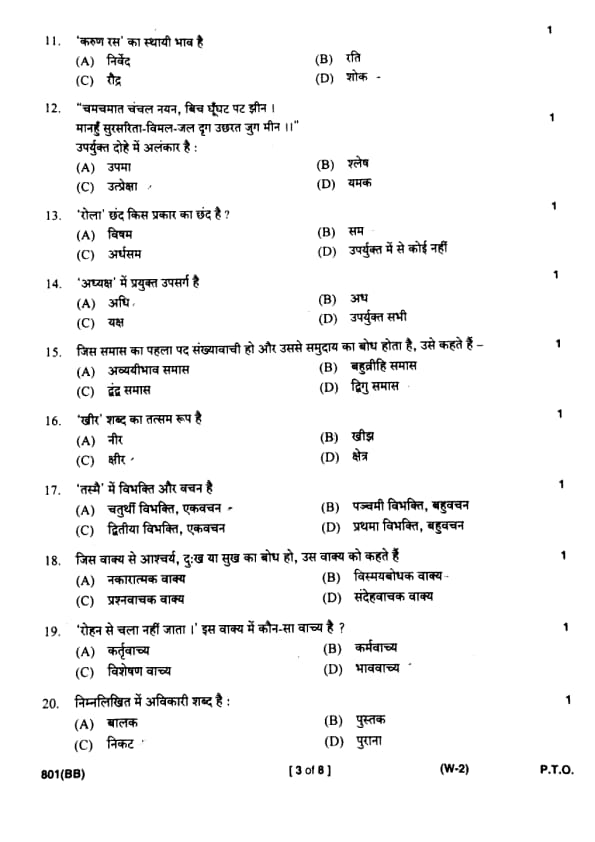
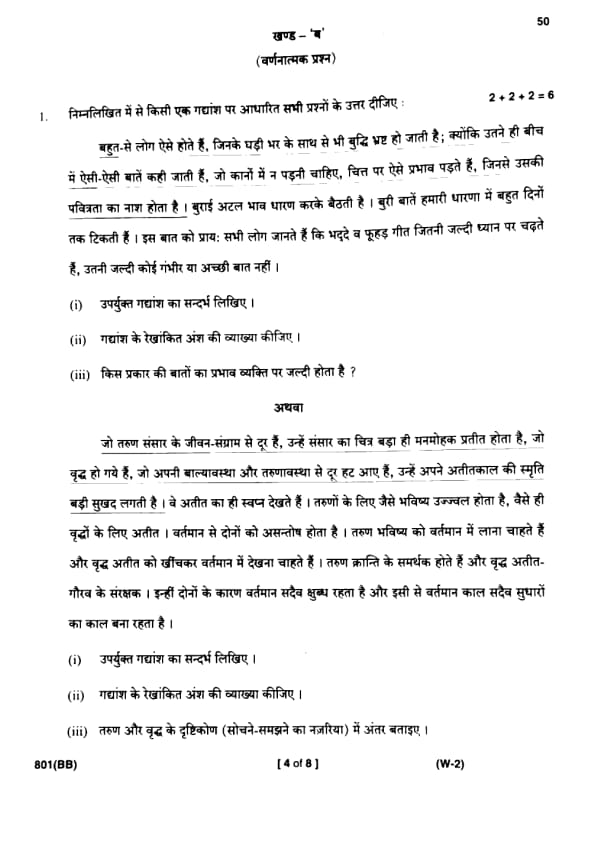
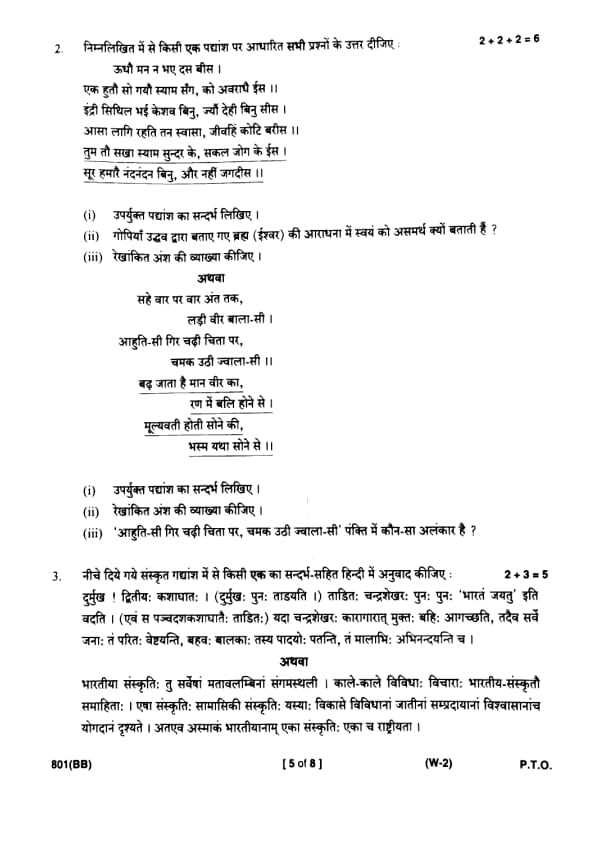
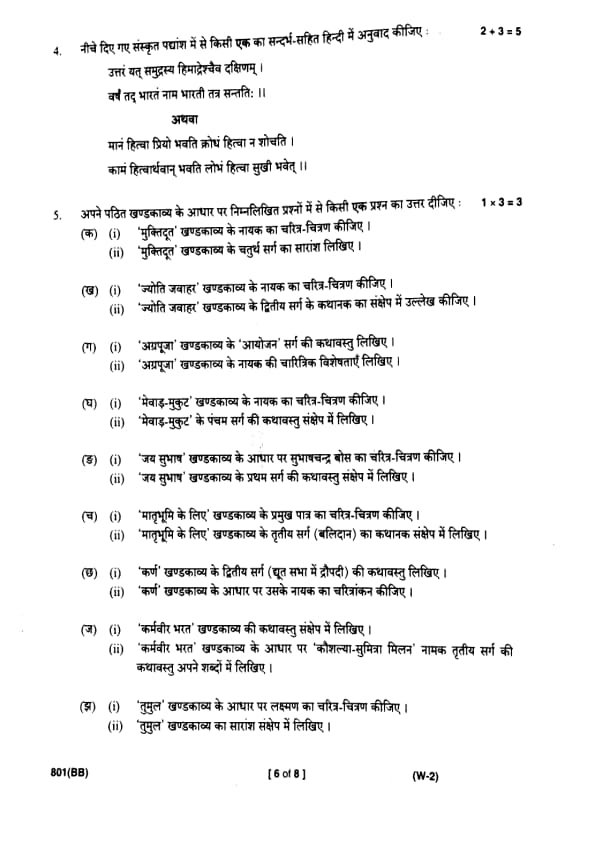
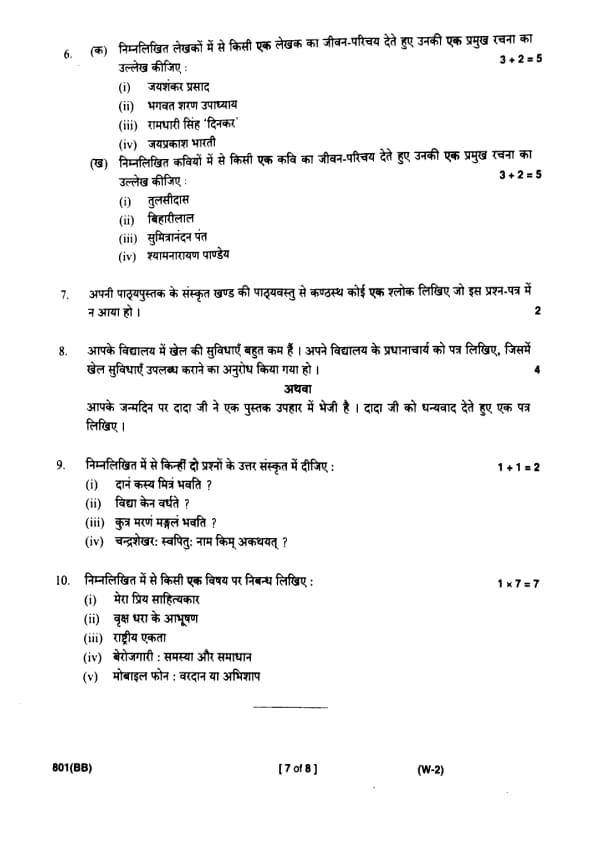





Comments