The Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) conducted the Class 10 Hindi Elementary Code 802 exam in the scheduled session. The medium of the paper was Hindi. The question paper included both objective and descriptive questions. An official answer key or solution set was released to help students assess their performance.
UP Board Class 10 Hindi Elementary (Code 802) Question Paper with Answer Key
| UP Board Class 12 Hindi Elementary (Code 802) Question Paper with Solutions PDF | Download PDF | Check Solutions |
‘कंकाल’ किस विधा की रचना है?
View Solution
Step 1: कृति की पहचान.
‘कंकाल’ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिन्होंने कविता, नाटक तथा गद्य—सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
Step 2: विधागत निर्धारण.
‘कंकाल’ उपन्यास विधा का ग्रंथ है; यह नाटक/आत्मकथा/रेखाचित्र नहीं है।
Step 3: विकल्प-परीक्षण.
(1) नाटक — गलत; प्रसाद के नाटक ‘स्कंदगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’ आदि हैं।
(2) आत्मकथा — गलत; ‘कंकाल’ आत्मकथात्मक नहीं।
(3) उपन्यास — सही; मान्य विधा यही है।
(4) रेखाचित्र — गलत; यह लघु गद्य-विधा है।
Quick Tip: लेखक-रचना-सूची याद रखें—शीर्षक देखकर विधा पहचानना आसान होता है।
‘वैशाली में वसन्त’ किसका नाटक है?
View Solution
Step 1: तथ्य-स्मरण.
‘वैशाली में वसन्त’ लक्ष्मी नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक है।
Step 2: विकल्प-अपवर्जन.
(1) उपेन्द्रनाथ अश्क — प्रमुख नाटककार/एकांकिकार, पर यह शीर्षक उनका नहीं।
(2) जयशंकर प्रसाद — उनके नाटक ‘स्कंदगुप्त’, ‘चंद्रगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’ आदि हैं।
(3) सेठ गोविन्द दास — साहित्य/संस्कृति-जगत के नाटककार, किन्तु यह कृति उनकी नहीं।
(4) लक्ष्मी नारायण मिश्र — सही।
Quick Tip: ऐतिहासिक-सांस्कृतिक नाटकों में प्रसाद और मिश्र—दोनों के नाम आते हैं; शीर्षक-लेखक जोड़ियों को अलग-अलग याद रखें।
जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं?
View Solution
Step 1: युग-सीमा.
हिंदी काव्य में छायावाद लगभग 1918–1936 माना जाता है।
Step 2: प्रतिनिधि कवि.
छायावाद के चार स्तंभ—प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी—हैं; प्रसाद जी की ‘कामायनी’, ‘झरना’, ‘आँसू’ आदि इसी प्रवृत्ति की कृतियाँ हैं।
Step 3: विकल्प-जांच.
(1) भारतेन्दु-युग — 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध; असंगत।
(2) शुक्ल-युग — आलोचनात्मक परंपरा से संबद्ध; प्रसाद का उत्कर्ष बाद का है।
(3) द्विवेदी-युग — 1900–1918; छायावाद से पूर्व।
(4) छायावाद-युग — सही।
Quick Tip: युग-आधारित प्रश्नों में समय-सीमा और प्रतिनिधि रचनाकार—दोनों को साथ में याद करें।
ऐतिहासिक उपन्यासकार है—
View Solution
Step 1: विधा की पहचान.
प्रश्न ऐतिहासिक उपन्यास के प्रतिनिधि लेखक के बारे में है।
Step 2: साक्ष्य.
वृन्दावनलाल वर्मा ‘झाँसी की रानी’, ‘मृणालिनी’, ‘कुँवर चंद्रसेन’ जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों हेतु प्रसिद्ध हैं।
Step 3: अपवर्जन.
(1) प्रेमचन्द — सामाजिक यथार्थ (‘गोदान’, ‘गबन’)।
(2) जैनेंद्र — मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति (‘त्यागपत्र’)।
(4) रेणु — आंचलिक उपन्यास (‘मैला आँचल’)।
अतः (3) सही उत्तर।
Quick Tip: उपन्यास-प्रकारों (ऐतिहासिक/सामाजिक/मनोवैज्ञानिक/आंचलिक) के साथ प्रतिनिधि लेखकों की सूची बनाकर अभ्यास करें।
शुक्लोत्तर-युग की समयावधि है—
View Solution
Step 1: पद का अर्थ.
‘शुक्लोत्तर’ का आशय—आचार्य रामचंद्र शुक्ल/द्विवेदी-युग (≈1900–1918) के बाद का काल।
Step 2: युग-संबंध.
द्विवेदी-युग के पश्चात छायावाद (≈1918–1936) आता है, जिसे अनेक ग्रंथ शुक्लोत्तर के अंतर्गत रखते हैं।
Step 3: विकल्प-मिलान.
(1) 1918–1936 — उचित (छायावाद की मान्य अवधि)।
(2) 1843–1900 — भारतेन्दु-पूर्व/भारतेन्दु-युग; असंगत।
(3) 1900–1918 — द्विवेदी-युग; ‘शुक्लोत्तर’ नहीं।
(4) इनमें से कोई नहीं — निरस्त; (1) सही है।
Quick Tip: समय-सीमा स्मरण: भारतेन्दु (≈1868–1893) → द्विवेदी/शुक्ल (≈1900–1918) → शुक्लोत्तर/छायावाद (≈1918–1936) → छायावादोत्तर/प्रगतिवाद (≈1936–1950)।
‘आश्रयदाताओं की प्रशंसा’ निम्न में से किस काल/वाद की विशेषता रही है?
View Solution
Step 1: रीतिकाल का काव्य-परिदृश्य.
रीतिकाल (लगभग 1650–1850) में दरबारी संस्कृति प्रबल थी, जहाँ कवि प्रायः राजाओं/संरक्षकों (आश्रयदाताओं) की प्रशंसा में काव्य रचते थे।
Step 2: प्रवृत्तियों का मिलान.
रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ—श्रृंगार-चित्रण, नायिका-भेद, अलंकार-प्राधान्य, आश्रयदाताओं की वंदना—रहीं।
Step 3: विकल्प-जांच.
(1) रीतिवाद — सही; आश्रयदाता-स्तुति इसकी केन्द्रीय प्रवृत्ति थी।
(2) छायावाद — आत्मकेंद्रित/भावुक/प्रकृतिप्रिय काव्य; दरबारी स्तुति नहीं।
(3) अतिक्रियावाद — हिंदी में मान्य प्रमुख वाद नहीं।
(4) प्रगतिवाद — समाज-यथार्थ, वर्ग-चेतना; आश्रयदाता-स्तुति नहीं।
Quick Tip: रीतिकाल = दरबारी संस्कृति, श्रृंगार और आश्रयदाता-स्तुति; छायावाद = अंतर्मन, प्रकृति; प्रगतिवाद = समाज-यथार्थ।
सुमित्रानंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि हैं?
View Solution
Step 1: युग-परिचय.
छायावाद (1918–1936 के आसपास) के चार प्रमुख कवि—प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी—माने जाते हैं।
Step 2: पंत की प्रतिनिधि कृतियाँ.
‘पल्लव’, ‘गुंजन’, ‘युगांतर’ आदि काव्य-संग्रह छायावादी सौंदर्य-बोध के द्योतक हैं।
Step 3: विकल्प-जांच.
(1) प्रयोगवाद — नयी कविता से जुड़ी प्रवृत्ति; पंत का मूल परिचय नहीं।
(2) प्रगतिवाद — सामाजिक यथार्थ; पंत मुख्यतः छायावादी हैं।
(3) छायावाद — सही।
(4) नई कविता — उत्तर-छायावादी दौर; पंत का प्रमुख स्थान छायावाद में है।
Quick Tip: युग-आधारित प्रश्नों में प्रतिनिधि कवि-सूची याद रखें: छायावाद = प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी।
खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता हैं—
View Solution
Step 1: तथ्य.
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य ‘प्रिय प्रवास’ माना जाता है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ हैं।
Step 2: शेष विकल्पों का अपवर्जन.
(1) प्रसाद — ‘कामायनी’ महाकाव्य है पर छायावादी युग में; खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं।
(2) गुप्त — ‘भारत-भारती’ दीर्घ काव्य; महाकाव्य नहीं माना जाता।
(3) दिनकर — ‘रश्मिरथी’ ख्याति-प्राप्त, पर प्रथम नहीं।
(4) हरिऔध — सही; ‘प्रिय प्रवास’ के रचयिता।
Quick Tip: “प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य = ‘प्रिय प्रवास’ (हरिऔध)”—इसे सूत्र की तरह याद रखें।
‘राम की शक्ति-पूजा’ किसकी रचना है?
View Solution
Step 1: कृति-परिचय.
‘राम की शक्ति-पूजा’ निराला की प्रसिद्ध दीर्घ कविता है, जिसमें राम द्वारा शक्ति-आराधना का दार्शनिक-आध्यात्मिक चित्रण है।
Step 2: विकल्प-अपवर्जन.
(1) गुप्त — राष्ट्रवादी काव्य के लिए प्रसिद्ध; यह कृति उनकी नहीं।
(3) महादेवी — विषाद-भाव की कवयित्री; यह शीर्षक नहीं।
(4) पंत — छायावादी कवि; इस कृति के रचयिता नहीं।
Quick Tip: निराला = ‘राम की शक्ति-पूजा’, ‘सरोज-स्मृति’; महादेवी = ‘नीरजा’; पंत = ‘पल्लव’; प्रसाद = ‘कामायनी’।
‘गाँव के पार धुआँ’ किसके द्वारा रचित है?
View Solution
Step 1: कवि-परिचय.
गिरिजाकुमार माथुर नयी कविता/आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख कवि हैं; ‘गाँव के पार धुआँ’ उनकी प्रसिद्ध कविता है।
Step 2: विकल्प-अपवर्जन.
(2) अज्ञेय — नयी कविता के शिखर कवि, पर यह शीर्षक उनका नहीं।
(3) रघुवीर सहाय — समकालीन जीवन की व्यंग्यात्मक संवेदना; यह कविता उनकी नहीं।
(4) धर्मवीर भारती — ‘अंधायुग’, ‘कनुप्रिया’ के रचयिता; यह शीर्षक नहीं।
Quick Tip: शीर्षक-आधारित प्रश्नों में कवि-आंदोलन का संबंध जोड़ें: ‘गाँव के पार धुआँ’ → आधुनिक/नयी कविता → गिरिजाकुमार माथुर।
‘द्वंद्व’ समास की परिभाषा है—
View Solution
Step 1: समास का स्वरूप.
समास में दो (या अधिक) पद मिलकर एक पद बनाते हैं।
Step 2: ‘द्वंद्व’ की निशानी.
‘द्वंद्व’ समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और अर्थ ‘और’ का बोध कराते हैं, जैसे—\;‘राम-लक्ष्मण’, ‘दिन-रात’।
Step 3: विकल्प-मिलान.
(1) दोनों पद प्रधान — यही द्वंद्व है, अतः सही।
(2) उत्तरपद प्रधान — यह तत्पुरुष की विशेषता है।
(3) प्रथम पद प्रधान — यह सामान्यतः बहुव्रीहि/कर्मधारय पर लागू नहीं; द्वंद्व नहीं।
(4) तीसरा अर्थ — यह बहुव्रीहि की पहचान है।
Quick Tip: याद रखें—द्वंद्व: दोनों प्रधान; तत्पुरुष: उत्तरपद प्रधान; बहुव्रीहि: तीसरा अर्थ।
‘बादल’ का पर्याय है—
View Solution
Step 1: शब्दार्थ.
‘वारिद’ = ‘वर्षा देने वाला’ (बादल) — संस्कृत समास वर् (वर्षा) + द (देने वाला) से।
Step 2: अन्य विकल्पों का अर्थ.
(2) जलीधि = जल + निधि = सागर/समुद्र; बादल नहीं।
(3) वारिज = वारि (जल) + ज (जन्मा) = कमल; बादल नहीं।
(4) नीरज = नीर (जल) + ज (जन्मा) = कमल; बादल नहीं।
अतः बादल का पर्याय वारिद सही है।
Quick Tip: जल से जन्मे = वारिज/नीरज (कमल); जल का भंडार = जलीधि (समुद्र); वर्षा देने वाला = वारिद (बादल)।
‘कृतज्ञ’ (स्कैन में ‘कृतञ्ज/कूटज’ सा अस्पष्ट) का विलोम है—
View Solution
Step 1: शब्दार्थ.
कृतज्ञ = उपकार/सहायता याद रखने वाला, आभारी, grateful.
Step 2: विलोम-निर्धारण.
कृतघ्न = उपकार न मानने वाला, उपकार-विस्मरण करने वाला (ungrateful) — यह ‘कृतज्ञ’ का सीधा विलोम है।
Step 3: अन्य विकल्प क्यों नहीं.
(2) पापी = पाप करने वाला; आभार के विपरीत नहीं।
(3) उपकृत = जिसके ऊपर उपकार हुआ/उपकार-प्राप्त; विलोम नहीं।
(4) दुष्ट = बुरा व्यक्ति; ‘कृतज्ञ’ का विपरीत नहीं।
टिप्पणी: प्रश्न-चित्र में मूल शब्द धुँधला था; प्रसंग और विकल्पों के आधार पर ‘कृतज्ञ’ मानकर उत्तर दिया गया है।
Quick Tip: कृत = किया हुआ (उपकार) + ज्ञ = जानने वाला ⇒ कृतज्ञ (grateful); घ्न = हन्त/नष्ट करने वाला ⇒ कृतघ्न (ungrateful)।
“चौराहा” का तत्सम है—
View Solution
Step 1: परिभाषा.
तत्सम = संस्कृत से यथावत् लिया गया रूप।
Step 2: रूप-सम्बन्ध.
‘चौराहा’ (चार दिशाओं का मिलन-बिंदु) का संस्कृत तत्सम रूप चतुष्पथ (चतु{=चार+पथ{=मार्ग) है।
Step 3: अन्य विकल्प.
(1) चतुर्द्व — मान्य/प्रचलित तत्सम रूप नहीं।
(3) तिराहा — तीन मार्गों का मिलन-बिंदु; अर्थ भिन्न।
(4) इनमें से कोई नहीं — आवश्यक नहीं क्योंकि (2) सही है।
Quick Tip: चतुर्/चतु: = चार, पथ = मार्ग ⇒ चतुष्पथ (चौराहा); तीन राहों का मिलन = त्रिमार्ग/तिराहा।
‘कर्ण’ का तद्भव है—
View Solution
Step 1: सिद्धान्त.
तद्भव वह रूप है जो लोक-भाषाओं में विकसित हुआ हो।
Step 2: रूप-सम्बन्ध.
संस्कृत ‘कर्ण’ (ear) का तद्भव हिन्दी में कान होता है। अन्य विकल्प अर्थ/रूप से मेल नहीं खाते।
Quick Tip: संस्कृत ‘ण’ ध्वनि का तद्भव में ‘न’ बन जाना सामान्य है: कर्ण→कान, वर्ण→बन/रंग (सन्दर्भानुसार)।
जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, उसे कहते हैं—
View Solution
Step 1: परिभाषा.
आस्तिक = ईश्वर/शास्त्र/परलौकिक सत्ता में विश्वास रखने वाला; नास्तिक = ऐसा विश्वास न रखने वाला।
Step 2: विकल्प-जांच.
परिभाषा के अनुसार नास्तिक ही उपयुक्त शब्द है। बाकी विकल्प अर्थ से मेल नहीं खाते।
Quick Tip: आस्तिक/नास्तिक—‘ना’ उपसर्ग के कारण नकारात्मक अर्थ—याद रहना आसान।
‘पुरोहित’ का संधि-विच्छेद है—
View Solution
Step 1: मूल पदों की पहचान.
‘पुरः’ (= साम्हने/आगे) + ‘हित’ (= कल्याण)
Step 2: संधि-नियम.
‘ः + ह’ के संयोग से ‘र’ ध्वनि का आगमन होता है, अतः ‘पुरः + हित’ \(\rightarrow\) पुरोहित।
Step 3: विकल्प-जांच.
(1) पुरः + हित — नियमानुसार सही। अन्य विकल्प मूल-रूप/अर्थ से मेल नहीं खाते।
Quick Tip: ‘ः + ह’ \(\rightarrow\) ‘र’ (या ‘रो’) बनने का नियम याद रखें: पुरः + हित → पुरोहित।
‘पतिव्रता’ शब्द में विभक्ति और वचन है— (विकल्प अस्पष्ट)
View Solution
Step 1: पद-रूप.
‘पतिव्रता’ स्त्रीलिंग संज्ञा है; प्रश्न में स्वतंत्र रूप दिया गया है, अतः सामान्यत: प्रथमा विभक्ति, एकवचन मानी जाती है।
Step 2: टिप्पणी.
यदि वाक्य-संदर्भ दिया हो तो विभक्ति-वचन बदल सकते हैं; किन्तु यहाँ सन्दर्भ न होने से प्रथमा-एकवचन मानक उत्तर है।
Quick Tip: बिना वाक्य-संदर्भ के दिये गए स्वतंत्र संज्ञा-रूप को सामान्यतः प्रथमा-एकवचन माना जाता है।
‘पठेयं’ में वचन और पुरुष है—
View Solution
Step 1: रूप-पहचान.
‘पठेयं’ संस्कृत विधिलिङ् (सम्भावना/इच्छा) का उत्तम पुरुष, एकवचन रूप है—अर्थ: “मैं पढ़ूँ/पढ़ूँगा (कदाचित्)”।
Step 2: विकल्प-जांच.
रूपांत \(-ेयं\) का अंत सामान्यतः उत्तम-एकवचन को सूचित करता है; अतः (1) सही।
Quick Tip: विधिलिङ् में \(-ेयं\) \(\Rightarrow\) उत्तम पुरुष एकवचन; \(-ेत\) \(\Rightarrow\) प्रथम (अन्य) पुरुष।
निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
क्रोध का असर सबसे भयावह होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि की बात नष्ट नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की स्मृति यदि दूषित हो जाएगी, तो उसकी कोई भी योजना—जो वह पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर और जल्दी-जल्दी तैयार करे—उन दिनों असफल हो जाएगी। लोक-हित की ओर न जाकर, वह निजी प्रतिहिंसा/दुराग्रह में बदल जाएगी और यदि प्रतिहिंसा न भी हो तो वह सस्ते ढंग से हँसा देने वाली मूर्ख वायु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर ढकेल देगी।
प्रश्न:
(ii) व्याख्या (रेखांकित अंश): क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है; तथा क्रोधजन्य प्रवृत्ति व्यक्ति को लोक-हित से हटा कर हल्की-फुल्की, मूर्खतापूर्ण दिशा में ले जाती है।
(iii) क्रोध का प्रभाव: नीति-बुद्धि का नाश, स्मृति/विवेक का दूषित होना, योजनाओं का असफल होना और उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर गिरना।
View Solution
Step 1: प्रसंग (Context).
गद्यांश में लेखक यह सिद्ध करता है कि क्रोध मनुष्य की बौद्धिक-संरचना को सबसे अधिक क्षति पहुँचाता है; यह विषय आचरण-नीति/चरित्र-विकास के प्रसंग में उठाया गया है।
Step 2: रेखांकित अंश की व्याख्या.
(क) “बुद्धि का भी नाश कर देता है”—क्रोध क्षणिक आवेग में मन की विवेक-शक्ति छीन लेता है; परिणामस्वरूप सही-गलत का निर्णय भंग हो जाता है और निर्णय आवेग-प्रधान हो जाते हैं।
(ख) “सस्ते ढंग से हँसा देने वाली मूर्ख वायु”—क्रोध की दिशा लोक-हितकारी नहीं रहती; वह हल्के, अपरिपक्व, चंचल और दिखावटी व्यवहार में बदल जाती है, जो क्षणिक संतोष तो दे परन्तु दीर्घकालीन उन्नति में बाधक होती है।
Step 3: प्रभाव का निरूपण.
क्रोध: (i) नीति/सद्बुद्धि को निष्प्रभावी करता है, (ii) स्मृति और योजना-क्षमता को दूषित कर देता है, (iii) अनुभव-आधारित योजनाएँ भी असफल होने लगती हैं, (iv) व्यक्ति निजी प्रतिहिंसा/दुराग्रह में फँसकर अवनति की ओर लुढ़कता है।
Quick Tip: व्याख्या-प्रश्न लिखते समय (a) प्रसंग—कहाँ/किस उद्देश्य से कहा गया, (b) व्याख्या—शब्दार्थ व आशय, (c) समापन—मुख्य संदेश—तीन खंडों में उत्तर लिखें।
अथवा
निम्न वैकल्पिक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
जहाँ-जहाँ हमारे नैतिक सिद्धान्तों का वर्णन आया है, अहिंसा को उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम ‘क्षमा’ भी माना गया है और क्षमा का दूसरा रूप त्याग या संयम के रूप में हमारे सामने आता है। यदि हमारी संस्कृति ने हमें अभिमान से ऊपर उठना और त्याग सीखाया है तो वह इसी नैतिक परंपरा के कारण है; अतः क्षमा-भाव को अपनाकर व्यक्ति के मन से क्रोध, द्वेष और प्रतिहिंसा हटती है, और जीवन-आचरण शुद्ध तथा आत्म-शासन से भर जाता है।
प्रश्न:
(ii) व्याख्या (रेखांकित): अहिंसा का व्यावहारिक रूप क्षमा है; क्षमा अपनाने से अहंकार-द्वेष शान्त होते हैं और व्यक्ति त्याग/संयम से युक्त शुद्ध आचरण की ओर अग्रसर होता है।
(iii) प्रमुख स्थान: अहिंसा; इसका दूसरा रूप: क्षमा (और व्यावहारिक विस्तार में त्याग/संयम)।
View Solution
Step 1: प्रसंग (Context).
यह गद्यांश भारतीय सांस्कृतिक नैतिकता की व्याख्या करता है—समाज और व्यक्ति के आचरण में अहिंसा को सर्वोच्च आदर्श मानते हुए।
Step 2: रेखांकित अंश की व्याख्या.
(क) “अहिंसा का दूसरा नाम क्षमा”—अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से विरति नहीं, बल्कि मन-वाणी-कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाने की वृत्ति है; इसका आंतरिक रूप क्षमा है, जो द्वेष का शमन करती है।
(ख) “यदि हमारी संस्कृति ने अभिमान से ऊपर उठना और त्याग सिखाया है”—भारतीय परंपरा अहंकार-त्याग, संयम, आत्म-शासन पर बल देती है; इससे व्यक्ति में करुणा, सहिष्णुता, आत्मसंयम विकसित होते हैं।
Step 3: निष्कर्ष.
भारतीय नैतिक सिद्धान्तों का केन्द्रीय मूल्य = अहिंसा; इसका व्यावहारिक/द्वितीय रूप = क्षमा (और उसके सहायक रूप त्याग/संयम) हैं, जो व्यक्ति-समाज दोनों के शुद्ध आचरण का आधार बनते हैं।
Quick Tip: नैतिकता-सम्बन्धी गद्यांश में परिभाषा (अहिंसा/क्षमा), व्यावहारिक रूप (संयम/त्याग), और प्रभाव (व्यक्तिगत-सामाजिक लाभ)—तीनों को जोड़कर उत्तर लिखें।
दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
सुनि सुंदर बैनि मधुरास साने, सयानी हैं जानकी जानी भली।
तिरछे करि नैन दे सैंन तिन्हें, समझाइ करू मुसुकाइ चली॥
तुलसी तेहि औसर सोहें सबै, अवलोकति लोचन लालु अली।
अनुराग-तड़ागा में मानु उठे, विगसि मनो मञ्जुल कंज कलि॥
(ii) व्याख्या: कवि कहता है—उस समय सीता के लोचन (नेत्र) ऐसे भँवरों (अली) से प्रतीत होते हैं जो अनुराग रूपी सरोवर में उड़कर कमल-कलियों (मुख/मुखकमल) पर बार-बार अवलोकन कर रहे हों; अर्थात प्रेम, लज्जा और सौंदर्य से भरी हुई दृष्टि चारों ओर छा गई।
(iii) अलंकार: रूपक (मुख=कमल, नेत्र=भँवरे—रूप का आरोप)\; सहायक: अनुप्रास (सुनि सु{ं}दर, मधुरास साने, मञ्जुल कज कलि)।
छन्द: सवैया (दीर्घ-गणप्रधान, तुक-ध्वनि-संरचना सवैया के अनुरूप)।
View Solution
Step 1: प्रसंग.
कवि सौम्य-शृंगार को लोकमर्यादा से जोड़ते हैं; सीता का व्यवहार विनय, लज्जा, संयम से युक्त है।
Step 2: रेखांकित अंश की व्यंजना.
‘लोचन लालु अली’—यहाँ लोचन = भँवरे (अली) की तरह स्वाभाविक चंचल हैं; ‘अनुराग-तड़ाग’ में उठना-विगसना प्रेम की तरंग और मुखकमल के विकास का संकेत है।
Step 3: अलंकार-छन्द का औचित्य.
रूपक से दृश्य एकात्म हो उठता है (उपमेय-उपमा का भेद मिटता है), और सवैया की संगति सौंदर्य की लयात्मकता बढ़ाती है।
Quick Tip: यदि उपमा में ‘सा/सम’ हो तो उपमा; बिना ‘सा/सम’ सीधे रूप आरोपित हो तो रूपक—यही भेद याद रखें।
अथवा
(अथवा) निम्न पंक्तियाँ पढ़कर उत्तर दीजिए—
चींटी को देखा?
वह सरल, विरल काली रेखा,
तम के तागे-सी जो हिल-डुल
चलती लघु पद पल-पल मिल-जुल,
वह है पिपीलिका पाँति।
देखो ना, किस भाँति
काम करती वह सतत!
कण-कण कणक चुनती अविरत।
(ii) व्याख्या (रेखांकित “कण-कण कणक चुनती अविरत”): चींटियाँ बूंद-बूंद/कण-कण अन्न (कणक) को निरंतर चुनती-संग्रह करती हैं—अल्प साधनों से, पर लगातार श्रम से बड़ा संचय हो जाता है।
(iii) शिक्षा: निरंतर परिश्रम, अनुशासन, सहयोग, अल्प-संचय की महत्ता—इन्हीं से सफलता मिलती है।
View Solution
Step 1: दृश्य का अर्थ-आलोक.
‘सरल, काली रेखा’—चींटियों की क़तार; ‘तम के तागे-सी’—उपमा से रंग/आकृति का बोध।
Step 2: रेखांकित अंश की व्याख्या.
‘कण-कण’ की पुनरुक्ति पद-गौरव एवं अनुप्रास का भाव देती है—निरंतरता का प्रभाव बढ़ता है।
Step 3: नीतिपरक निष्कर्ष.
सामूहिकता और सतत श्रम व्यक्ति-निर्माण का मूल तत्व है—यही कविता का संदेश है।
Quick Tip: ‘पुनरुक्ति-प्रयोग’ (दोहराव) से निरंतरता/ज़ोर का प्रभाव उत्पन्न होता है—व्याख्या में इस संकेत का उपयोग करें।
(क) दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सन्दर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए:
एषा नगरी भारतीय संस्कृते। संस्कृत भाषायाः केन्द्र–स्थानीम् अस्ति। इतः एव संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृतेः आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मग़ध–गुजरातः, द्वार–शिखरः; अयं भारतीय–दर्शन–शास्त्राणां अध्यात्मस्य अङ्कुरः। सः तेजसा ज्ञानेन च प्रभातितः। अम्बरात्, यत्र तेः उपनिषद्–अनुवादः पारसी भाषायाम् अपि कृतः।
विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः। एक एव इति भारतीयः संस्कृतिः मन्यते। विभिन्न मतावलम्बिनां विधिः: नगानां; एकमेव एव ईश्वरं भजन्ति। अग्निः, इन्द्रः, कृष्णः, शिवः, रमाः, लक्ष्मीः, जगन्नाथः, शिवता–आदि:—इत्यान्ये\; नामानि एकस्य एव परमानन्दस्य: सकलं। तं एव ईश्वरम् जनाः: गुरुः इति मन्यन्ते। अतः सर्वेषां मतानां समभावः—समन्वयस्य उत्कृष्टं संस्कृतः संदेशः।
View Solution
N/A Quick Tip: अनुवाद में पहले कर्त्ता–क्रिया–कर्म पहचानें, फिर समुच्चय/सम्बन्ध सूचक अव्ययों (एव, च, अपि) का अर्थ जोड़ें—भावार्थ स्वतः साफ़ होगा।
अथवा
(ख) दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सन्दर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद कीजिए:
किंसिद्ध प्रवसतो मित्रं, किंसिद्ध गृहमेव सतः।
आतुरस्य च किं मित्रं, किंसिद्ध मित्रं मरणेः॥
मङ्गलं मरणं यत्र विभूतिर्वर्ण भूषणम्।
कौशेयं यत्र कौशेयं काशि के नोपरायणम्॥
View Solution
श्लोक–1:
Step 1: संदर्भ. नीति-शास्त्रीय श्लोक जीवन-स्थितियों में सच्चे सहायक को पहचानने की शिक्षा देता है।
Step 2: भावार्थ. परिस्थिति-विशेष में उचित/सच्चा मित्र बदल सकता है—पर मृत्यु-क्षण में केवल धर्म/कर्म ही साथ देता है।
श्लोक–2:
Step 1: संदर्भ. श्लोक काशी की मोक्ष-भूमि और धार्मिक–आध्यात्मिक महिमा का गुणगान करता है।
Step 2: भावार्थ. काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है, भस्म/विभूति पवित्र मानी जाती है—अतः वह श्रेष्ठ तीर्थ है।
Quick Tip: नीति/तीर्थ-महिमा के श्लोकों में अनुवाद + संक्षिप्त विवेचन दें—उदाहरण/संदर्भ जोड़ने से उत्तर प्रभावी बनता है।
(क) निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन-परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए:
View Solution
Step 1: संक्षिप्त जीवन-परिचय. जन्म–वाराणसी; पारिवारिक पृष्ठभूमि—तंबाकू-व्यापार; साहित्य-साधना में आरम्भ से रुझान।
Step 2: साहित्यिक योगदान. काव्य में छायावादी प्रवृत्ति, नाटक में ऐतिहासिक/पौराणिक चेतना, गद्य में कथा-शिल्प।
Step 3: प्रमुख कृतियाँ और महत्व. ‘कामायनी’—मानव-जीवन के मानस-चक्र का रूपक; नाटक—भारतीय गौरव-परंपरा का नवीनीकरण।
Final Answer:
जयशंकर प्रसाद (1889–1937): वाराणसी में जन्मे प्रसाद जी छायावाद के चार स्तंभों में से एक थे। काव्य, नाटक, कथा-साहित्य—तीनों में समान अधिकार रहा। उनकी काव्य-कृति ‘कामायनी’ (महाकाव्य) तथा नाट्य-कृतियाँ—‘स्कन्दगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’, ‘चन्द्रगुप्त’—विशेष प्रसिद्ध हैं। गद्य में ‘आँसू’, ‘झरना’, ‘लहर’ काव्य-संग्रह; कहानी-संग्रह ‘इन्द्रजाल’, ‘प्रतिध्वनि’ आदि आते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में आध्यात्म, सौंदर्य-बोध, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय करुणा का समन्वय मिलता है।
प्रमुख रचना: ‘कामायनी’। Quick Tip: जीवन-परिचय लिखते समय क्रम रखें: जन्म–शिक्षा–वैयक्तिक विशेषता–मुख्य विधाएँ–प्रमुख कृतियाँ–वैशिष्ट्य/योगदान।
(ख) निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन-परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए:
View Solution
Step 1: युग व स्थान. भक्तिकाल (सगुण शाखा), पुष्टि-मार्ग परंपरा से सम्बद्ध।
Step 2: काव्य-विशेषता. ‘दृश्य-चित्रण’, ‘मानवीय मनोविज्ञान’, ‘सहज बोलचाल की ब्रजभाषा’।
Step 3: रचना-सार. ‘सूरसागर’ में कृष्ण के लीलावतार की मार्मिक, रम्य, जीवंत प्रस्तुति।
Final Answer:
सूरदास (15वीं–16वीं शती): भक्तिकाल के श्रृंगार-रस/वात्सल्य-भाव के अमर कवि। जन्म-स्थल विवादित; परंपरा में वल्लभाचार्य के आश्रित माने जाते हैं। कृष्ण-लीलाओं के मानवीय–आलौकिक रूप का सुकोमल चित्रण उनकी विशेषता है।
प्रमुख रचना: ‘सूरसागर’ (विशेषतः ‘बाललीला’, ‘रास-लीला’ प्रसंग)। Quick Tip: कवि-परिचय में युग, भाषा, धारा, प्रमुख भाव/रस, एक-दो प्रतिनिधि रचनाएँ अवश्य लिखें।
दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए (यहाँ सभी तीनों के उत्तर दिए जा रहे हैं):
View Solution
Step 1: कर्तृ–क्रिया–कर्म पहचान. ‘कुत्र’ = कहाँ; ‘कः’ = कौन; ‘कस्मात् उच्यते’ = किस कारण से कहलाता है।
Step 2: सरल वाक्य-रचना. कर्ता–कर्म–क्रिया क्रम में प्रथमा/सप्तमी विभक्तियाँ प्रयोग करें: ‘गङ्गायाः तटे’ (सप्तमी)।
Step 3: परिभाषात्मक उत्तर. ‘पिता’—जनन/पालन करने वाला (कर्त्ता) — ‘उच्यते’ धातु से परिभाषा।
Final Answer:
(i) वाराणसी नगरी गङ्गायाः तटे स्थिताऽस्ति।
(ii) ईश्वरः विश्वस्य स्रष्टा अस्ति।
(iii) यः जनयति पालनं च करोति सः पिता उच्यते। Quick Tip: संस्कृत उत्तरों में सदा सरल विभक्ति और लकार चुनें: प्रथमा (कर्ता), सप्तमी (स्थान), अस्ति/उच्यते—स्पष्टता बढ़ती है।
(क) ‘हास्य’ अथवा ‘करुण’ रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए।
View Solution
Step 1: रस-तत्त्व. रस = स्थायीभाव का रस-निष्पादन; विभाव–अनुभाव–व्यभिचारी का समुच्चय।
Step 2: किसी एक रस का ठोस उदाहरण. हास्य में उपहास/विदूषक; करुण में वियोग/विलाप—उदाहरण सहित लिखें।
Final Answer:
हास्य रस: विघ्न/विचित्र/उपहासजन्य स्थितियों से उत्पन्न आनन्द/हँसी की भावावस्था; स्थायीभाव—हास (हँसना); विभाव—हास-कारक कारण/वेषभूषा; अनुभाव—हँसना, दाँत दिखाना, अंगों का कम्पन इत्यादि।
उदाहरण: विदूषक का लतीफ़ा सुनकर सभा में सब जोर से हँस पड़े—हास्य रस व्यक्त।
(या) करुण रस: शोक/दुःख से उत्पन्न रस; स्थायीभाव—शोक; विभाव—वियोग, वध, पराभव; अनुभाव—आँसू, विषाद, निःश्वास आदि।
उदाहरण: भरत का राम-वनगमन पर विलाप—करुण रस। Quick Tip: उत्तर में स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव तीन शब्द अवश्य आएँ—इन्हीं से रस की पहचान पक्की होती है।
(ख) ‘रूपक’ अथवा ‘उत्प्रेक्षा’ अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए।
View Solution
Step 1: भेद-रेखा. रूपक = रूप आरोप, सूचक नहीं; उत्प्रेक्षा = कल्पना, सूचक अव्यय होते हैं।
Step 2: उदाहरण चुस्त. एक-एक पंक्ति पर्याप्त—उपमेय/उपमान स्पष्ट रहें।
Final Answer:
रूपक अलंकार: जब उपमेय पर उपमान का सीधा रूप आरोपित कर दिया जाए और उपमा–सूचक शब्द (सा/सम/जैसे) न हों।
उदाहरण: “मुख कमल खिल उठा, लोचन अलि बनने लगे।”
(या) उत्प्रेक्षा अलंकार: किसी वस्तु में दूसरी वस्तु के गुण होने की कल्पना करना—मानो/यदि/जैसे आदि सूचक हों।
उदाहरण: “नभ में मानो चाँदनी चाँदी बिछा रही हो।” Quick Tip: याद रखें—“जैसे/मानो” दिखे तो उत्प्रेक्षा; नहीं दिखे और सीधा रूप आरोप हो तो रूपक।
(ग) ‘दोहा’ अथवा ‘चौपाई’ छन्द के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए।
View Solution
Step 1: मात्रा-संरचना. दोहा—24 प्रति पंक्ति (13+11/11+13); चौपाई—16 मात्रिक चौ-चरण।
Step 2: उदाहरण-संगति. पाठ्यपुस्तक/लोकोक्ति से मानक पंक्तियाँ चुनें—लक्षण से मेल अनिवार्य।
Final Answer:
दोहा (लक्षण): 24 मात्राएँ प्रति पंक्ति; पहली और तीसरी चरण में 13–11, दूसरी और चौथी में 11–13 मात्राओं का क्रम (विराम 13 पर)।
उदाहरण (दोहा):
“जो उगे सो ढलना है, जो फूले सो झार।
जो आए सो जाना है, रहे न कोउ संसार॥”
(या) चौपाई (लक्षण): चार चरण; प्रत्येक में 16-16 मात्राएँ (सममात्रिक), तुलसी काव्य में व्यापक।
उदाहरण (चौपाई):
“श्रीगुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि।
बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥” Quick Tip: छन्द-प्रश्न में मात्रा-गणना का एक वाक्य अवश्य लिखें—यही सबसे बड़ा अंक दिलाने वाला बिन्दु है।
निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए उसको अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए:
View Solution
Step 1: लोकोक्ति/मुहावरा का भावार्थ एक वाक्य में स्पष्ट करें।
Step 2: उसी भावार्थ को स्वाभाविक प्रसंग में रखकर एक सही, संक्षिप्त वाक्य लिखें।
Step 3: अर्थ और प्रयोग में काल/पुरुष/वचन की संगति बनाए रखें।
Final Answer:
(i) अर्थ: जो बात स्पष्ट प्रमाण सहित हो, उसे साबित करने के लिए अलग दिखावे/दलील की आवश्यकता नहीं।
वाक्य-प्रयोग: अंक–तालिका सामने है—हाथ कंगन को आरसी क्या, मेरी योग्यता पर संदेह क्यों?
(ii) अर्थ: दोषी व्यक्ति ही अपने दोष छिपाने के लिए निर्दोष को उलटे डाँटे/इल्ज़ाम दे।
वाक्य-प्रयोग: चोरी पकड़ी जाने पर रमेश ने गार्ड को ही दोषी बताना शुरू कर दिया—यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे है।
(iii) अर्थ: अल्पज्ञ/अकुशल व्यक्ति ही अधिक दिखावा करता है; सच्चा विद्वान विनम्र रहता है।
वाक्य-प्रयोग: दो अध्याय पढ़कर ही रवि बड़े-बड़े ज्ञान बाँटने लगे—अधजल गगरी छलकत जाय। Quick Tip: पहले अर्थ लिखें, फिर प्रयोग; यदि उदाहरण में प्रसंग सटीक हुआ तो पूरे अंक मिलते हैं।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए:
View Solution
(i) विज्ञान: वरदान या अभिशाप — निबंध
प्रस्तावना: विज्ञान ने मानव-जीवन को गति, सुविधा और संभावना दी है; परंतु दुरुपयोग से वही शक्ति विनाश भी ला सकती है।
विज्ञान का वरदान: चिकित्सा में प्रगति (टीके, प्रत्यारोपण), संचार–क्रांति, परिवहन–विस्तार, कृषि–उत्पादन, अंतरिक्ष–अनुसंधान—सभी ने मानवता का क्षितिज बढ़ाया।
संभावित अभिशाप: परमाणु–शस्त्र, साइबर–अपराध, निजता–भंग, पर्यावरण–हानि, निर्जीव–मानवीय संबंध—ये दुष्परिणाम मानव–केंद्रित नैतिकता के अभाव से पैदा होते हैं।
समाधान: एथिक्स–बाई–डिज़ाइन, हर शोध में मानव–कल्याण की कसौटी, पर्यावरणीय नियमन, डिजिटल साक्षरता।
उपसंहार: विज्ञान स्वयं न ता वरदान, न अभिशाप—यह उपयोग का उपकरण है; सही उपयोग इसे वरदान बनाता है।
(ii) प्रदूषण समस्या: कारण और निवारण — निबंध
भूमिका: वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण आज वैश्विक संकट हैं।
मुख्य कारण: अनियंत्रित उद्योगीकरण, वाहनों की भीड़, पॉलीथिन/सिंगल–यूज़ प्लास्टिक, गंदे नालों का नदियों में गिरना, वन–क्षय।
परिणाम: श्वास–रोग, कैंसर–जोखिम, कृषि–उत्पादकता में गिरावट, जैव–विविधता का ह्रास, जल–संकट।
निवारण: स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, कचरा–विभाजन/रिसाइक्लिंग, अपशिष्ट–प्रबंधन, जलशोधन, वृक्षारोपण, कड़े पर्यावरण–क़ानून और नागरिक भागीदारी।
उपसंहार: हरित विकास ही टिकाऊ भविष्य का मार्ग है—Reduce–Reuse–Recycle को जीवन–शैली बनाना होगा।
(iii) अनुशासन का महत्त्व — निबंध
परिचय: अनुशासन—नियमबद्ध जीवन का नाम; स्व–नियंत्रण इसका मूल है।
व्यक्तिगत स्तर: समय–पालन, लक्ष्य–निर्धारण, नियमित अभ्यास—यही सफलता का सूत्र।
सामाजिक/राष्ट्रीय स्तर: यातायात–नियम, कर–ईमानदारी, कर्तव्य–पालन—इनसे व्यवस्था और विकास सुनिश्चित होता है।
निष्कर्ष: स्व–अनुशासन बिना बाहरी दंड के सर्वोत्तम परिणाम देता है—यही सच्ची स्वतंत्रता है।
(iv) मेरा प्रिय कवि — (उदाहरण: सुमित्रानंदन पंत)
परिचय: छायावाद के अग्रणी; प्रकृति–सौंदर्य और मानवीय संवेदना के कवि।
काव्य–वैशिष्ट्य: कोमल चित्रात्मकता, संगीतात्मक लय, मानवीय करुणा; ‘पल्लव’, ‘गुंजन’ आदि संग्रह।
मुझे क्यों प्रिय: उनकी कविताएँ प्रकृति–प्रेम और मानव–मूल्यों को एक करती हैं; भाषा सरल, भाव गहन।
उपसंहार: पंत की काव्य–धारा आज भी रसमय प्रेरणा देती है—इसी कारण वे मेरे प्रिय हैं। Quick Tip: बोर्ड परीक्षा में निबंध 250–300 शब्द का रखें; थीम–स्टेटमेंट पहली पंक्ति में, कार्य–उपाय अंत में लिखें।




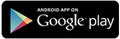


Comments